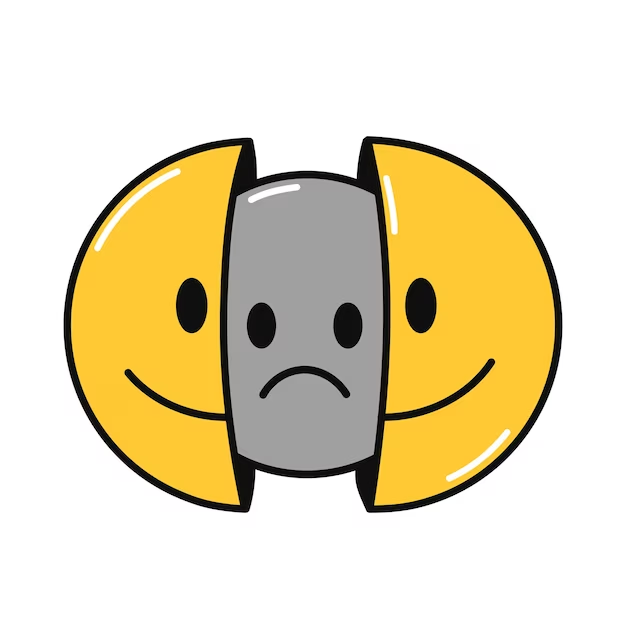देश में उदारीकरण के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं. कोई आम आदमी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज कराने का सपना भी नहीं देख सकता है. विकल्प सरकारी अस्पताल हैं. लेकिन, जब ज़रूरी दवाएं भी न मिलें, तो उसका जीवन भगवान भरोसे ही रह जाता है.
 यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर दवाइयों तक, अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की क़ीमत का निर्धारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाज़ार के हवाले कर दिया. कुछ साल पहले तक आवश्यक दवाओं की क़ीमत का निर्धारण कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग (सीबीपी) मेकनिज्म के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य मार्केट बेस्ड
यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर दवाइयों तक, अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की क़ीमत का निर्धारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाज़ार के हवाले कर दिया. कुछ साल पहले तक आवश्यक दवाओं की क़ीमत का निर्धारण कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग (सीबीपी) मेकनिज्म के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य मार्केट बेस्ड
प्राइजिंग (एमबीपी) मकेनिज्म के आधार पर किया जा रहा है. सीबीपी के तहत दवा के निर्माण में आई कुल लागत में एक निश्चित सीमा तक मुनाफा जोड़कर दवा की ख़ुदरा(रीटेल) कीमत निर्धारित की जाती थी. इसके लिए मूल्य निर्धारण नियामक यानी नेशनल फॉर्मासुटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) दवा निर्माताओं की यूनिटों में सीधे जाकर दवा निर्माण में आने वाली लागत के आंकड़े एकत्र करती थी. लागत मूल्य प्राइज रेगुलेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे. इसे मेनीपुलेट करने की कंपनियां हरसंभव कोशिश करती थीं. उदाहरण के लिए नई तकनीक के उपयोग के नाम पर कंपनियां हमेशा अपनी लागत को बढ़ाना चाहती थीं. 2011-12 की शुरुआत में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सभी कंपनियों, जिनमें औषधि निर्माता कंपनियां भी शामिल थीं, को उत्पाद बनाने में आई लागत के आंकड़े जारी करने का निर्देश दिया. इसके बाद से दवा कंपनियों द्वारा लागत के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग दवाओं के रीटेल प्राइज निर्धारण करने में किया जाने लगा.
वर्ष 1990 के बाद ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के अंतर्गत आने वाली दवाओं की संख्या में लगातार कमी आने लगी. 1979 में डीपीसीओ के अंतर्गत 347 दवाएं आती थीं, जो कि वर्ष 1987 में घटकर 142 और 1995 में घटकर केवल 76 तक पहुंच गईं. 2002 में जो नीति प्रस्तावित थी, उसमें यह संख्या घटकर 35 हो गई होती, लेकिन भला हो सिविल सोसायटी का, जिसने सरकार के इस फैसले के विरोध में आवाज उठाई. इस मसले सुनवाई करते हुए 2003 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस नीति पर रोक लगा दी. इसके बाद से ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित था. इसके बाद एक नई नीति का आगमन सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सीधा-सीधा परिणाम है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को न केवल सभी जीवन रक्षक दवाओं को प्राइज कंट्रोल के दायरे में लाने का निर्देश दिया, बल्कि 1995 की सीबीपी मेकेनिज्म को भी यथावत रखने को कहा. वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) जारी करने का निर्देश दिया. सरकार ने एनएलईएम-2011 जारी की. इसके बाद औषधि विभाग ने नई औषधि नीति पर काम करते हुए विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत शुरू की. बड़े और मझोले औषधि उत्पादक बाज़ार आधारित क़ीमत निर्धारण के तरीके के पक्ष में थे, जबकि छोटे औद्योगिक संस्थान कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग (सीबीपी) मेकेनिज्म को यथावत रखने के पक्ष में थे. यहां तक कि सरकार में भी इसे लेकर दो धड़े थे, जो क़ीमत निर्धारण के अलग-अलग तरीकों की पैरवी कर रहे थे. पिछले तीन दशकों में न केवल कंट्रोल्ड दवाओं की संख्या में कमी आई, बल्कि कंट्रोल कैटेगरी की संख्या भी घटी है, जबकि इस दौरान कई दवाइयां पेटेंट के दायरे से बाहर आ गईं. बावजूद इसके, उनकी क़ीमतों में कमी नहीं हुई. दवा निर्माताओं के मुनाफे में लगातार इजाफा होता गया. 1995 के प्राइज कंट्रोल ऑर्डर ने उत्पादन के बाद के खर्च को बढ़ाकर लागत का 100 प्रतिशत कर दिया था, जबकि 1979 में यह 40 से 75 प्रतिशत के बीच सीमित था. इससे यह ज़ाहिर होता है कि सरकार संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को ताक पर रखकर दवा निर्माताओं के कल्याण की नीतियां बना रही थी. नई नीति में आवश्यक औषधियों की क़ीमतों का निर्धारण मार्केट बेस्ड प्राइज के जरिए करने के पीछे सरकार का तर्क था कि वर्ष 2015 के अंत तक अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों में लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की दवाएं पेटेंट से बाहर होंगी. उसके बाद उत्पन्न होने वाली निर्यात की संभावनाओं का लाभ देश नहीं उठा पाएगा. नई नीति की मदद से कंपनियों को खुद को उचित मूल्य बैंड में रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, जिससे वे वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सकेंगी.
एनएलईएम-2011 में सूचीबद्ध दवाओं का नियंत्रण मूल्य दवा की खुराक और ताकत के आधार पर निर्धारित होता है. आज आवश्यक दवाओं की क़ीमत का निर्धारण निम्न फॉर्मूले के आधार पर हो रहा है:- (बाज़ार में संबंधित दवा की बिक्री में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली तीन कंपनियों का भारित औसत मूल्य(डब्लूएपी)+ बाजार में एक प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों का डब्लूएपी)/दवा का उत्पादन करने वाले उत्पादकों की कुल संख्या.
वर्ष 1979 में औषधियों के दाम निर्धारित करने का सीधा और सरल तरीका ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के रूप में जारी किया गया था. इसके बाद 1986 एवं 1995 में डीपीसीओ अपने लिए ताकत आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3 से हासिल करते रहे. वर्ष 1979 की नीति और इसके बाद की नीतियों के निर्माण में जयसुख लाल हाथी आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख भूमिका रही. दवा बाज़ार का चरित्र मोनापोली के माध्यम से समझा जा सकता है. दवा बाज़ार पर कुछ कंपनियों की मोनोपोली होती है.बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं सामान्य तौर पर सबसे मंहगी या महंगी दवाओं में से एक होती हैं.
दवाओं की कीमत निर्धारण के नए तरीके से जनता को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है. सिप्रॉफ्लॉक्सिन नामक एंटीबायोटिक दवा बाजार में एक कंपनी 9.79 रुपये में बेचती है, वही दवा बाज़ार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी 73.30 रुपये में बेचती है. बाज़ार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली तीन सबसे बड़ी कंपनियों की औसत क़ीमत 67 रुपये और एक प्रतिशत या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों की औसत क़ीमत 50.40 रुपये है. लागत आधारित व्यवस्था के तहत इस दवा की क़ीमत 26.57 रुपये होती है, जबकि बाज़ार आधारित व्यवस्था के तहत यह कीमत 58.70 रुपये है. इसका सीधा मतलब है कि सरकार दवा कंपनियों को दुगने से भी ज्यादा मुनाफा बनने की क़ानूनी तौर पर छूट दे रही है. वह भी उस मुद्दे पर जिसका सीधे तौर पर आम आदमी के जीन-मरने से है. दवा कंपनियां क़ानूनी तौर पर आम आदमी को लूट रही हैं और सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों के नियंत्रण का खोखला दंभ भर रही है.
राजनीतिक दलों को दवा कंपनियों का चंदा
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में चार प्रतिशत हिस्सेदारी दवा निर्माता कंपनियों की है. जॉयडस वेलनेस लिमिटेड, कैडिला फॉर्मासुटिकल्स लिमिटेड, यूनीकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, हेट्रो ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रैनुल्स इंडिया लिमिटेड, जेनिक्स फॉर्मा, बायोसर्व क्लीनिकल रिसर्च, नवयुग मेडिकल्स, डायना मेडिकल सर्विस, अरबिंदो फॉर्मा, विकास फार्मा, देहली फॉर्मा, दिशमान फॉर्मासुटिकल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आदि कंपनियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा दिया है. 2004-05 से 2011-12 तक रसायन और दवा कंपनियों ने 16.54 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिए हैं, जिसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा 10.12 करोड़ रुपये मिले. इसके बाद कांग्रेस 5.54 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है.