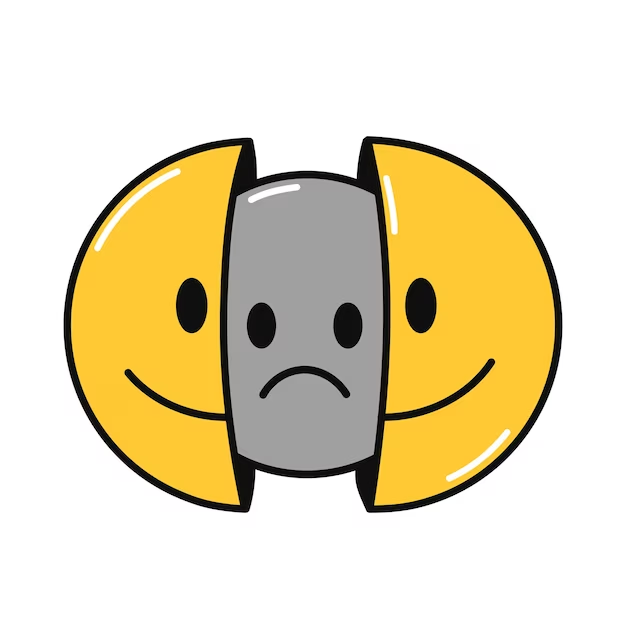‘तालिबान’ के बरक्स अफगानिस्तान से भारत के कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं, जो शायद तालिबान चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे। हालांकि कट्टरपंथ की विशेषता यही है कि वो जो कहता है, करता उसका उल्टा है। एक साथ दो नावों पर सवार होकर अपना लक्ष्य साधता रहता है। अफगानिस्तान के बदतर होते हालात के बीच एक खबर काबुली चने की आई और यह भी कि तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर काबिज होते ही भारत में सूखे मेवे ने महंगाई का रास्ता पकड़ लिया है। कारण कि माल की सप्लाई अटक गई है। भारतीय व्यापारियों का पैसा फंस गया है। हालात कब सामान्य होंगे, कहा नहीं जा सकता। काबुली चने से अफगानों का रिश्ता हो न हो, लेकिन ‘काबुली वाला’ कहानी के माध्यम से पठानो के भावुक चरित्र का एक हिस्सा हमारे जेहन में बसा हुआ है। यह वो किरदार है, जो जाहिल तालिबानियों से बिल्कुल उलट है। जो शायद अफगानिस्तान से आता भी नहीं है, वो चना काबुली बनकर हमारे पाकशास्त्र का अभिन्न हिस्सा बन गया है। और जो अफगानिस्तान से आती है, उस काबुली हींग के हालात भी कब बिगड़ेंगे, कहा नहीं जा सकता। हालांकि आम अफगानी आज भी भारत को चाहता है। उसे अपना दोस्त और मददगार समझता है।
यह भी अपने आप में दिलचस्प बात है कि एक दलहन चना ‘काबुली ‘नाम कैसे ओढ़ लेता है? उसका काबुल या अफगानिस्तान से भला क्या रिश्ता है? क्या यह वहां उगाया या खाया जाता है? इन सवालों का जवाब नकारात्मक ही है। अफगानी मुख्य रूप से मांसाहारी हैं और चावल ज्यादा खाते हैं। उनकी वेज डिशेज भी बहुत कम हैं। इसलिए चना चबेना खाने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में काबुली चने से बने स्वादिष्ट छोले उनके लिए विदेशी ही हैं। तो फिर इस चने को ‘काबुली’ नाम किसने और क्यों दिया?
इसके बारे में कहानी बताई जाती है कि भारत मे इसका आयात उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के इलाकों से काबुल के मार्फत 18 वीं सदी में शुरू हुआ। भारत में अफगान (पठान) इसे लेकर आते थे। सो लोग इसे काबुली चना कहने लगे। मानकर कि हर पठान काबुल से ही आता है। अलबत्ता यह जरूर है कि काबुली चना (जिसे अंग्रेजी में चिकपी कहते हैं) की खेती साढ़े 9 हजार साल पहले मध्य एशिया में शुरू हुई। लेकिन अब यह मुख्य रूप से भारतीय फसल है। हम ही दूसरे देशों को काबुली चना निर्यात करते हैं, वो काबुल से दिल्ली नहीं आते। काबुली चने को हम चना मसाला, छोले, भुने चने अादि के रूप में खाते हैं। रसरंजन की महफिलों में ‘नमकीन’ के रूप में भी काबुली चना जगह पाता रहा है। काबुली चने की कई किस्में हैं। स्वाद में अमेरिकी और ईरानी काबुली चना भारतीय काबुली चने की तुलना में ज्यादा मीठा बताया जाता है। हालांकि हमारा देशी चना भी काबुली चने की टक्कर का है। वैसे काबुली चना देसी चने के मुकाबले आकार में बड़ा और वजन में हल्का होता है। पौष्टिकता की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि काबुली चना प्रोटीन से भरपूर होता है।
काबुली चने के साथ-साथ हमारे यहां काबुली हींग भी बेहद मशहूर रही है। हींग का पौधा मुख्य रूप से मध्य एशिया के शुष्क मौसम वाले देशों में होता है। यह पहाड़ों पर उगता है ( अब इसकी खेती भारत में भी होने लगी है)। इससे निकलने वाले रस से हींग बनती है, जो हमारे शाकाहारी खानों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आजादी के पहले अफगानिस्तान से पठान अपने साथ सूखे मेवों के साथ शुद्ध और तीखी गंध वाली हींग भी लेकर आते थे। सो काबुली हींग की आज भी वैसी ही मांग है। माना जा रहा है कि तालिबानी सत्ता के चलते वहां से हींग के आयात पर भी असर पड़ेगा।
दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स के मामले में अमीर है। सूखे मेवे का उत्पादन और निर्यात अफगानिस्तान की अर्थ व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। भारत भी अफगानिस्तान से पिस्ता, अखरोट, अंजीर, बादाम, चेरी, गोंद आदि बड़े पैमाने पर मंगवाता रहा है। पहले दोनो देशों के बीच व्यापार व्हाया पाकिस्तान सड़क मार्ग से होता था। आजकल यह दुबई के मार्फत होता है। लेकिन यह लंबा रूट है।
सड़क मार्ग के व्यापार में पाकिस्तान द्वारा बार बार अड़ंगे डाले जाने के बाद मोदी सरकार ने 2017 में सीधे विमान से व्यापारिक उड़ाने शुरू कर दी थीं,जिसके फलस्वरूप भारत-अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी बढ़ गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ो के मुताबिक 2020 21 में दोनो देशों के बीच व्यापार 103 अरब रू. का था। हालांकि यह भारत के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि हम अफगानिस्तान को निर्यात काफी अधिक करते हैं, बजाय आयात के। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है मेवे की यह महंगाई खुद व्यापारियों द्वारा बढ़ाई हुई है। सप्लाई सुधरने पर रेट फिर गिरने लगेंगे।
बहरहाल, अफगानी काबुली चना खाते हों न खाते हों, खुद हींग का भरपूर इस्तेमाल करते हों न करते हों, लेकिन काबुल और प्रकारांतर से अफगान (पठान) हमारी संस्कृति में कहीं रच गए हैं। यह कहावत तक हिंदी में रूढ़ हो गई कि ‘क्या काबुल में गधे नहीं होते?’ यानी काबुल में सिर्फ घोड़े ही नहीं होते, गधे भी होते हैं। यह कहावत शायद तब बनी थी, जब काबुल में तालिबानी नहीं हुआ करते थे। आज वो वहां की औरतों के साथ जो भी सलूक कर रहे हों, कवीद्र रवींद्रनाथ टैगोर ने सवा सौ साल पहले एक अफगान की संवेदनशीलता उसके वात्सल्य में बूझी, जो अपनी झोली में से पिस्ते-बादाम-िकशमिश निकाल कर कोलकाता की नन्हीं मिनी को दिया करता था। मिनी भी उसे ‘काबुली वाले काबुली वाले’ कहकर बुलाया करती थी। मिनी के लिए काबुली वाले की झोली ‘जादू का पिटारा’ थी। एक बार काबुली वाले ने उधार के पैसे न मिलने पर तैश में एक ग्राहक को चाकू मार दिया। उसे सजा हुई। काबुली वाला आठ साल बाद जेल से छूटा तो उसकी आंखें फिर उसी नन्हीं मिनी को खोजने लगीं। तब तक मिनी बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी होने वाली थी। मिनी को दुल्हन के भेस में देखकर पठान मिनी के पिता से कहता है कि साहब अपनी बेटी को याद करके आपकी बिटिया के लिए थोड़ा सा मेवा लाया था। उसे दे दीजिएगा। मैं यहां सौदा बेचने नहीं आता…। अफसोस इस बात का कि उसी काबुली वाले के देश में आज धर्म के नाम सत्ता का सौदा हो रहा है।