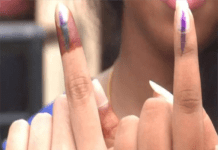ओडीशा के जाजपुर जिले का एक ब्लॉक है सुकिंदा. इसी ब्लॉक के तहत आता है नगडा गांव. इस गांव में आप जाएं तो आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा. लेकिन, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि तीन-चार महीनों के अंदर इस गांव में 19 बच्चों की मौत हो गई है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला? स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलीं या फिर कुपोषण से उनकी मौत हुई? कई सवाल आपके मन में कौंध जाएंगे. खाद्य सुरक्षा क़ानून, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा जैसे कई क़ानून, विकास की बातें और भारत बदल रहा है के तमाम दावों के बाद भी अगर किसी गांव में 19 बच्चों की मौत हो जाए, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे?
ओडीशा के जाजपुर जिले का एक ब्लॉक है सुकिंदा. इसी ब्लॉक के तहत आता है नगडा गांव. इस गांव में आप जाएं तो आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा. लेकिन, जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि तीन-चार महीनों के अंदर इस गांव में 19 बच्चों की मौत हो गई है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उन बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिला? स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलीं या फिर कुपोषण से उनकी मौत हुई? कई सवाल आपके मन में कौंध जाएंगे. खाद्य सुरक्षा क़ानून, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा जैसे कई क़ानून, विकास की बातें और भारत बदल रहा है के तमाम दावों के बाद भी अगर किसी गांव में 19 बच्चों की मौत हो जाए, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे?
फिलहाल, इस घटना के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक नगडा गांव के इन बच्चों को एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पोषण और स्वास्थ्य सेवा का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नहीं मिल पा रहा था. इस गांव का निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र आठ किलोमीटर की दूरी पर है. यह आंगनबाड़ी केंद्र 2007 में स्थापित किया गया था. लेकिन, सच्चाई ये है कि यह आंगनबाड़ी केंद्र कागज पर तो मौजूद है, लेकिन वास्तव में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है. यह आंगनबाड़ी केंद्र एक पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके में बनाया गया था. सवाल है कि जब ऐसी जगहों पर अधिकारी और कर्मचारी तक जाने से कतराते हैं, तो कोई गर्भवती महिला या छोटा बच्चा भला इस आंगनबाड़ी केंद्र तक जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकती है?
शिशुओं की मौत की खबर स्थानीय मीडिया में आने के बाद ओड़ीशा के ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन कर इस पूरे मामले की जांच की. इस टीम ने जुलाई में उक्त गांव का दौरा किया और जो तथ्य पेश किए, उससे पता चला कि इन शिशुओं की मौत किन वजहों से हुई. इस टीम में राइट टू फुड से जुड़े प्रदीप प्रधान, कलांडी मलिक, सुधीर मोहंती, अधिवक्ता, उड़ीसा हाईकोर्ट, आरटीआई कार्यकर्ता संजय साहू, देबेन्द्र कुमार राउत और इंद्रजीत शामिल थे. इस टीम के मुताबिक नगडा जुआंग जनजाति समूहों की बस्ती है.
यह गांव पहाड़ व जंगल से घिरा हुआ है. टाटा माइनिंग अस्पताल से यह करीब 20 किलोमीटर दूर है. गांव से जुड़ी कोई सड़क नहीं है. पहाड़ पर ट्रैकिंग कर ही यहां तक पहुंचा जा सकता है. यहां जुआंग जनजाति की कुल 250 लोगों की आबादी है. यहां से 15 किलोमीटर दूर टाटा का खनन ऑपरेशन चल रहा है. टीम ने पाया कि इस गांव के तकरीबन सभी लोग दुबले-पतले व कुपोषित हैं और उनका कद काफी कम है. 3 से 4 वर्ष के लगभग सभी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. वहां न तो आंगनबाड़ी केंद्र हैं और न ही गांव में कोई प्राथमिक स्कूल है.
टीम ने जांच में पाया कि गांव के लगभग सभी बच्चे कुपोेषण से पीड़ित हैं. आंगनबाड़ी केंद्र में चलने वाली ममता योजना के बारे में किसी भी महिला को कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें इस योजना के तहत कभी एक रुपया मिला था. इस गांव में चारों तरफ गंदगी पसरी है, पीने के पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है. स्नान और अन्य कार्यों के लिए गांव के लोग नदी के पानी का उपयोग करते हैं. टीम ने जब गांव के निवासियों से पूछा कि उन्हें खाने के लिए क्या मिलता है, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था. टीम को पता चला कि जुआंग जनजाति के इन लोगों को केवल चावल, प़ेडों की छालें व पत्तियां और नमक ही मिल पाती है. टीम ने कई घरों का निरीक्षण किया और पाया कि किसी भी घर में दाल, आलू, प्याज या तेल मौजूद नहीं था. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्त्योदय अन्न योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, जुआंग समेत सभी आदिम जनजातीय समूह प्रति माह 35 किलो चावल के हकदार हैं. लेकिन इस गांव में परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से चावल की मात्रा (प्रति माह प्रति व्यक्तिमात्र 5 किलो) निर्धारित की गई है. इस प्रकार चार सदस्यों के परिवार को पूरे महीने के लिए केवल 20 किलो चावल मिल रहा है. यदि इस परिवार को अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किया जाता, तो उन्हें 35 किलो चावल प्रति माह मिलता. अब, इस दोषपूर्ण सर्वेक्षण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा के तहत इस गांव में किसी को भी कोई काम पिछले कई वर्षों से नहीं मिला है. टीम को गांव में किसी के पास भी जॉब कार्ड नहीं मिला. जाहिर है, इस गांव में नरेगा के तहत अभी तक कोई काम ही शुरू नहीं हुआ है.
इस गांव के 19 शिशु पहले ही कुपोषण का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं. राज्य सरकार ने शुरू में इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या मानकर मामले को दबाना चाहा, लेकिन यहां आने के बाद पता चलता है कि यहां की असली समस्या कुपोषण है, जिसके लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. नगडा गांव में शिशु मृत्यु के लिए चिकित्सा उपचार की कमी, कुपोषण और भूख एक बड़ी वजह है. गांव में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में प्रशासन ने लापरवाही बरती है. गांव में आईसीडीएस कार्यक्रम बच्चों के लिए लागू ही नहीं की गई है. इस योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है. सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रम इन गांवों तक आते-आते दम तोड़ देते हैं.
ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ नगडा गांव की है. नियामगिरी के कुटिया कोंध जनजाति का भी बुरा हाल है. राइट टू फुड कैंपेन की इस फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कालाहांड़ी जिले में लांजीगढ़ ब्लॉक स्थित कुटिया कोंध जनजाति के इलाकों का भी दौरा किया. टीम ने लांजीगढ़ ब्लॉक में जुआंग जनजाति की आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, खान-पान की आदत, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की स्थितियों का आकलन करने के लिए दौरा किया. टीम त्रिलोचनपुर ग्राम पंचायत, जहां कुटिया कोंध जनजातियों का निवास है, वहां भी गई. यह क्षेत्र लांजीगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से 10 किमी दूर है. यह पंचायत नियामगिरी पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां हजारों करोड़ रुपए की बॉक्साइट अब भी सुरक्षित है. यहां ध्यान देने की बात है कि कुटिया कोंध जनजाति के लोगों ने बातचीत के दौरान वेदांता कंपनी की प्रायोजित माइनिंग ऑपरेशन पर भी अपने गुस्से का इजहार किया. वे नियामगिरी पहाड़ की सुरक्षा को लेकर दृढ़ संकल्प थे. टीम ने कुटिया कोंध जनजाति के कई गांवों का दौरा किया. पहाड़ की चोटी पर स्थित हर गांव में इस जनजाति के 8 से 10 परिवार के लोग रहते हैं. जनजाति की एक महिला सरपंच डर के कारण टीम से बात करने के लिए बाहर नहीं आई.
टीम की तथ्यपरक रिपोर्ट के मुताबिक खेमुन्डिपाडार गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में चार-पांच बच्चे दिखे, जबकि यहां बीस बच्चे केंद्र से जुड़े हैं. बच्चे बिना साग-सब्जी के घटिया क्वालिटी के चावल और पतली दाल खाते दिखे. केंद्र पर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं था और हेल्पर ही केंद्र चला रहा था. केंद्र पर कोई रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों की जानकारी मिल सके. कुटिया कोंध जनजाति के निवासियों ने बताया कि उन्हें ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कभी कोई रोजगार नहीं मिला. यहां तक कि वे जॉब कार्ड के नाम से भी अपरिचित थे. इन गांवों में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है. यहां का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है. बीजू पक्का गृह योजना व आईएवाई का बुरा हाल है. राज्य सरकार को इन योजनाओं के तहत पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद देनी थी. लेकिन तीन गांवों में सिर्फ दो मकान ही इस योजना के तहत बने दिखे. कुटिया कोंध जनजाति के विकास के लिए केंद्र सरकार की मदद से 1986 में विकास योजनाएं शुरू की गई थीं. केकेडीए ऑफिस जाने पर पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं आए हैं. एक मुख्य क्लर्क ने बताया कि केकेडीए योजना के अंतर्गत 16 ग्रामीणों को इसका लाभ मिला है. 30 साल बीत जाने के बाद भी कुटिया कोंध डेवलपमेंट एजेंसी, केकेडीए का लाभ सभी 21 ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचा है. भ्रष्टाचार, फंड के दुरुपयोग व बेहतर योजना के अभाव में कुटिया कोंध जनजाति का विकास संभव नहीं हो सका है. सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका है. अन्त्योदय योजना और फुड सिक्योरिटी के बावजूद उन्हें आवश्यकता से कम चावल दिया जाता है, जिसके कारण वे आम की गुठली और पेड़ की छाल खाकर गुजर-बसर करने को मजबूर हैं. कृषि और हार्टिकल्चर संबंधी सुविधाओं के अभाव में किसान परंपरागत तरीके से पोडू और कुछ मोटे अनाज का उत्पादन करने को मजबूर हैं.
जिला प्रशासन ने 2004 में राज्य सरकार से अनुरोध किया कि सभी कुटिया कोंध जनजाति के 21 गांवों को केकेडीए योजना में शामिल कर लिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है. इस फैैैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी तरफ से सिफारिश की है कि कुटिया कोंध के सभी परिवार को प्रत्येक महीने अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम चावल दिया जाए. जनजाति समूह को भूख से बचाने के लिए राज्य सरकार सर्वे कराए कि प्रत्येक परिवार को कितने चावल और अन्य अनाज की जरूरत है और उस आधार पर अनाज दिए जाएं. आंगनबाड़ी केंद्र खुलें और बच्चों को सभी सुविधाएं दी जाएं. जिला स्तर पर उनके मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए. आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने, अनाज वितरण और फंड के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. केकेडीए योजना के तहत जनजाति के लोगों को सुविधा प्रदान की जाए और विस्तृत विकास योजना चलाकर कृषि और फूलों की खेती के अत्याधुनिक तरीकों को शुरू किया जाए. चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में बच्चे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. रोड सुविधा के अभाव में वे अस्पताल नहीं पहुंच पाते. दो या तीन दिनों के अंतराल में यहां के लोगों को मोबाइल अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए. बेहतर सड़क सुविधाओं का नहीं होना यहां की सबसे बड़ी समस्या है. जिला प्रशासन इसके लिए जल्द कदम उठाए. लेकिन, क्या ओड़ीशा सरकार इस फैैक्ट फाइंडिंग टीम की सिफारिशों पर ध्यान देगी?