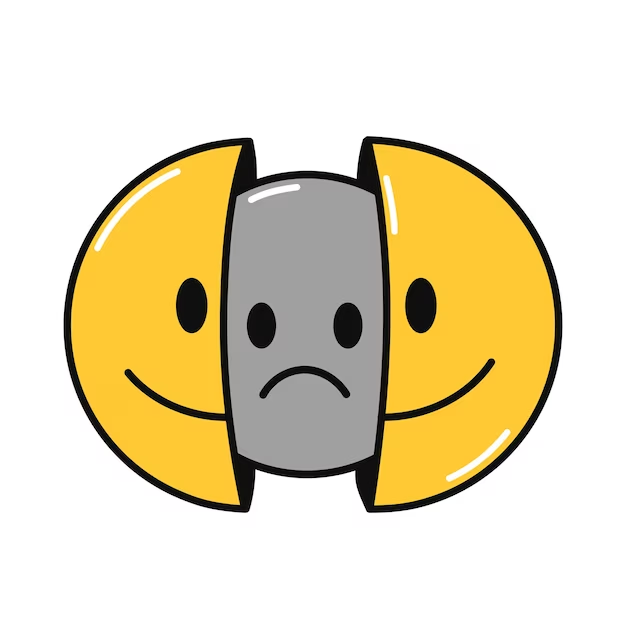राजा बड़ा या विद्वान- अपने देश में यह सवाल बहुत पुराना है और इसका जवाब बड़ा ही जाहिर! हजार साल पुरानी किताब ‘हितोपदेश’ कहती है कि बड़ा तो विद्वान को ही माना जायेगा क्योंकि राजा सिर्फ अपने देश में पूजा के काबिल माना जाता है जबकि विद्वान की पूजा चहुंओर होती है- स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते!
लेकिन विद्वान को राजपद मिले या राजा विद्वता हासिल करे- यह एक मंगल-कामना भर है. इस मंगल कामना की सच्चाई भी जगजाहिर है. अब हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित को ही लीजिए. वे विद्वान थे लेकिन राजा नहीं. उनकी विद्वता को आश्रय तो बंगाल के राजा धवलचंद्र ने दिया- धवलचंद्र के दरबारी कवि थे वे!

विद्वान को राजा से बड़ा ठहराने वाले हितोपदेश के रचयिता की सच्चाई उसकी मंगलकामना के एकदम उलट है. जगजाहिर सच्चाई यह है कि राजा का राजकोष पर अधिकार होता है, सो सारे गुणवान आखिरकार ताबेदारी तो उसी की करते हैं. राजनीति के सबसे पुराने सिद्धांतकारों में शुमार चाणक्य के यहां इस कड़वी सच्चाई का स्वीकार मिलता है, वर्ना वे यह ना लिखते कि सारे गुण आखिर को धन की शरण में जाते हैं- ‘सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते.’
चाणक्य ने बड़ी तल्खी से नोट किया है कि जिसके पास धन है वही कुलीन कहलाता है ; वही पण्डित, बहुश्रुत, गुणों की पहचान रखनेवाला, वक्ता तथा दर्शनीय समझा जाता है—‘यस्यास्ति वित्तं स नर:कुलीन:, स पण्डित: स श्रुतवान् गुणज्ञ:, स एव वक्ता स च दर्शनीय…’
जब एक इतिहास बना
लेकिन जगजाहिर सच्चाइयां कभी-कभी एकदम से उलट जाती हैं और इतिहास बदल जाता है. पुराने भारत की मंगल-कामना नये भारत में साकार हुई, दुनिया ने देखा कि एक विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक की धरती रही भारतभूमि पर खड़े नये राष्ट्र-राज्य का प्रधान बना!

जी हां, आपने ठीक पहचाना कि 14 मई 1962 के दिन एक इतिहास बना- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने.
गरीब ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था डॉ. राधाकृष्णन का. पिता की ख्वाहिश बस इतनी सी थी कि बेटा पढ़-लिखकर जल्दी से गांव के मंदिर का पुजारी हो जाए. पिता की कामना पूरी हुई लेकिन कई गुणा विस्तार लेकर. डॉ. राधाकृष्णन पश्चिम की दुनिया में ‘पूरब का भाष्यकार’ कहलाये. विद्वानों की मंडली में कभी उन्हें ‘पश्चिम और पूरब के बीच का पुल’ कहा गया तो कभी ‘हिंदू धर्म का श्रेष्ठ व्याख्याता’.
बर्ट्रेंड रसेल और दार्शनिक राजा का मुहावरा
अपने वक्त के सबसे कुशाग्र दार्शनिकों में एक गिने गए बर्टेंड रसेल ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति नियुक्त होने की अहमियत तो नोट करते हुए लिखा, ‘दर्शनशास्त्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने हैं और एक दार्शनिक के रूप में मुझे इसकी खास खुशी हो रही है. प्लेटो की इच्छा थी कि दार्शनिक को राजपद मिले और भारत को बड़भागी माना जाएगा जो उसने एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाया है.’
क्या रसेल ऐसा कहते वक्त प्लेटो के रिपब्लिक में आये सुकरात के इस कहे को याद कर रहे थे कि- ‘जब तक दार्शनिक राजा बनकर शासन नहीं चलाते या फिर जिन्हें आज के वक्त में राजा कहा जाता है वे ठीक-ठीक चीजों को ज्ञान की रोशनी में नहीं देखते यानी जब तक सियासत की ताकत और ज्ञान की ताकत में एका कायम नहीं हो जाता तब तक हमारे नगर-राज्यों को बुराइयों से निजात नहीं मिल सकती..ना तो घरों में कोई खुशी हो सकती है ना ही चौपालों पर…’
डॉ. राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने पर बर्ट्रेंड रसेल प्लेटो के दार्शनिक राजा का मुहावरा याद करते हुए क्या सोच रहे थे यह कहना मुश्किल है. लेकिन एक बात पक्की है कि बतौर राष्ट्रपति भारत की तरफ से दुनिया को देने के लिए डॉ. राधाकृष्णन के पास एक संदेश था और यह संदेश कोई भारतीय दार्शनिक ही गढ़ सकता था कि जब तक आप अध्यात्म की राह पर ना चलोगे तब तक बुराई से निजात नामुमकिन है!
बात कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी लगे तो यहां आप याद कर सकते हैं कि उनकी लिखी शुरुआती किताबों में एक का नाम ही है- ‘ऐन आयडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ’ यानी एक आदर्शवादी की जीवन-दृष्टि.
एक भारत प्रेमी दार्शनिक
अध्यात्म की राह पर चलकर ही बुराइयों का खात्मा हो सकता है- आदर्श से लबरेज इस अकीदे तक डॉ राधाकृष्णन कैसे पहुंचे होंगे इसके कुछ कयास लगाए जा सकते होंगे. दरअसल डा. राधाकृष्णन का दर्शन-प्रेम और भारत-प्रेम दो अलग-अलग चीज नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आगे बढ़कर यह भी कह सकते हैं कि अपने भारत-प्रेम में ही वे दार्शनिक हुए.
1909 में एमए करने के बाद मद्रास प्रसिडेंसी कॉलेज में दर्शनशास्त्र का व्याख्याता नियुक्त होने से लेकर 1929 में ऑक्सफोर्ड के हैरिस मैन्चेस्टर कॉलेज में प्रिंसिपल का पद संभालने तक डॉ. राधाकृष्णन ने देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का ओहदा संभाला, भारतीय दर्शन के व्याख्याता के रूप में जगत-प्रसिद्ध हुए.
एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलाम भारत के इस रोशनख्याल दिमाग का लोहा ब्रिटिश साम्राज्य को भी मानना पड़ा. 1931 में किंग जार्ज ने शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. राधाकृष्णन के योगदान को स्वीकार करते हुए नाइटहुड की उपाधि से नवाजा.
लेकिन यह वह वक्त था जब देश की आजादी का आंदोलन अपने परवान चढ़ चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य के सारे अलंकरण देशभक्त हिंदुस्तानी लौटाने लगे थे. डॉ. राधाकृष्णन भी आजादी के आंदोलन के दौर की इसी राह पर चले, उन्होंने नाइटहुड की यह उपाधि लौटा दी.
हां, डॉक्टरेट की उपाधि का सूचक डॉक्टर अपने नाम के साथ जोड़े रखा और इसकी वजह का अनुमान लगाना आसान है. यह उपनिवेश बसाने के ख्याल से तैयार किए गए अंग्रेजों के भारत सबंधी ‘ज्ञानकांड’ से बतौर हिंदुस्तानी उनकी वैचारिक लड़ाई का पता देता है.
डॉ. राधाकृष्णन को जिस पहली किताब(1908) ने दुनिया में मशहूर बनाया उसका नाम है ‘द ईथिक्स ऑफ वेदांत एंड इट्स मैटेरियल प्रिसपोजिशंस.’ बस बीस साल की उम्र थी उनकी इस किताब के प्रकाशन के वक्त और किताब एम.ए. के दौरान लिखी जाने वाली थीसिस का ही सुथरा रूप थी. किताब भारत को वैचारिक रूप से गुलाम रखने के उपनिवेशवादी ज्ञानकांड के खिलाफ लिखी गई थी.
अंग्रेज हिंदुस्तानी के धर्म और दर्शन में खोट निकालने के लिए कहते थे कि भारत में हमारे आने से पहले कभी भी कायदे का कोई राज कायम नहीं हुआ क्योंकि इनका धर्म और दर्शन या तो इन्हें पाप (मूर्तिपूजा) सिखाता है या फिर पूरे संसार को ही एक ‘लीला’ या फिर ‘माया’ यानी झूठा बताता है.
राधाकृष्णन ने अपनी पहली ही किताब में अंग्रेजों के इस ज्ञानकांड को अपने निशाने पर लिया. साबित किया कि शंकराचार्य के वेदांत को ठीक-ठीक नहीं समझा गया. वेदांत के हिसाब से दुनिया माया नहीं बल्कि सत्कर्म करने की जगह है, नैतिकता के पालन के साथ जीवन-निर्वाह करने की जगह!
आगे चलकर इस किताब को याद करते हुए उन्होंने लिखा- ‘ईसाई आलोचकों की चुनौती के मद्देनजर मैं हिंदू धर्म के अध्ययन की ओर मुड़ा और पता किया कि उसमें क्या जीवंत है और क्या मृत…मैंने वेदांत की नैतिक पक्ष पर एक थीसिस तैयार की, वेदांत पर आरोप था कि उसमें तो नैतिकता के लिए कोई जगह ही नहीं है और यह थीसिस इसी आरोप का जवाब थी.’
भारत की संस्कृतियों का एक दूत
राधाकृष्णन राजनीति में सीधे-सीधे नहीं आए बल्कि यह कहना ठीक होगा कि बुलाए गए थे. उनकी विद्वता की अंतरराष्ट्रीय धाक को देखते हुए 1946 में उन्हें यूनेस्को में भारत का दूत बनाया गया और 1949 में पंडित नेहरू ने डॉ. राधाकृष्णन को तत्कालीन सोवियत संघ का राजदूत नियुक्त किया.
इसका भी एक किस्सा है. सोवियत संघ में भारत की पहली राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित (नेहरू की बहन) थीं. सोवियत रुस के तत्कालीन प्रमुख जोसेफ स्टालिन ने उनसे भेंट करने से इनकार कर दिया था. अपनी ताकत के गरूर में चूर स्टालिन को लगा कि विजयलक्ष्मी पंडित का बात-बरताव शाहाना है और वो दंभी हैं. स्टालिन के इस रवैये से विजयलक्ष्मी पंडित का दायरा सोवियत संघ में भारतीय दूतावास तक ही सिमटा रहा.
पंडित नेहरू ने स्टालिन के रवैये की काट निकाली और डॉ. राधाकृष्णन को सोवियत संघ को राजदूत बनाया. सोवियत रुस में साहित्यकारों और दार्शनिकों की हमेशा से धूम रही है. जिक्र मिलता है कि डॉ. राधाकृष्णन की नियुक्ति के वक्त उनके दार्शनिक होने की बात सोवियत संघ में खूब उछली. नियुक्ति के बाद मास्को के राजकीय दायरों में चर्चा चल निकली कि ‘हिंदुस्तान से एक ऐसा दार्शनिक राजदूत बनकर आया है जो बस दो घंटे सोता है और दिन-रात बिना थके दर्शन के ग्रंथों को पढ़ते रहता है.’
इस चर्चा ने ऐसा रंग जमाया कि स्टालिन आखिरकार 1950 में डॉ. राधाकृष्णन से निजी भेंट के लिए तैयार हो गए. यह बात मायने रखती है क्योंकि नियुक्ति के वक्त स्टालिन की सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन से कहा था कि अपने कागजात हमारे उप विदेशमंत्री को सौंपिए, जबकि चलन यही है कि राजदूत अपनी पहचान के कागजात राष्ट्राध्यक्ष को सौंपते हैं.
राधाकृष्णन की कोशिशों से ही सोवियत संघ से भारत की शुरुआती नजदीकी कायम हुई. वे दिन दुनिया के मुल्कों को पूंजीवादी और साम्यवादी खेमे में बांटते शीतयुद्ध की शुरुआत के थे और स्टालिन नेहरू की गुटनिरपेक्षता की पहल को शक की नजर से देखते थे.
सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में डॉ. राधाकृष्णन की नियुक्ति अनायास नहीं थी. दरअसल उस वक्त पूंजीवादी और साम्यवादी देशों की आपसी लड़ाई से अलग बीच का रास्ता अपनाते हुए नई मिली आजादी के नए मायने तलाशते भारत जैसे देश के लिए डॉ. राधाकृष्णन से बेहतर राजदूत शायद ही कोई हो. वे राजदूत तो थे ही भारत के संस्कृति-दूत भी थे.
संविधान-सभा में डॉ. राधाकृष्णन
दो ध्रुवों में बंटती दुनिया में एक आजाद मुल्क के रूप में भारत अपनी संस्कृति का कौन-सा संदेश लेकर जाए? यह आजादी के आंदोलन का एक बड़ा प्रश्न था, बड़ा इसलिए कि यह सवाल भारत की पहचान से जुड़ा है. मुल्कों की बिरादरी अपने में शामिल करने से पहले किसी देश को तौलना चाहती है कि आखिर युद्ध और शांति, प्रेम और घृणा जैसे सनातन सवालों पर वह क्या सोचता है?
अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हमारे मुल्क ने इस सवाल का जवाब तैयार कर लिया था. और, दुनिया के नाम भारत का यह संदेश डॉ. राधाकृष्णन से ज्यादा बेहतर लफ्जों में शायद कोई तैयार भी नहीं कर सकता था. वाकया उस वक्त का है जब संविधान-सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना.
इस दिन डॉ. राधाकृष्णन ने संविधान-सभा में बोलते हुए मानो भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा की. कहा कि ‘कोई राष्ट्र नस्ल, भावनाओं के ज्वार या पुराने वक्त की किसी याद पर निर्भर होने से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है सदियों से चली आ रही किसी जीवनशैली को बुनियाद बनाकर और ऐसी एक जीवनशैली हमारी धरती की आत्मा रही है…यह जीवनशैली उतनी ही पुरानी है जितना कि गंगा का पानी या हिमालय की बर्फ और सिंधुघाटी की सभ्यता के शुरुआती वक्त से आज दिन तक लगातार चली आई है…यह जीवनशैली हमारी धरती पर हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है और मुसलमानों की भी…हां हम सदियों से करुणा और उदारता की राह पर चले हैं.’
इस सिलसिले में उन्होंने महात्मा बुद्ध को याद किया और सम्राट अशोक को भी और कहा कि ‘जब बुद्ध के महान शिष्य ने देखा कि उसके साम्राज्य में सभी धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं तो उसके मुंह से निकला- ‘समवाय एव साधुः’ यानी समन्वय का रास्ता ही सबसे अच्छा है!’
तकरार नहीं प्यार- यह दुनिया को भारत का संदेश है, इसकी व्याख्या करते हुए उस दिन (11 दिसंबर 1946) डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था- ‘भारत एक सिम्फनी का नाम है, बिल्कुल किसी आर्केस्ट्रा की तरह जहां हर साज अपने अलग-अलग सुर और स्वर में बोलते हैं लेकिन समवेत सुर और स्वर मिलने पर धुन एक बजा करती है. हमारा देश ऐसे ही हेल-मेल का प्रतीक है. इसने कभी यातना-गृह नहीं बनाये. इसने नहीं कहा शरण लेने आए पारसियों, यहूदियों या ईसाइयों और मुसलमानों से कि अपना अकीदा बदलो और एकसार हिंदू पहचान में समाहित हो जाओ.
भारत ने कभी ऐसा नहीं किया. जियो और जीने दो- इस देश का यही अकीदा रहा है. अगर हम अकीदे के सच्चे हैं, अगर यह अकीदा पांच-छह हजार साल से लगातार यहां चला आ रहा है और अब भी कायम है तो इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि हम आज के संकट से भी उसी तरह पार लेंगे जैसे इतिहास के पिछले अनगिनत संकटों से हमने पार पाया है.’
आगे इसमें यह भी जोड़ा कि ‘हेल-मेल का यह भाव ही हमारी असली आध्यात्मिक पूंजी है, यही हमारी आत्मा है और आत्मा को खोकर सिर्फ देह बचाना सबसे बड़ा पाप है. अगर हम अपने अध्यात्म की इस पूंजी के साथ खड़े हुए, अगर हमने अपनी इस आत्मा को बचाया तो निश्चित ही एक आजाद और अटूट भारत बनाने के हमारी कोशिशों को गति मिलेगी.’
जब जंग से सामना हुआ…
डॉ. राधाकृष्णन के राष्ट्रपति रहते भारत दो युद्धों की आग से गुजरा. ये युद्ध एक तरह से विश्व के नाम भारत के संदेश को चुनौती के समान थे.
चीन का आक्रमण पंचशील के सिद्धांत पर आघात था तो पाकिस्तान का हमला हेल-मेल के हमारे सांस्कृतिक विश्वास पर आघात.
डॉ. राधाकृष्णन के लिए भी ये दोनों युद्ध अपने निजी विश्वास पर आघात की तरह थे. विश्वास-भंग की इस घड़ी में दायित्व-निर्वाह का सवाल सबसे पहला था.
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है और अपनी इस भूमिका निर्वाह करते हुए डॉ. राधाकृष्णन ने बड़ी मजबूत आवाज में राष्ट्र से कहा, ‘चीनियों के पास संख्या बल ज्यादा है और लड़ाई दुर्गम ठिकानों पर लड़नी पड़ी है इसलिए हमारी फौजी ताकत को नुकसान उठाना पड़ा है. हालात की नई सच्चाइयों ने हमें आगाह किया है, हम आज की जरूरत और भविष्य की मांग को देखते हुए तैयार हैं, देश में नया संकल्प जगा है, उसमें नई इच्छा-शक्ति जगी है.’
1965 में पाकिस्तान ने देश की पश्चिमी सीमा पर हमला बोला और सेना के सर्वोच्च कमांडर के रुप में डॉ. राधाकृष्णन ने 25 सितंबर 1965 के दिन राष्ट्र को जो संदेश दिया वह आज पाकिस्तानी की साजिशों को देखते हुए पहले की तरह मौजूं है.
डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था, ‘पाकिस्तान समझता है, भारत बड़ा कमजोर है, बहुत भयभीत है या फिर इतने गरूर में हैं कि जंग में उसका सामना नहीं कर सकता. बेशक भारत को स्वाभाविक तौर पर हथियार उठाने से परहेज रहा है लेकिन जब उसपर हमले हुए हैं तो उसने अपनी हिफाजत की है. पाकिस्तान यह भी मान बैठा है कि भारत में सांप्रदायिक परेशानियां उठ खड़ी होंगी और ऐसी आपा-धापी में उसे अपना मनमाना करने का मौका मिल जाएगा. पाकिस्तान की इस खामख्याली को आज जरूर ही तेज झटका लगा होगा.’
हर हाल में शिक्षक
वे दार्शनिक थे, दुनिया के धर्मों के व्याख्याता और भारत की संस्कृति के दूत भी! सेना के सर्वोच्च कमांडर के रुप में उन्होंने देश की दो जंगों में अगुवाई की लेकिन इन सारी भूमिकाओं के निर्वाह के बीच उनका मन अपने को शिक्षक ही मानता रहा.
राष्ट्रपति पद पर रहते उनसे इसरार किया गया कि आपका जन्मदिन मनाया जाय लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि अगर सम्मान ही करना है तो देश के शिक्षकों का करो. वे मानते थे कि जो सबसे ज्यादा मेधावी है, उसे शिक्षक बनना चाहिए. उनका अपना जीवन उनके इसी विश्वास का प्रमाण है.
कृतज्ञ राष्ट्र इस ‘भारत-रत्न’ का जन्मदिन (5 सितंबर) शिक्षक-दिवस के रूप में मनाते हुए सोचता है क्या हमारा दार्शनिक राजा लोकतंत्र को भी एक शिक्षा ही मानता था? शायद हां, क्योंकि डॉ. राधाकृष्णन ने लोकतंत्र को जीवन जीने की शैली का दर्जा दिया है जिसमें ‘राजकाज शांति और सुलह से चलाया जाता है, जिसमें बदलाव शांतिपूर्वक होते हैं और बुनियादी सुधार अहिंसक आंदोलन के जरिए!’