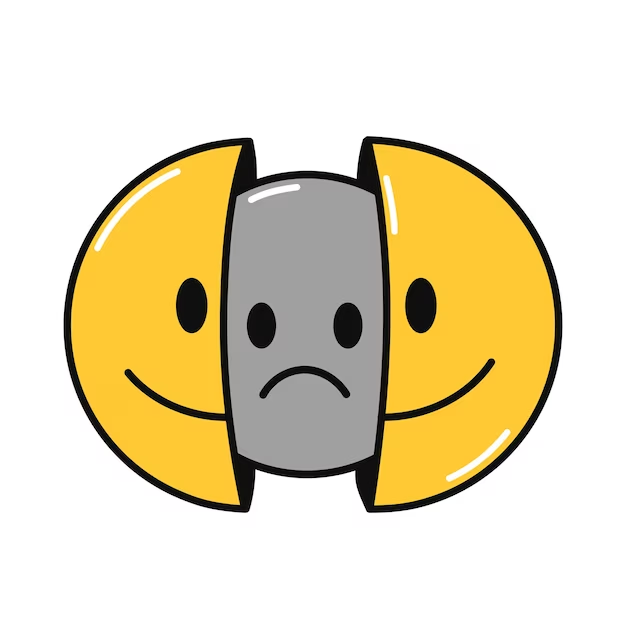महाराष्ट्र के पालघर जिला के कलेक्टर के दफ्तर के सामने 1,500 अनुसूचित जनजाति के किसानों ने वन अधिकार कानून के तहत ज़मीन पर अपना अधिकार हासिल करने के लिए विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया. इन किसानों ने कलेक्टर के दफ्तर के सामने लंबी लाइन बना कर सत्याग्रह की शुरुआत की. इन किसानों ने वर्ष 2013 में आरटीआई (सत्याग्रह) का इस्तेमाल कर वन अधिकार अधिनयम (एफआरए) 2006 के तहत मिलने वाले अपने अधिकारों की जानकारी हासिल की थी.
महाराष्ट्र के पालघर जिला के कलेक्टर के दफ्तर के सामने 1,500 अनुसूचित जनजाति के किसानों ने वन अधिकार कानून के तहत ज़मीन पर अपना अधिकार हासिल करने के लिए विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया. इन किसानों ने कलेक्टर के दफ्तर के सामने लंबी लाइन बना कर सत्याग्रह की शुरुआत की. इन किसानों ने वर्ष 2013 में आरटीआई (सत्याग्रह) का इस्तेमाल कर वन अधिकार अधिनयम (एफआरए) 2006 के तहत मिलने वाले अपने अधिकारों की जानकारी हासिल की थी.
उन आरटीआई के जरिए इन्हें पता चला था कि एफआरए के तहत जो ज़मीन इन्हें मिली है, वो इनकी जोत की ज़मीन से बहुत कम है. शिकायत के बाद 60 दिन के भीतर आवंटित ज़मीन की दुबारा माप करनी थी. लेकिन किसानों का कहना है कि तीन साल तक इंतज़ार करने के बाद भी अब तक जमीन की माप नहीं हुई. इन किसानों का यह भी कहना है कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है, तो अब लाइन में खड़े हो कर हमने सत्याग्रह शुरू किया है.
इस सत्याग्रह में शामिल होने वाले किसानों में से ज्यादातर किसान 2013 में आयोजित आरटीआई सत्याग्रह में भी शामिल थे. आरटीआई द्वारा हासिल जानकारियों से यह पता चलता है कि सरकारी तंत्र आरटीआई के प्रावधानों की कैसे धज्जियां उड़ाता है. दरअसल, वन विभाग ने बिना सत्यापन के कम ज़मीन देने की अनुशंसा कर दी थी, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति और सब डिवीज़न लेवल समितियों ने आवेदक को सूचित किए बिना ही स्वीकार कर लिया था.
जबकि नियमानुसार ग्राम सभा की सहमती के बिना किसी को ज़मीन आवंटित नहीं किया जा सकता था. आरटीआई सत्याग्रह के बाद राज्य सीआईसी ने यह आदेश दिया था कि एफआरए के तहत आवंटित ज़मीन की सभी जानकारियां जिला अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएं. बहरहाल, 2013 में दाखिल अपील के बाद भी अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है. जनजातियों को अपने उन अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो उन्हें बिना किसी लाग लपेट के मिल जाना चाहिए था.
दरअसल, यह स्थिति केवल महाराष्ट्र के पालघर जिले की ही नहीं है, एफआरए के कार्यान्वयन के मामले में देश के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है. कई जगह तो स्थिति और भी ख़राब है. एफआरए को पारित हुए दस साल बीत चुके हैं. किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए दस साल का समय बहुत होता है.
यहां तो मामला संवैधानिक है, लेकिन इसके बावजूद समाज के सर्वाधिक वंचित समूहों के प्रति सरकारों का रवैया न केवल बहुत ही लचर, टाल-मटोल करने वाला या सिरे से नज़रंदाज़ करने वाला है, बल्कि द्वेषपूर्ण भी है. सरकारों ने एफआरए को कमज़ोर करने का कोई भी मौक़ा हाथ से जाने नहीं दिया है.
एफआरए के पारित होने के दस साल बाद वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के एक समूह (सीएफआर-एलए) ने एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में जो नतीजे ज़ाहिर किए गए हैं, उनसे यह साबित होता है कि सरकारें समाज के सबसे वंचित तबकों के लिए बड़े-बड़े वादे करती हैं, कानून भी पारित कर देती हैं, लेकिन खुद ही उन कानूनों की धज्जियां भी उड़ा देती हैं.
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 या वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. वरना क्या वजह है कि जिस कानून को पारित हुए दस साल बीत चुके हैं, उसका केवल तीन प्रतिशत ही अब तक कार्यान्वित किया जा सका है. हालांकि बीच-बीच में सरकारें इसके कार्यान्वयन पर अपनी पीठ थपथपा लेती हैं.
बहरहाल, एफआरए के तहत न्यूनतम अनुमानित वन क्षेत्र (पांच उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) लगभग 85.6 मिलियन एकड़ (34.6 मिलियन हेक्टेयर) है, जिसपर सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) का अधिकार मिल सकता है. इन वन क्षेत्रों के 1.70 लाख गांव में रहने वाले लगभग 20 करोड़ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (ओटीएफडी) के अधिकारों
को मान्यता देने का अनुमान है. लेकिन सीएफआर-एलए की रिपोर्ट के मुताबिक एफआरए के पारित होने के दस साल बाद भी वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकार नहीं दिए गए हैं. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोगों में से लगभग 19 करोड़ लोगों के अधिकारों का सम्मान अभी नहीं किया गया है.
ज़ाहिर सी बात है, इस स्थिति के लिए एक तरफ जहां केंद्र सरकार और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय ज़िम्मेदार हैं, वहीं राज्य सरकारें भी इसके लिए कम ज़िम्मेदार नहीं हैं. एक तरफ जहां ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आगे रहे हैं, वहीं असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे पीछे हैं.
एफआरए के क्रियान्वयन में आगे रहने वाले राज्यों की स्थिति भी कम दयनीय नहीं है. इसका अंदाज़ा महाराष्ट्र के पालघर जिले में चल रहे आंदोलन से लगाया जा सकता है. यहां आंदोलनरत अनुसूचित जनजाति के किसानों का आरोप है कि वन अधिकारियों ने मनमाने ढंग से और ग्राम सभा के सत्यापन के बिना ही जनजातीय किसानों को कम ज़मीन देने की अनुशंसा कर दी थी.
जबकि एफआरए के तहत इस मामले में ग्राम सभा की सहमती आवश्यक है. जब महाराष्ट्र का ये हाल है, तो जिन राज्यों में इस मामले में कोई काम नहीं हुआ, वहां के वनक्षेत्र में रहने वाले जनजातियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.
इस लचर सरकारी रवैये को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा. नवंबर 2016 में पीएमओ की तरफ से सात राज्यों को यह आदेश दिया गया कि सदियों से वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के अधिकार उन्हें वापस दिलाने में शीघ्रता बरतें. ये सात राज्य हैं- असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और झारखण्ड.
एक लम्बी लड़ाई के बाद सदियों से उपेक्षा के शिकार और अपने अधिकारों से वंचित, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए और इन क्षेत्रों में नक्सलवाद के असर को कम करने और वन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन योजना आयोग की अनुशंसा पर वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था.
लेकिन इसके क्रियान्वयन पर जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने अधिकार हासिल करने के लिए अभी और संघर्ष करना पड़ेगा. शायद सरकार के पास उनकी सुध लेने का समय नहीं है. हालांकि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित कर रखा है, लेकिन वो अब तक फिसड्डी साबित हुआ है. सरकारों ने न केवल एफआरए को लागू करने में विलम्ब से काम लिया है, बल्कि इसे कमज़ोर करने की कोशिश भी की है.
दो मंत्रालयों के बीच पत्राचार
चौथी दुनिया ने अपने 20 जून 2016 के अंक में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें एनडीए सरकार के दो मंत्रालयों के बीच हुए पत्राचार के हवाले से बताया गया था कि सरकार कैसे एफआरए के अंतर्गत आदिवासियों और वन में निवास करने वाले लोगों के अधिकार को छिनना चाहती है. यह पत्राचार जून 2015 और दिसंबर 2015 के दरम्यान जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुआ था.
इन पत्रों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि वन भूमि को किसी परियोजना के लिए आवंटित करने से पहले एफआरए के तहत उस क्षेत्र के ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है. जबकि पर्यावण मंत्रालय इस ग्राम सभा की सहमति के क्लॉज़ हटाने की बात कर रहा था. एफआरए की सहमति वाले क्लॉज़ को लेकर इन दो मंत्रालयों के बीच की रस्साकसी के दौरान केंद्र सरकार ने कैम्पा बिल पेश किया था, उस बिल में ग्राम सभा की सहमती का क्लॉज़ शामिल नहीं था.
वन अधिकार अधिनियम को कमज़ोर करने की साज़िश
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के एक क़ानून के मुताबिक उद्योग, कारखानों और दूसरे गैर-वन उपयोग के लिए काटे गए जंगलों के बदले नए पेड़ लगाने और कमज़ोर या क्षीण हो रहे जंगल को घना बनाने के लिए वन भूमि का उपयोग करने वाली कंपनियां और संस्थाओं को मुआवजे देना पड़ता है. वर्ष 2002 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 को लागू करने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिपण्णी की थी कि इस मद में जमा फण्ड या तो खर्च नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम खर्च हो रहा है.
इसी टिपण्णी के मद्देनज़र तत्कालीन यूपीए सरकार ने वर्ष 2008 में कैम्पा बिल पेश करने की कोशिश की थी, जिसे संसद की स्थाई समीति ने एफआरए के तहत ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों का हवाला देते हुए नामंज़ूर कर दिया था. बहरहाल, मौजूदा केंद्र सरकार ने कैम्पा बिल 2015 में पेश किया था, जिसे लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था.
लेकिन चूंकि राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इस बिल में एफआरए के तहत ग्राम सभा को दिए गए अधिकारों के अनुरूप ग्राम सभा की सहमती के क्लॉज़ को शामिल किया जाय. इस संबंध में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसोधन प्रस्ताव पेश किया था. इसके बाद पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने आश्वासन भी दिया कि विपक्ष द्वारा उठाई गई अपत्तियों को इस अधिनियम के तहत बनने वाले कानून में शामिल कर लिया जाएगा.
इस बिल में ग्राम सभा के क्लॉज़ को शामिल करने के लिए वन अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली देश भर की 45 सिविल सोसाइटी की संस्थाओं ने राज्यसभा को एक ज्ञापन भी दिया था. उनका कहना था कि इसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के उस प्रावधान को बेअसर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों एवं पारंपरिक रूप से वन में निवास करने वाले लोगों का वन के ऊपर अधिकार सुनिश्चित किया गया है.
वन अधिकार अधिनियम क्या है?
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 या वन अधिकार अधिनियम- 2006, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एक लंबी लड़ाई के बाद दिसंबर 2006 में पारित किया गया. यह कानून वन संसाधनों और वन क्षेत्र पर उन लाखों लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिन अधिकारों से यहां बसने वाले लोगों को सैकड़ों सालों से वंचित कर रखा गया. यह कानून पूरे भारत में वन भूमि और वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार देता है.
यह कानून 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था. इस कानून को, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर हो रहे ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने का एक बड़ा हथियार माना गया. वन अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद यह आशा की जा रही थी कि इससे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को भी मजबूती मिलेगी और लोगों के जीविका का मसला बहुत हद तक हल होगा, जिसे गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी. साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी और जो वन क्षेत्र हिंसा ग्रस्त हैं, वहां हिंसा में कमी आएगी.
इस अधिनियम के दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष ये हैं कि यह व्यक्तिगत संपत्ति के साथ-साथ सामूहिक संपत्ति का प्रावधान भी करता है. यह कानून सामुदायिक वन लगाने, उनकी रक्षा करने और उनके संरक्षण का अधिकार देता है. इसमें विस्थापित लोगों के अधिकार और वन क्षेत्र में विकास के कार्यों से संबंधित अधिकारों का भी प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
लेकिन पिछले दस वर्षों में इस अधिनियम को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है. इन कोशिशों में वर्ष 2016 में ग्राम सभा के क्लॉज़ के बिना कैम्प बिल का पारित होना और ग्राम सभा के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों के पत्राचार का लीक होना महत्वपूर्ण हैं.