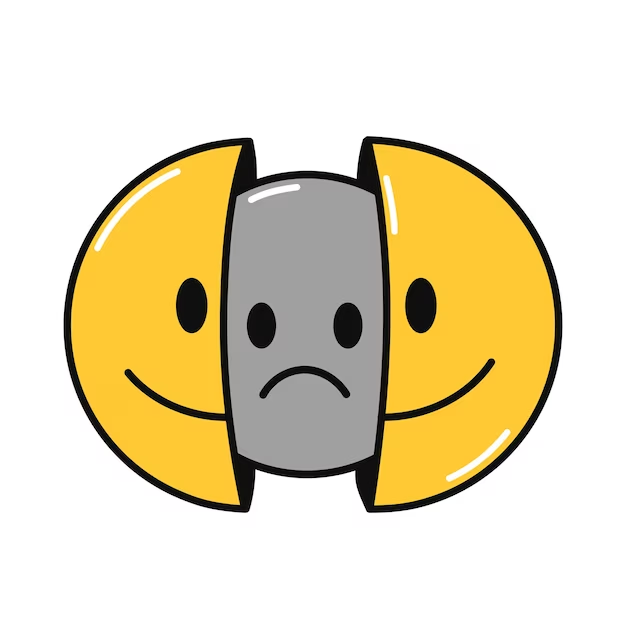भारतीय चुनाव काफी मजेदार होते हैं. इनमें स़िर्फ इतना ही मजेदार नहीं होता है कि अपने सबसे बेहतरीन रंगीन कपड़ों में शांति से लाइन में लगे सैकड़ों मतदाता मतदान के दौरान आपस में बातचीत करते हुए दिखते हैं, बल्कि चुनाव आयोग की भी प्रशंसा करनी होगी, जो उस काम को कुछ घंटों में आसानी से पूरा करा देता है, जिसे पूरा करने में इंग्लैंड और अमेरिका में कई दिन लग जाते हैं. जहां तक मुझे याद है, पिछली कई बार के मुकाबले इस बार का चुनाव ज़्यादा हो-हल्ले से भरपूर और क्रोधपूर्ण रहा. हालांकि इसमें एक-दूसरे के लिए घृणा जैसी कोई बात नहीं दिखी. एक प्रकार से यह ऐसा चुनाव है, जहां भारत कई तरह के मौलिक डरों का सामना कर रहा है. 3 जून, 1947 को भारत के बंटवारे पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही देश के मुसलमान एक विषम अवस्था में पड़े हुए हैं. वे एक संरक्षित अल्पसंख्यक समुदाय बनकर रह गए हैं, जिनके स्वघोषित अभिभावक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं.
भारतीय चुनाव काफी मजेदार होते हैं. इनमें स़िर्फ इतना ही मजेदार नहीं होता है कि अपने सबसे बेहतरीन रंगीन कपड़ों में शांति से लाइन में लगे सैकड़ों मतदाता मतदान के दौरान आपस में बातचीत करते हुए दिखते हैं, बल्कि चुनाव आयोग की भी प्रशंसा करनी होगी, जो उस काम को कुछ घंटों में आसानी से पूरा करा देता है, जिसे पूरा करने में इंग्लैंड और अमेरिका में कई दिन लग जाते हैं. जहां तक मुझे याद है, पिछली कई बार के मुकाबले इस बार का चुनाव ज़्यादा हो-हल्ले से भरपूर और क्रोधपूर्ण रहा. हालांकि इसमें एक-दूसरे के लिए घृणा जैसी कोई बात नहीं दिखी. एक प्रकार से यह ऐसा चुनाव है, जहां भारत कई तरह के मौलिक डरों का सामना कर रहा है. 3 जून, 1947 को भारत के बंटवारे पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही देश के मुसलमान एक विषम अवस्था में पड़े हुए हैं. वे एक संरक्षित अल्पसंख्यक समुदाय बनकर रह गए हैं, जिनके स्वघोषित अभिभावक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं.
अब भी मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक दर्जे की बात करना उन्हें देश का आम नागरिक बनने से रोकने जैसा है. ऐसा करना उन्हें इस बात की आज्ञा से भी रोकता है कि वे देश के अन्य नागरिकों की तरह अपने अधिकारों का आनंद उठा सकें. चाहे वह मुंबई में किराए का मकान लेने का मसला हो या फिर एकाउंटेंसी फर्म में हिस्सेदारी का, सभी जगह मुसलमानों की अवस्था एक जैसी है. मुसलमानों को लगता है कि वे देश के दोयम दर्जे के नागरिक हैं. अभी तक महाराष्ट्र की कोई भी सरकार इस बात के लिए आगे नहीं आई कि वह मुंबई में मुसलमानों को किराए का मकान दिलाने में मदद करे और न किसी को इस बात के लिए सजा दी गई कि वह मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहा है. राज्य सरकार ने कभी इस बात की अपील भी नहीं की कि मुसलमानों को नौकरी देने में भेदभाव न बरता जाए. इस बात का दु:खद रूप से आरक्षण कोई समाधान नहीं है. कई दशकों तक मुसलमानों की समस्या पर मुखर होकर कोई बात नहीं की गई. शायद यही वजह है कि अब सांप्रदायिक ताकतों ने इस मसले को भुनाना शुरू कर दिया है.
हालांकि इस बार चुनाव में ऐसे सारे भेदभाव मिट गए हैं. दशकों तक रुकी रहने वाली सारी परेशानियों को इस बार मजबूत ढंग से रखा गया. एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगे. कई बार तो आरोप लगाने वालों के लिए ही परेशानी खड़ी हो गई. भाजपा के घोषणापत्र की कांग्रेस ने आलोचना की, जबकि सांप्रदायिकता के मामले में दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों एक-दूसरे का प्रतिरूप हैं. अमित शाह अपने ही वक्तव्य में फंस गए. मामला ज़्यादा गंभीर इसलिए भी हो गया, क्योंकि वह बाद में उसे संभाल नहीं पाए. आजम खान ने शिकायत की कि करगिल युद्ध में मुसलमान सैनिकों के बलिदान की अनदेखी की गई. बहुत हद तक यह संभव भी हो सकता है, लेकिन यह शिकायत करने के लिए 15 सालों की देरी क्यों की गई? नरेंद्र मोदी को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए गुंडा कहा गया और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने की धमकी दी गई. मुख्तार अब्बास नकवी साबिर अली के साथ इस बात के लिए उलझ पड़े कि आख़िर भाजपा का अच्छा मुसलमान चेहरा कौन है?
प्रत्येक पार्टी दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और उसी दौरान खुद दागी लोगों को टिकट भी दे रही है. ऐसे दागी उम्मीदवारों के लिए आदर्श तर्क यह दिया जा रहा है कि जिसे सजा नहीं मिली, वह मासूम है. अन्य पार्टियों से आगे जाकर मोदी ने गुड गवर्नेंस और विकास की बात करते हुए अपने आपको सबसे बेहतरीन प्रत्याशी बताया है. वह कांग्रेस की हालिया विफलताओं के बारे में चर्चा और विकास की रफ्तार तेज करने की बात करते हैं. वह मंदिर मुद्दे या हिंदू-मुसलमान पर बातचीत करने से बच रहे हैं. उनके ऐसा करने से विरोधियों में गुस्सा भर रहा है, शायद इसी वजह से वे चुनाव क़रीब आने के साथ सांप्रदायिकता की बातें कर रहे हैं. भारतीय राजनीति के दबे हुए मुद्दे अब खुलकर सामने आ गए हैं. दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं. कांग्रेस यह आह भरती रही है कि मुसलमान ख़तरे में हैं. यह सांप्रदायिक है या धर्मनिरपेक्ष?
क्या भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को शंकराचार्य से यह अपील करनी चाहिए कि सभी हिंदू वोट भाजपा की तरफ़ जाएं? क्या अगर वह ऐसा करेंगे, तो जेल जाएंगे? कौन जाने क्या होगा और आख़िर कौन इस बात की चिंता करता है? मुख्य बात यह है कि क्या इन सब हथकंडों से वोट मिलेगा या नहीं? अगर वोट बैंक की बात की जाए, तो जाट अब आधिकारिक तौर पर ओबीसी मतदाता हो गए हैं. जल्दी ही हिंदू समुदाय में ब्राह्मणों के अलावा शायद ही कोई जाति ओबीसी कैटेगिरी के बाहर हो. आख़िर क्यों एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में हिंदुओं को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों को नहीं? क्या भारत को मंडल आयोग की सिफारिशें कूड़े में नहीं डाल देनी चाहिए और आरक्षण के लिए सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर सकारात्मक क़दम नहीं उठाने चाहिए?
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब 16 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, तो क्या उसके बाद 67 सालों से चल रहा मुसलमानों के साथ व्यवहार बदलेगा? क्या हिंदुओं के साथ व्यवहार बदलेगा? मंडल मानसिकता आज़ादी के बाद 42 सालों तक आर्थिक विकास ठहर जाने के कारण बढ़ी, क्योंकि समाजवादी आर्थिक नीतियां मशीन और फैक्ट्री बनाने में व्यस्त थीं, बजाय इसके कि रोज़गारों का सृजन करतीं. स़िर्फ सरकारी नौकरियां बढ़ रही थीं, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग ने नौकरियों में जगह बनाने के लिए आरक्षण की सोची. 1989 में जब कांग्रेस को बहुमत मिलना समाप्त हो गया, तो मंडल आयोग की सिफारिशें नीति बन गईं. 23 सालों के आर्थिक सुधारों के बाद भी यह विसंगति ठीक नहीं हो पाई. क्या अब हम एक नई आर्थिक नीति की अपेक्षा कर सकते हैं जिससे रा़ेजगारों का सृजन होगा, जिसमें कोई आरक्षण नहीं होगा? क्या भारत अपने भूत को भूलकर आगे बढ़ पाएगा?
Adv from Sponsors