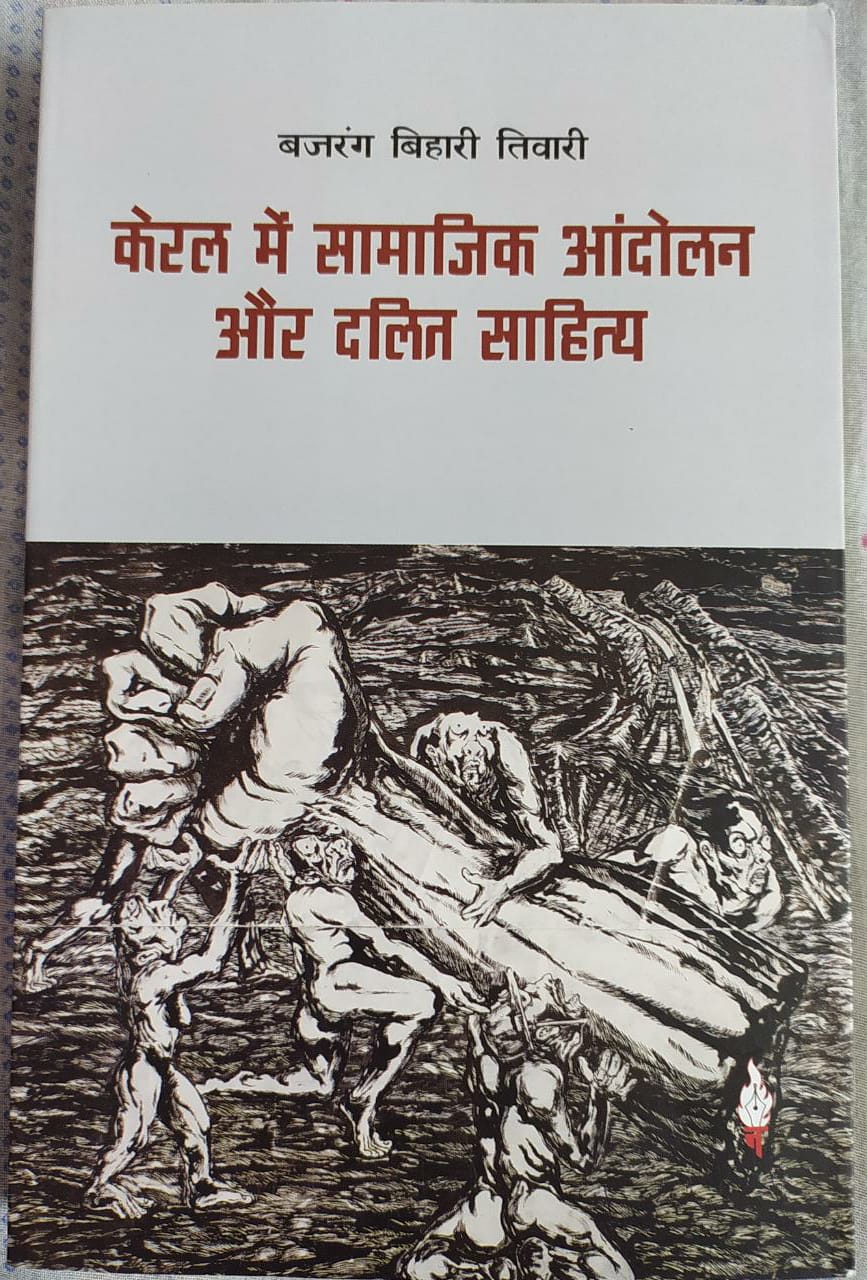|
डाॅ.बजरंग बिहारी तिवारीजी की पुस्तक’ “केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य” हमें जनवरी में प्राप्त हुई थी। बजरंग जी के माध्यम से ही हम दलित साहित्य से परिचित हो पाए। इसके पूर्व हमें यही लगता था कि साहित्य तो सब साहित्य ही होता है बस थोड़ी बहुत विचारधारा ही बदलती होंगी।
पर इस किताब की भूमिका को पढ़ने के बाद हम अंदर तक हिल गए और हमें यह लगा कि साहित्य को पढ़ने के पूर्व दलितों की वस्तुस्थिति को समझना नितांत आवश्यक है। लेखन हमारा मूड है ,शौक नहीं । पर पढ़ना
हमारा शौक है लेकिन इस भूमिका को पढ़कर मन में यह विचार हुआ कि क्यों न इस किताब की समीक्षा लिखी जाए।और बजरंग जी से अनुमति ली।
समीक्षा कैसे लिखी जाए इसके लिए गूगल को ढूँढा। समीक्षा लिखने के नियमों को जाना कई समीक्षाएं पढ़ीं कि कैसे लिखी जाए। लेकिन पहली आवश्यकता थी पूरी पुस्तक को पढ़ा जाए। यह उपन्यास या कहानी जैसा रुचि कर नहीं होगा यह स्पष्ट था। किन्तु पढ़ते हुए जाना कि इस प्रदेश के जन समुदाय की पीड़ा ,परंपराओं के बंधन ,दासत्व की क्रूरता , धर्मांधता का भय दिखाकर प्रभुत्व स्थापित करना। एक मानव किस हद तक क्रूर हो सकता है उसकी हद है। ईश्वर की छत्रछाया में रहने के लिये अधिकृत लोगों को भगवान का रत्ती भर भय नहीं ।किन्तु वे दूसरों के अंतर्मन में उस भय को इस तरह व्याप्त करता है कि जीवन भर उनका भय उससे चार कदम आगे चलकर उसे बाधित करता है।
वाकई लेखक होना कठिन काम है। हमें 7माह लगे। कई बार पढ़कर मन इतना विचलित हुआ कि कई दिन किताब नहीं उठाई। थोड़ा थोड़ा पढ़ा पर पढ़ा पूरी ईमानदारी से।और लिखा मेहनत से।
हमने पूरी कोशिश की है कि यह समीक्षा आपको किताब पढने के लिये प्रेरित करे। और हम सब समझ पाएँ कि हम जिस भी स्थिति में हैं बहुत बेहतर हैं पर कुछ लोग आज भी शापित सा जीवन भोग रहे हैं क्योंकि आज भी वही स्थिति कमोबेश बनी ही हुई है।
सिर्फ शिक्षा से ही सोच बदलेगी यह सही है किन्तु हम पहले एक अच्छे इंसान तो बन पाएँ !अगर मानव हैं तो अपने आचार-विचार और कर्म से तो मानव बन पाएँ ।मनसा वाचा कर्मणा
सद्भाव सम्पन्न हों।यह जरूरी है।
इस किताब को पढ़कर हम केरल को जान पाए।वहाँ का समाज, संस्कृति ,केरल राज्य की उत्पत्ति,भौगोलिक स्थिति को समझ पाए।
आप सबको यह लंबी लग सकती है। पर विषय ही ऐसा है लगभग 350 पेजों की दास्तान की अभिव्यक्ति इतना स्थान तो लेगी ही ।
अपने लेखन को हमने लगभग25-30 बार या शायद और भी ज्यादा बार पढ़ा हर बार कुछ नया जोड़ा ,घटाया और सुधारा। अब यह आपकी नजर है। समीक्षक की दृष्टि तो तेज होती है( हालांकि हमारे पास वह दृष्टि नहीं ।हमारा प्रयास भर है।) पटल तलवार की धार है। चमक यहीं प्राप्त होती है।
सादर
नीलिमा करैया
*समीक्षा*
*श्रीमती नीलिमा करैया*
—————-
**केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य*
(लेखक- डाॅ.बजरंग बिहारी तिवारी)
————————–
दलित विमर्श के चर्चित अध्येता डाॅ.बजरंग बिहारी तिवारी की पुस्तक ‘केरल में सामाजिक आंदोलन
और दलित साहित्य’ पिछले दिनों प्रकाशित हुई है। वे केरल के दलित साहित्य पर पिछले एक दशक से सोच और लिख रहे हैं। यह पुस्तक उस श्रम की परिणति है। श्रोतों की तलाश और विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग बजरंग जी के लेखन की विशेषता है। हिंदी में केरल के सामाजिक आंदोलन और दलित उपस्थिति को समझने के लिए यह श्रम अपेक्षित भी था। यह पुस्तक केरल के अतीत से प्रारंभ होकर उसके वर्तमान तक की श्रमसाध्य यात्रा है। इस शोध का विवेकपूर्ण ढंग से किया गया दायित्व एक उद्देश्य की पूर्णता के लिए किए गए अनवरत शारीरिक और मानसिक श्रम का परिणाम है। बार बार केरल की खर्चीली लंबी यात्रा, साक्ष्य जुटाना, पुस्तकालयों से किताबों की तलाश ,मलयाली पुस्तकों को साथियों की मदद से समझना और लिखना सहज नहीं था। निःसंदेह प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा का दायरा सीमित होता हैं। पर हिन्दी में लिखे जाने से बहुसंख्यक लोग इसे पढ़ सकते हैं। लेखक का यही उद्देश्य रहा कि देश का व्यापक पाठक-वर्ग वहां के दलित शोषण की इंतहा से परिचित हो और यह तभी संभव था जब हिन्दी में यह जानकारी उपलब्ध हो। आज के अधिकांश शिक्षित जन प्रकृति के अकूत सौंदर्य से आपूरित केरल के अतीत की उन जातिगत व दासत्व की सामाजिक जटिलताओं के साथ-साथ स्त्रियों के तिहरे शोषण के त्रास की सच्चाई और उसके सामाजिक इतिहास को समझ सकें, उससे परिचित हो सकें । उस कारण को जन-जन तक पहुँचाने और समझाने के लिये एक ऐसी भाषा अपेक्षित थी जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और पढ़ी जाती रही हो। यह किताब केरल को समग्रता में प्रस्तुत करने की दृष्टि से निश्चय ही सफल मानी जाएगी।
किसी ग़ैर दलित का, दलित आंदोलन और दलित साहित्य के प्रति इतना लगाव और रुचि आश्चर्यजनक भी लगती है।लेकिन यह भी सच है कि अपने को समस्त जातिगत भेद से परे रखकर अन्याय के विरुद्ध सबका एक साथ आगे आना निहातय जरूरी है।
इसी तरह के प्रयासों से हमारा देश मानवता से परिपूर्ण सभ्य समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो सकता है।
केरल के सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य पर लिखना किसी गल्प,लेख या गद्य की अन्य विधाओं की तरह सहज सरल नहीं जिसे एकांत में टेबल पर बैठ कर कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाए। यह चट्टानों के बीच कुँआ खोदने की तरह श्रमसाध्य कार्य था। केरल जैसे सुदूर प्रांत में वहाँ के सामाजिक आंदोलन के इतिहास को ढूंढना नींव से नगर बसाने जैसा कार्य था। अनवरत असंख्य पुस्तकों में उपलब्ध जानकारियों को अनुवादकों के सहयोग से एकत्र करना, समझना और क्रमबद्धता में उसे लिपिबद्ध करना उतना ही कठिन था जितना दृढ़ संकल्प से समुद्र में गोता लगाकर रत्नों की तलाश करना । इस किताब ने हिन्दी भाषा के कोष को समृद्ध कर केरल के बेहद तकलीफदेह सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य को समझने का अवसर दिया है।
केरल की सामाजिक संरचना का इतिहास इतना सुंदर नहीं, जितना आज हमें दिखाई देता है । इसे समझना ऊँची-नीची पहाड़ियों से चढ़ते उतरते हुए, हर प्रकार के जंगली पशु पक्षियों से भरे घने जंगलों में पगडंडी की तलाश करते हुए, जातीय त्रास और दासत्व की भूल-भुलैया में चक्कर खाते हुए, उनकी पीड़ा की खाइयों में डूबने उतरने की तरह है।निश्चित ही यह प्रांत पूरी तरह देश के अन्य हिस्सों से अलग है।
कोई भी साहित्य अपने कालखंड के सामाजिक और राजनीतिक उठापटक के प्रभाव से अछूता नहीं रहता । साहित्य को समाज का दर्पण ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन साहित्य को भी प्रभावित करते हैं । सदियों से उपनिवेशों में बँटे क्षेत्र के राष्ट्र के रूप में संगठित होने के पीछे की लंबी प्रक्रिया में जातियों ,
जनजातियों व उपजातियों में बँटे मानव समाज की सामाजिक गतिविधियों ने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है।
जातिगत भेद और दुर्भावना इंसान को किस तरह इंसान का दुश्मन बना देती है इसका आइना है केरल का सामाजिक इतिहास जिसे आप इस पुस्तक को पढ़कर जान पाएँगे।
*यहाँ की जाति प्रथाअपनी जड़ता क्रूरताऔर विचित्रता के लिए जानी जाती थी।यह व्यवस्था पिछड़ों और दलितों केप्रति घोर असंवेदनशील थी। इसकी विचित्रता इसकी असमीपता,अदृश्यता और अस्पृश्यता में व्यक्त होती थी। स्पर्श से तो छूत लगती ही थी किन्तु यहाँ देखने भर से छूत लग जाती थी।दो भिन्न जातियों के लोग कितनी दूरी बनाकर रहेंगे यह तय था।यह दूरी कदमों से नापी जाती थी ।जाति पिरामिड में कंगूरे पर बैठे ब्राह्मण से ईषव को 36 कदम की दूरी बनाकर रखना पड़ता था ,जबकि एक पुलय को ईषव जाति के व्यक्ति से 48 कदम की दूरी बनाए रखनी पड़तीथी ।ईषव अति पिछड़ी जाति थी तथा पुलय दलित जाति ।दो दलित जातियों के बीच भी छुआछूत का प्रावधान था तो दो ब्राह्मण जातियाँ भी दूरी बनाकर रहती थीं। वह पूरी तरह कठोर जातीय मर्यादाओं में बंधा संसार था*
(पृ. 9)
कवि अपनी कल्पना के भव्याकाश में विचरण करते हुए अपनी संवेदनाओं को कलात्मकता से अभिव्यक्त करते हैं ,और गद्य लेखक अपने विषयानुसार ,रुचि के अनुरूप इच्छित विधा पर अपनी कलम चलाते हैं ; पर किसी राज्य के इतिहास को पुरातत्ववेत्ताओं की तरह खोद कर निकालना ,काल का पता लगाना, भाषा को समझना ,आसान नहीं होता। केरल राज्य का सामाजिक इतिहास, आंदोलन, स्थापना और उसके बाद से निरंतर विकासक्रम को इस तरह समझाना कि काल स्वयं आपके सम्मुख उपस्थित होकर आपबीती सुनाता हुआ आभास दे ,तो किताब के बारे में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी । कथात्मक शैली में ऐतिहासिक वर्णन आपको पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
यह किताब केरल के सामाजिक आंदोलनों पर ऐतिहासिक उपन्यास की तरह है। जातीय आधार पर समग्रता में आरंभ से ही निरंतर संघर्षरत रहकर आंदोलनों के रास्ते अधिकार और विकास की विजय गाथा है।
*”यहाँ के जाति – व्यवहार की जटिलता देखकर विवेकानन्द ने इसे ‘ पागलखाना कहा था। “*
(पृ.-27)
इस किताब को पढ़ते हुए कुछ अनजाने अविश्वसनीय रहस्यों से आपका परिचय होगा । जातिवाद को पढ़ते हुए जाति की रेलम पेल आपको चौंका देगी; जैसे भूल भुलैया जैसी रास्तों की उलझन। यहाँ की छुआछूत ऐसी कि दलित (दास) लोग सड़क पर थूक भी नहीं सकते थे। उन्हें थूकने के लिए पुरवा रखना होता था। यह एक मिट्टी का बर्तन होता है, कुछ कुल्हड़ और कुछ खप्पर जैसा।
*केरल में प्राचीन और मध्यकालीन युगों की जातिगत क्रूरता के साक्ष्य नहीं मिलते, इसका मतलब यह नहीं कि इस क्रूरता का अस्तित्व ही नहीं था ; असल बात यह थी कि वर्ण – जाति की क्रूरता का दस्तावेजीकरण ही नहीं हुआ था, इन अत्याचारों का ब्योरा कौन देता? जिनके पास ऐसा करने की क्षमता थी, अधिकार था, वही उत्पीड़नकारी थे। उत्पीड़न का दर्द भला उन्हें क्यों सालता? जो उच्च वर्ण की क्रूरताएँ झेल रहे थे उन्हें भाग्य और कर्मफल का सिद्धांत बताकर चुप करा दिया गया गया था।”*
( पृ.-28 )
*” केरल में जातिगत हिंसा का स्वरूप क्या था? दलित लंगोटी ही पहन सकते थे ,उनका अधोवस्त्र अधिक से अधिक घुटने तक हो सकता था, दलित औरतों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने की छूट नहीं थी ,उनकी अपनी जमीन नहीं हो सकती थी, वे छप्पर के अलावा और कोई घर नहीं बना सकते थे ,उन्हें मुख्य मार्ग पर चलने की सख्त मनाही थी, सड़क के किनारे चलते हुए वे खास तरह की हाँक लगाते रहते थे जिससे उनके उधर से निकलने की सूचना ऊँची जाति वालों को मिलती रहे ;अगर कोई वर्णधारी उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें सड़क के किनारे की कँटीली झाड़ियों और कीचड़ में कूद जाना पड़ता था कीचड़ में डूब जाने या कँटीली झाड़ियों से शरीर छिल जाने पर मालिकों का अहम खुश होता था।”*
( पृ .29 )
यह पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जातिगत भेदभाव की हद केरल में कहाँ तक थी । यह एक उदाहरण मात्र है पर जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो और भी कई प्रसंग ऐसे मिलेंगे जो पाठकों को नि:शब्द कर देंगे ।
केरल में दासों की दुर्दशा विचलित करती है। दलितों और दासों के शोषण का वर्णन रोंगटे खड़े कर देता है कि यह उसी भारत की कहानी है जिसकी गौरव गाथा गाते हम अघाते नहीं। प्रगति के आयामों को छूने के पूर्व कितनी क्रूरता , कितने ही दर्द और कितनी ही यातनाओं का दंश इसकी नींव में दफन है।
मानव जीवन की प्रारंभिक जानकारी से यह तथ्य अनवरत है कि सिर्फ जातिगत ही नहीं बल्कि आर्थिक समायोजन के अभाव के कारण पूँजीपतियों और संभ्रांत लोगों ने अपनी सुविधा का पूरा ख्याल रखा और शायद यही दास प्रथा के जन्म का कारण बनी । और फिर यह उनकी जरूरत बन गई। उनकी गुणवत्ता यूज एंड थ्रो की तरह थी। वे इंसान होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ वस्तु थे। दासप्रथा केरल की पुरानी जाति व्यवस्था का अंग थी।
*”बीमार होने पर उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया जाता था । उम्र दराज होने पर वे निकाल बाहर किए जाते थे। मालिक की क्रूरता के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। वह अंतिम निर्णायक था। मलबार के कलेक्टर वाटसन ने मालिकों की तमाम क्रूरताएँ देखी थीं । उनका कहना था कि पहले मालिक दासों की नाक काट लिया करते थे।”*
( पृ.37)
दासों के लिये मानव जीवन नारकीय यातना की तरह था। उनका आर्तनाद सुनने वाला कोई नहीं था। न कोई उपाय न कोई रास्ता न व्यक्ति । भगवान पर तो वर्ग विशेष का अधिकार था।
यह बहुत कम है जो दृष्टांत में उद्धृत है। किताब को पढ़ने पर नए-नए तथ्य उभरते हैं-
*” मिस्टर ई. बी. थाॅमस कालीकट में जज के रूप में कार्यरत थे ।उन्होंने सत्र अदालत को 1841 में लिखी चिट्ठी में बताया कि कुछ तालुकों में दास पैदा करने के लिए ऊँचे दामों में औरतें बेची जाती हैं । उन्होंने यह सूचना भी दी कि 10 साल से कम उम्र वाले एक (दास) बच्चे की औसत कीमत 3 रुपये आठ आने है। एक अदालती नीलामी में 10 माह का शिशु 1रुपया 10 आना 6 पैसे में बेचा गया। मां की कीमत इसमें शामिल नहीं है।”*
( पृ.37)
*” द लैंड ऑफ चैरिटी “में सैमुवल मतीर ने लिखा है कि लोग अपने मित्रों को, मंदिरों को उपहार स्वरूप दास दिया करते थे।”*
(पृ.37 )
*”अगर कभी किसी दास को गवाही आदि देने अदालत जाना पड़े, तो वह महकमे द्वारा तय स्थान पर खड़ा होता था। पारंपरिक अदालतों में तब जज और अन्य कर्मचारी सवर्ण हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था उन्हें दूषित करने का साहस नहीं कर सकती थी। मर्यादित दूरी पर खड़े पुलयन की आवाज माननीय न्यायाधीश तक मुश्किल से पहुँचती होगी। दोनों के बीच की दूरी पर एक सिपाही खड़ा करके इस समस्या का हल निकाला गया । सिपाही ‘उभय प्रबोधक ‘ संवादी हुआ करता था।”*
(पृ.39)
दरअसल जाति और दास प्रथा इस किताब के केन्द्रीय तथ्य हैं।
केरल भौगोलिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य रहा। सवर्णों का यहाँ प्रभुत्व रहा। धीरे-धीरे यह ईसाई मिशनरियों के हाथों में पहुँचा और यहाँ के शोषितों को जातीय और दासत्व त्रास से मुक्ति का मार्ग मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरण में नजर आया।
ऐसा नहीं था कि विकास के पहिए थमे हुए थे। वह तो निरंतर बढ़ रहे थे। पर दासों की स्थिति जस की तस थी ।ऐसा इसलिए क्योंकि तत्कालीन शासन भी उसमें सुधार नहीं चाहता था ,पर कहते हैं ना कि घूरे के दिन भी फिरते हैं !
यद्यपि कहा जाता है कि *दर्द जब हद से गुजरता है तो दवा बन जाता है* पर ऐसा भी होता है कि इंसान थक कर अपनी राह भी बदल ले! और ऐसा ही हुआ। कई दलित जातियों ने स्वेच्छा से लेकिन कई लोगों ने मुस्लिम जनसंख्या को बढाने के प्रशासनिक दबाव के चलते मुस्लिम धर्म अपनाया । बाद में ईसाई मिशनरियों के आगमन और कंपनी के शासन ने उन्हें भावनात्मक रूप से ईसाई धर्म से जोड़ दिया। और इस तरह बहुसंख्यकों ने ईसाई धर्म अपना लिया।
*”श्रीधर मेनन ने ,”सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ़ केरल “(1979)में बताया है कि कालीकट के जमोरिन राजाओं ने मुकुवन को (मुस्लिम) अरब व्यापारियों के साथ मिलने- जुलने ,वैवाहिक संबंध बनाने और मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया था। राजा का आदेश था कि परिवार के एक सदस्य को मुसलमान बनाया जाए, इस तरह बड़ी संख्या में मछुआरे मुसलमान बने थे लेकिन दास जातियों के लिए इस धर्म में ईसाई मिशनरियों के आने और कंपनी का शासन कायम होने के बाद कोई आकर्षण नहीं रह गया था। मिशनरियों के धर्म मत से वे भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे ।तमाम कष्ट झेल कर दास प्रथा का उन्मूलन अंग्रेजों ने ही करवाया था। बेहतर शिक्षा, बेहतर आजीविका की संभावनाएं ईसाई बनने पर सुलभ थीं।”*
( पृ. 45)
*”दास प्रथा का उन्मूलन वास्तव में तब हुआ जब इसे जनवरी 1862 में लागू होने वाले इंडियन पीनल कोड से जोड़ दिया गया। इसके पहले दासों की खरीद- बिक्री किसी ना किसी रूप में जारी थी। भारतीय दंड संहिता में शामिल कर लिये जाने के बाद दास रखना अपराध की श्रेणी में आ गया ।”*
( पृ.54)
*”मिशनरियों और कुछ-एक कंपनी अधिकारियों ने दास प्रथा उन्मूलन के लिए जो लड़ाई छेड़ी थी वह कानूनन सफल हो गई, लेकिन दासों को सामान्य मनुष्यता के स्तर पर लाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी था ।वास्तविक भौतिक स्थिति में सुधार हुए बिना मुक्ति बेमानी थी। मिशनरियों ने इसके लिए संगठित और सतत प्रयास किए उन्होंने बड़े पैमाने पर स्कूल खोले। इसमें मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाती थी। सैमुअल मतीर ने लिखा है कि मिशनरी स्कूलों में ईसाई और गैर ईसाई दोनों पढ़ते थे। इनमें सबसे ज्यादा जोर बालिका शिक्षा पर था ,जिससे अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित की जा सकें और उपयुक्त पत्नियाँ मिल सकें।”*
( पृ 54)
दास प्रथा के लिये निरंतर प्रयास सराहनीय था। किन्तु जो शोषण को अधिकार समझते हों उनकी सामंती सोच को परिवर्तित करना इतना सहज नहीं था। जातीय अभिशाप दासता के बंधन से बंधा ईश्वर के प्रकोप के भय के साए में पोषित था।परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन खुले नेत्रों से भले ही दिखाई न दें पर हमारी धमनियों में प्रभुत्त्व की तरह निरंतर संचरित होकर मन प्राण पर अधिपत्य रखते हैं। वे आशा ,उत्साह ,विवेक या अन्य मानवीय मनोभावों को सर उठाने के पहले ही कुचल देते हैं, जो अन्याय , भेद या अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिये प्रेरित करें ।
धीरे-धीरे औपचारिक रूप से दास प्रथा का अंत दलितों के लिये परिवर्तन की एक नई भोर की तरह रहा।शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार ने उनमें आगे बढ़ने हेतु नई ऊर्जा का संचार किया । इस नई ऊर्जा से उनके आत्मविश्वास को बल मिला जिससे केरल में सामाजिक आंदोलनों का दौर शुरू हुआ ।
चानार एक दलित जाति थी। जो त्रावणकोर के दक्षिण में रहती थी। पूरा चानार विद्रोह वस्त्रों को पहनने के अधिकार की लड़ाई है। अन्याय की इंतहा विद्रोह की ज्वाला बनी ।जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है और मौत का खौफ इंसान के मन से निकल जाता है तो लड़ाई आर या पार की हो जाती है। चानार विद्रोह स्त्री की अस्मिता की लड़ाई थी।
*”नायरों से नीची जाति वाले को चप्पल, छाता और (खास तरह के )आभूषण पहनने की मनाही थी ; लेकिन जो प्रथा मिशनरियों को बुरी लगी वह थी कमर से ऊपर वस्त्र पहनने पर प्रतिबंध। वक्ष खुले रखने की प्रथा नायर स्त्रियों में थी । नायर स्त्रियाँ वैसे कामचलाऊ कपड़े पहन सकती थीं लेकिन मंदिर के पुजारियों और उच्च वर्णियों के सामने उन्हें अपनी छाती उघाड़नी पड़ती थी । नायर शुद्र थे।”*
(पृ.61)
इस अन्याय, प्रथा, परंपरा या फिर जबरदस्ती के बारे में सोचते हुए घृणा सी होती है। यह स्थिति मरने और मारने जैसे विचारों की सृजनकर्ता है और चानार विद्रोह इसी प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब दो जीवन शैलियों का अंतर समझ में आने लगता है, महसूस होने लगता है, तभी अधिकार का महत्व समझ आता है और प्रतिरोध की अग्नि बदला बन धधकने लगती है।अगर एक बार किसी ने कदम बढ़ाने का साहस कर लिया; फिर पीछे देखने के लिए कोई वजह नहीं बचती।
अतीत के पन्नों में चाहे कितने ही पीछे लौट जाएँ लेकिन हर पन्ने पर स्त्रियों का शोषण नजर आएगा । सारे प्रतिबंध ,सारे नियम,सारे कानून उसकी खिलाफत में खड़े नजर आते हैं । कमर से ऊपर वस्त्र न पहनने के समर्थकों में अधिकारियों के रूप में शासन भी कहीं न कहीं सम्मिलित था । और यह प्रतिद्वंद्विता सख्तआंदोलन के रूप में जंगल की आग की तरह फ़ैल गई। इसमें सिर्फ इंसानियत ही नहीं अपितु कई चर्च भी जल कर स्वाहा हो गए।कितना अजीब लगता है न! जातीय पहचान – वस्त्र न पहनने से हो !!!
अंततः परिस्थितियाँ बदलीं।
*”इस बदली परिस्थिति में त्रावणकोर सरकार ने 1865 में एक नया प्रोक्लेमेशन जारी करके सभी प्रतिबंध और शर्त हटाते हुए इच्छा अनुसार पोशाक पहनने का अधिकार दे दिया । ‘चानार विद्रोह 1859’ के नाम से प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक परिघटना का केरल के सांस्कृतिक इतिहास पर गहरा असर पड़ा ।सामाजिक आंदोलनों का एक सिलसिला इसके बाद चल पड़ा।”*
( पृ.69)
केरल रेनेसां और’श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम्’ भाग हर तरह के परिवर्तन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है । श्री नारायण जी ने इस दलित उत्थान के लिये जो संघर्ष और परिश्रम किया, वह अवर्णनीय है।सदियों से समाज में बैठी रूढ़ियों और परंपराओं की ऐसी गहरी सामाजिक पैठ जो कुरीतियों के रूप में जन- जीवन को मृत्यु पर्यंत पीड़ित करती हो, जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिये मजबूर करती हो, उस सोच में दखल देना, परिवर्तन लाने की बात सोचना या उस क्षेत्र में काम करने की प्रतिबद्धता एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम है।
हम अपने जीवन में ,अपने
परिवार में या कुटुंब में स्थापित या बनाए गए सामान्य पारंपरिक नियमों को भी सहजता से नहीं बदल पाते फिर समाज से लड़ना सरल नहीं ।
और फिर जहाँ की सारी जातीय व्यवस्था धर्म और दासत्व के ताने बानों से उलझी पड़ी हो उसे सुलझाना ओखली में सिर देने की तरह था।
असभ्य से सभ्य समाज की स्थापना के लिये किया गया संघर्ष भी देश की आजादी के लिये किये गये संघर्ष से कम नहीं ।
और इस क्रांति की ज्वाला में स्वयं को होम करने वाले लोग सामाजिक उत्थान में नींव की ईंट की तरह हैं। इस भाग में परिस्थितियाँ इतनी तेजी से बदलती दिखाई देती हैं कि मानो बार बार संभलना फिर गिरना ,फिर उठने की कोशिश फिर किसी का धक्का देना और फिर…… और फिर ……..और इसी तरह का एक लंबा क्रम-कहीं अंगारों पर चलना,कहीं समुद्री तूफान,कहीं जंगली जानवरों से घिरा जंगल।
यह स्थिति श्री नारायण जी की ही नहीं अपितु उनके नेतृत्व में अपनी अस्मिता और अधिकार के लिये लड़ने वाले लोगों की भी रही।
शैक्षिक जागरण से सोच में परिवर्तन हुआ और दुष्प्रथाओं को लोग समझने लगे। वे खटकने लगीं । प्रथाएं भी अजीबोगरीब! इनमें एक प्रथा ‘तालि ‘ बांधने की थी।
*’बचपन में ही दूल्हे द्वारा लड़कियों के गले में सोने की एक छोटी-सी पत्ती बाँध दी जाती थी।यह लड़की के ‘विवाहित’होने का सबूत था। ब्राह्मण अधिकार संपन्न थे इसलिए वे भी ‘संबंधम्’ के लिए तालि बाँधा करते थे।तालि ब्राह्मण स्त्रियों में नहींबांधी जाती थी।इसके लिए सिर्फ नायर स्त्रियाँ ही विहितथीं’ ‘तालि’ बाँधने के बाद वह स्त्री उनकी पत्नी हो जाती थी; लेकिन उसका औपचारिक पति कोई नायर ही हुआ करता था। एक स्त्री को एक सेअधिक ब्राम्हण ‘तालि ‘बाँध सकते थे। यह प्रथा पूरी तरह से ब्राह्मणों के अनुकूल थी। ‘संबंधम् ‘से यौनेच्छा की पूर्ति की जाती थी लेकिन उत्पन्न संतान या संतानों का जिम्मा नहीं लिया जाता था। वास्तव में बच्चों पर सिर्फ मां का अधिकार हुआ करता थाऔपचारिक याअनौपचारिक पिता(ओं) का नहीं*
(पृ.70-71)
शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लोगों की सोच में परिवर्तन नजर आने लगा था किन्तु ब्राह्मण स्वयं के प्रभुत्व की स्थापित जड़ों को बनाए रखने के लिये हर कीमत पर अडिग थे।धर्म के ठेकेदारों ने ही धर्म को अपने सुख -ऐश्वर्य का साधन बना लिया था। सारे अत्याचार ईश्वर के अनुयायियों की देन रहे । वक्त देर से ही सही पर करवट बदलता ही है।
नई शिक्षा से जुड़े नायर युवाओं ने ऐसी परंपराओं के खिलाफ सोच को एक नई दिशा दी। श्री कृष्ण पिल्लै के नेतृत्व में ‘ मलयाली सभा ‘ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य ‘पश्चिमी ज्ञान प्रसार, स्त्री शिक्षा एवं विवाह व्यवस्था ‘ में सुधार के साथ मलयाली समुदाय का कल्याण था। जाति एवं उपजातियों की अधिकता को देखते हुए इसे ‘जाति- समूह’ कहना सार्थक होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया।
*”ईषवों को पहली बार संगठित करने वाले और उनमें आंदोलन की भावना पैदा कर दिशा देने वाले डॉक्टर पी. पाल्पू ( 1863-1950)थे। पाल्पू का जन्म त्रिवेंद्रम में हुआ था। पिता मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे।”*
( पृ.73)
पाल्पू डाॅक्टर बनना चाहते थे पर उनकी इस इच्छा के बीच जाति आ गई।उन्होंने जीवन भर ईषवों के उद्धार के लिये संघर्ष करने का संकल्प लिया। शिक्षा की एक बड़ी खूबी यह है कि वह व्यक्ति का अपने अधिकार से परिचय करवाती है। न्याय और अन्याय के विवेक को जागृत करती है।और वही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी बुलंद करती है। यही ज्ञान डा. पी. पाल्पू के संकल्प की पूर्णता के हवन में घी का काम करता रहा।
*”शिकागो की धर्म संसद से लौटे विवेकानंद की मुलाकात डॉक्टर पाल्पू से हुई। विवेकानंद ने पाल्पू को संगठन बनाने की सलाह दी और कहा कि संगठन का मुखिया किसी संन्यासी को ही बनाना चाहिए ।भारत में किसी संगठन की स्वीकृति और सफलता इसके बिना संभव नहीं। डॉ. पाल्पू ने श्री नारायण गुरु में ईषवों का सुरक्षित भविष्य देखा। श्री नारायण गुरु 1855 – 1928 )त्रिवेंद्रम के पास एक साधारण ईषव परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता पारंपरिक lpअध्यापक यानी ‘आशान’ थे।”*
(पृ.74 )
श्रीनारायण गुरु एक सदाचारी एवं उच्च आदर्शो के साथ मानवीय मूल्यों के समर्थक थे। वे समाज को धर्म , जाति या वर्ण भेदों से परे सामाजिक समभाव के साथ एक देखना चाहते थे ‘वसुदेव कुटुंबकम् ‘की तरह। इसीलिए इनका जीवन संघर्षमय रहा।उनकी सोच उनके लक्ष्य की पूर्णता के लिये मनसा-वाचा-कर्मणा उनके साथ थी।
*”श्री नारायण गुरु ने 1921 में अलवए के अपने अद्वैत आश्रम में विश्व भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें उन्होंने अपने हाथ से एक संदेश लिखा। इसका भाव था कि मनुष्यों में संप्रदाय, पहनावा, भाषा आदि को लेकर जो अंतर दिखता है वह एक ही सृष्टि के हैं।”*
(पृ.76 )
सदियों से व्याप्त धर्म जाति और परंपराओं की जंग लगी बेडियों से समाज को मुक्त करना इतना सहज न था।
श्रीनारायण गुरु ने अपना जीवन यज्ञ बना लिया; जिसमें अपने प्रतिबद्ध कर्मों की आहुति देते रहे ।अपने लक्ष्य के बीच आने वाली हर मुश्किलों का सामना उन्होंने निडरता से किया।उनके एक अनुयायी थे के. अय्यप्पन ! इन्होंनेे एवं डाॅक्टर पाल्पू ने परिवर्तन के इस ध्वज को थामने में श्री नारायण गुरु का भरपूर साथ दिया ।
*”के.अय्यप्पन(1889-1968)ने ‘सहोदर संघम् (1917 )आंदोलन शुरु किया ।यह भाईचारा आंदोलन था जो सहभोज और अंतर्जातीय विवाह पर बल देता था।अय्यपन रूस की कम्युनिस्ट विचारधारा से किसी न किसी रूप में परि चित थे।1918 के उनके वृहद् सहभोज में विभिन्न जातियों के पाँच हजार लोग सम्मिलित हुए।
श्री कुमार गुरुदेवन का जीवन आश्चर्य जनक विविधताओं से भरा हुआ रहा । उन्होंने बाइबिल पढ़ी और पाया कि वास्तव में उनके समाज के लिये उसमें कुछ है ही नहीं ।फिर उसे क्यों पूजा जाए! उन्होंने उसे जलाने का आव्हान किया। उनकी बाइबिल के प्रति अनासक्ति और उसे जलाने का आव्हान बेहद साहसिक कृत्य रहे।
अकल्पनीय था यह लेकिन कारण बहुत ही जायज और सटीक ।
बाइबिल को जलाने से पूरा चर्च प्रतिष्ठान नाराज हुआ।
यह उस समय बड़ा जोखिम था।
श्रीकुमार गुरुदेवन ने इसकी परवाह न की।
चर्चों के जातीय दखल ने स्तब्ध किया । बड़ी पेचीदगियों के दलदलों में डूबते उतरते रहे वे ,और ऐसे में उन्हें उठाने के लिये ,उनके उत्थान के लिये सोचना और काम करना सहज नहीं,बिल्कुल वैसे ही था जैसे उलझे धागे के गुच्छे को सुलझाना या दलदल में डूबते एक समाज को निकालना।
वास्तविकता यह है कि पहले दुख धर्म में पनाह पाता है,सुरक्षा समझता है और फिर धर्म ही उसके शोषण का कारण बनता है। अपने धर्म को छोड़ने वाले की स्थिति न घर की न घाट की तरह होती है। लेकिन इतना सब करके भी उसके बाद वो जिंदा रह पाए यह भी कम आश्चर्य जनक नहीं रहा। वास्तव में हर शख़्स को धर्म का आदर करना चाहिए पर अंधविश्वास की हद तक नहीं और अगर कुछ नाजायज या गलत लगता है तो उसे बदलने या सुधारने की कोशिश करना भी जरूरी है । हर मजहब परस्पर प्रेम,करुणा, दया और सद्भावना पर कायम है। )पर धर्माधिकारी स्वयं को भगवान समझने लगते हैं । धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना, जाने बिना अपना धर्म छोड़कर किसी भी दूसरे धर्म को अपनाना पछतावे के सिवा कुछ नहीं यह वाकई एक साहसिक कृत्य था।
लेकिन स्त्रियों के संबंध में उनकी सोच ने उनके प्रति श्रद्धा के ग्राफ को नीचे खींच दिया।
सामाजिक सुधार के अग्रदूत के रूप में काम करना और ईश्वर के अवतार होने में अंतर होता है।
मुसीबतों में साथ देकर उबारने वाला लोगों को भगवान सदृश लगता है।जनता के इस विश्वास को अगर वह भ्रांति स्वरूप सत्य मान ले तो यह उसके अंत के प्रारंभ का पहला कदम होता है।यह उनकी भूल रही।पर भीड़ के न्याय और विश्वास को चुनौती देना सरल भी नहीं होता । किंवदंतियां अंधविश्वास को पोषित करती हैं, बल देती हैं ।श्री कुमारगुरुदेवन को यह लाभ सहजता से मिला। मानव मात्र के कल्याण के लिये काम करना,तकलीफ सहना और समाज के लिये उत्थान ,जागृति और विकास के लिये कार्य करने में अंतर होता है
अपनी प्रशंसा में स्वयं गीत लिखना आश्चर्य जनक है।
यह100% सही है कि किसी भी देश समाज या जाति का लिखित इतिहास अत्यधिक आवश्यक है। होना भी चाहिए ताकि भविष्य यह समझ पाए के अतीत की किन पथरीली राहों ,पहाड़ियों और खाइयों से रास्ता बनाते हुए वर्तमान आज विकास से सुसज्जित नजर आ रहा है।
*”तमाम कौमों के इतिहास (ग्रंथ)हैं मेरे पास/केरल का हर इतिहास छाना /अपनी कौम की कहानी के लिये /पृथ्वी पर कोई नहीं लिखने को था/मेरी कौम की गाथा।”*
(पृ.122)
सौ बात की एक बात जो उन्होंने कही *’अज्ञानम् को बेधने के लिये ज्ञान की तलवार चाहिए’* यह सूत्र वाक्य की तरह हर काल के लिये महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि *प्राचीन काल के द्रविड़ ही आज के दलित हैं*। स्त्रियों के संबंध में श्री कुमार गुरुदेवम् की सोच ने उनके देवता स्वरूप को एक बार पुनः प्रश्न और संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया, जबकि उन्हीं के गीतों, उपदेशों और पी आर डी एस के सामान्य बोध में ‘पॉपुलर ‘ इतिहास दृष्टि के अनुसार द्रविड़ों की समाज व्यवस्था में स्त्री-पुरुष के बीच भी अंतर नहीं किया जाता था। एक बात उनकी बहुत अजीब लगी कि *किसी सभ्यता का उत्थान और पतन स्त्रियों की यौनिकता सुनिश्चित करती है*। पी आर डी एफ का स्वरूप अपने स्वार्थ के चलते भले ही धार्मिक रहा हो पर उसके उद्देश्य और लक्ष्य दलित उत्थान ,उनके विकास, जरूरत ,अवांछित बाध्यताएं जो प्रतिबंधित सजा की तरह थीं ।उन सब पर नियंत्रण और आजादी की दृष्टि से जायज थे।
“रक्षा निर्णयम्” जज्बातों को जगाने के लिये अग्निशेखर की तरह है।
*प्रसव के अगले ही दिन काम पर जाना बहुत दुष्कर है ।दासों का, दासियों का दर्द अपरिमित है*
अय्यनकाली के बारे में पढ़कर यह समझना आसान होगा कि प्रतिभा या गुणवत्ता कबीर की तरह शिक्षा की मोहताज नहीं इसका मतलब यह भी नहीं शिक्षा जरूरी ही नहीं पर कुछ लोग समय और परिस्थितियों से सीखते हैं और सफलता ,वर्चस्व और प्रसिद्धि ऐसे ही लोगों के आगे राह बनाती चलती है अकबर की तरह। अय्यनकाली की कर्मठता महाराणा प्रताप के समतुल्य है।
बचपन की एक छोटी सी घटना नेअय्यनकाली के बालमन पर गहरा प्रभाव डाला।फुटबॉल खेलते हुए उनकी बाॅल एक सवर्ण की छत पर चली गई जिसके कारण मालिक से तो तिरस्कृत होना ही पड़ा किन्तु माता पिता से भी प्रताड़ना मिली ।इसी तिरस्कार और प्रताड़ना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी।
अय्यनकाली ने चाणक्य की तरह सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया ।
*अय्यनकाली ने संगठन क्षमता का परिचय देते हुए अपनी जाति (पुलय)के युवकों को इकट्ठा कर एक टीम बनाई ।इसे ‘अय्यनकाली पद’ (सेना) कहा गया। ऊँची जातियों के हमलों के जवाब में अय्यनकाली सेना ने भी प्रति- आक्रमण करना शुरू किया। हिंसा का बदला हिंसा से लिया जाने लगा । पुलय युवकों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने के लिए अय्यनकाली ने बाहर से गुरुओं को आमंत्रित किया*।
(पृ.88)
वे सारे सामाजिक भेद -भाव जो जातीय मर्यादाओं में बाँधकर उन्हें समाज से अलग खड़ा करते थे, उनका विरोध करने का उन्होंने निश्चय किया। उन बंधनों से मुक्त होने के लिये प्रतिबंधों को तोड़ आगे बढ़ने का दृढ़ फैसला लिया ।
*उस समय दलितों को सार्वजनिक मार्गों पर चलने की सख्त मनाही थी। वह नंगे बदन नंगे पांव ,कँटीली और कीचड़ भरी पगडंडियों पर चलने के लिए बाध्य थे। ऐसे में कल्पना विल्लुवंडी (बैलगाड़ी) को छूने तक भी नहीं जा सकती थी ।इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिये अय्यनकाली ने एक नई और खूबसूरत विल्लुवंडी खरीदी। बैलों को उसने नाधा और सार्वजनिक रास्ते पर निकल पड़े। नायरों को यह सहन नहीं हुआ।उन्होंने बैलगाड़ी को घेर लिया।पहले से तैयार अय्यनकाली कटार लेकर कूद पड़े।भीड़ तितर-बितर हो गई ।वर्जित रास्तों पर अय्यनकाली देरतकअपनी बैलगाड़ी दौड़ाते रहे बैलगाड़ी का पहिया जाति मर्यादा की सांकेतिक और दूरगामी अवहेलना करता रहा*
(पृ.88-89)
अय्यनकाली ने सिर्फ अपनी जाति के लिये ही नहीं अन्य साधुजनों (गरीबों, वंचितों) के लिये भी काम किया एक संगठन,’साधुजन परिपालन संघम्’ की स्थापना की और इसकी शाखाओं का विस्तार हुआ ।
अय्यनकाली का सारा जीवन संघर्षमय रहा। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि प्रगति और उत्थान के सारे रास्ते शिक्षा की राह से ही होकर निकलते हैं । शिक्षा ही वह माध्यम है जो दूषित सामाजिक सोच को बदलकर लोगों में नवीन जाग्रति की जोत प्रज्वलित कर सकती है। वे निरंतर सरकारी स्कूलों में दलितों को प्रवेश दिलवाने के लिये वे कृत संकल्प रहे ।और सफलता न मिलती देख कई स्कूल खोल दिये।यह सब उनके लिये सहज न था पर केरल के सामाजिक उत्थान में अय्यनकाली की यह महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
इनके जीवन का अंत उदास करता है।श्रंखलाबद्ध कठोर श्रम,और अपना संपूर्ण जीवन,और वक्त उन्होंने गुलामी से मुक्त कर एक बेहतर सामाज की स्थापना और निर्माण के लिये होम कर दिया।
कर्म ही उद्देश्य का साधन होता है।
किन्तु अफसोस!!!जातिवादी उत्पीड़न आज भी कई जगहों पर चल रहा है।
हर युग,हर कालखण्ड परिवर्तन के चक्र से प्रभावित होता है। *निरंतर बदलते आस्था के आयाम और जीवन परंपराएं स्थायी आदर्श नहीं हो सकते*।
जब हम चर्च और ईसाई धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह सब एक हैं ।यहाँ कोई भेद नहीं है। पर वास्तविकता ऐसी नहीं थी। केरल में अपने जातिगत त्रास और दासत्व के संकट से बचने के लिए लोगों ने ईसाई धर्म अपना तो लिया पर भेदों से फिर भी न बच सके ।जातीय आधार का प्रभाव चर्च को भी अपने संक्रमण से अछूता न रख सका।
सांस्कृतिक अभ्युत्थान के नायक पोयिकयिल
योहन्नान धर्म परिवर्तन पर विश्वास करते थे अतः उन्होंने बाइबिल का अध्ययन किया ; किंतु यहाँ भी वास्तविकता के धरातल पर होने वाले जातिगत भेदभाव ने उन्हें आहत किया। बाइबिल पढ़ने के बाद उन्हें बाइबिल की प्रासंगिकता निरर्थक लगी। उनका मानना था कि ईसाई मत यहूदियों का धर्मसंघ है इसमें पुलयों के लिए कुछ भी नहीं है *अतः उन्होंने बाइबिल को जलाने का आव्हान किया*।
एस एन डी पी योगम् के प्रयासों से कुछ जागरूकता के चलते वामपंथी आंदोलनों ने निचली जातियों में लोगों की चेतना को जागृत किया। एक अरसे से उत्पीड़न के दंश की पीड़ा ने उससे मुक्ति की राह तलाशी और वह मार्ग उन्हें कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ने में नजर आया।
कम्युनिस्ट शासन और वामपंथी आंदोलन केरल की चर्चा में अनिवार्य संदर्भ है।
1957 में कम्युनिस्ट सरकार के शासन में आने के बाद कर्मचारियों के लिए न केवल प्रोविडेंट फंड दिया अपितु आवास निर्माण का काम अपने हाथों में लिया ।अवकाश की सुविधा को नियमित कर श्रमिक हितों की सुरक्षा के लिए समितियों का गठन किया ।वह समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था व केरल की आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी तेजी से बदल गई थी। साक्षरता ने मार्क्सवादी विचारों को पुष्ट किया। किन्तु केरल की परिस्थितियां अब भी अपने लक्ष्य से दूर थीं ।
सत्य तो यह है कि हिन्दुस्तान की जनता उस समय आजादी की लड़ाई के प्रति आंदोलनों में तत्पर थी किन्तु केरल के दलितों के सम्मुख दोहरी आजादी की लड़ाई थी। अंग्रेजों से भी और अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व की लड़ाई ।
यह किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि केरल राज्य की स्थापना के साथ ही वहाँ के दुख और दर्द की कहानी है ।इसे पढ़ते हुए आप कई भावों और अहसासों से गुजरेंगे ।अगर आपमें थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो आप अपने आप को ख़ुशनसीब महसूस करेंगे कि आप सबका जीवन कितना सुखमय है और तुलनात्मकता में उनकी पीड़ा आपको न जाने कहाँ- कहाँ स्तब्ध कर देगी,कहाँ आप विचलित हो उठेंगे और आपको कई जगह अपने आवेश पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा।
कई सालों तक जो कुछ दलितों ने अपने जीवन में भोगा वही उनके सृजन और रंगमंच पर मंचन के विषय हैं । योहन्नान की पी आर डी एस सभा इसी मंचन के माध्यम से भोगी हुई क्रूरता को दुनिया के सामने लाना चाहती थी
इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा और क्यों न हो?क्योंकि इंसान या आपबीती लिखता है या अपने आस पास के परिवेश, जाति,समाज इत्यादि को लिपिबद्ध करता है फिर चाहे काव्य कविता में हो या गद्य की किसी भी विधा में ।
दलित साहित्य भी उसी रंगमंच का सृजन है अतः यह उससे अछूता भी नहीं रह सकता।
स्वयं डा. बजरंग बिहारी तिवारी इस विषय में काफी कुछ पूर्व में भी अपने आलेखों में लिखते रहे हैं।
दलित साहित्य को जानने के पूर्व उसकी शैली को जानना आवश्यक है। हम भी इस किताब को पढ़कर ही यह जान पाए कि मलयालम भाषा तमिल एवं संस्कृत से कितनी गहरी जुड़ी है । मलयालम की दो प्रारंभिक शैलियाँ हैं पाट्ट और मणिप्रवाल । पाट्ट में तमिल या द्रविड़ श्रोतों से रचना-विधान, शब्द और छंद लिए जाते हैं ।इसमें लोक जीवन के श्रम और उससे जुड़े कथ्य प्रधान होते हैं ।पाट्ट ,गीत या लोक गीत को कहते हैं जबकि मणि प्रवाल संस्कृत की ओर झुकी हुई शैली है। श्रृंगारिक विषय इस शैली में ज्यादा है।
हर दलित जाति के अपने-अपने पाट्ट होते हैं। इन पाट्टगीतों में छुआछूत, श्रमिकों की व्यथा, दलित स्त्रियों पर अत्याचार के साथ ही प्राकृतिक चमत्कारों और घटनाओं की व्याख्या भी मिलती है।
दलितों का अतीत जिन स्थितियों में बीता ,वही जीवन ,चिंतन और प्रतिरोध इनके सृजन का विषय रहा।योहन्नान ने इसी को अपने कर्मक्षेत्र का विषय बनाया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मिल सकेगी। योहन्नान ने जो भी रचनाएँ लिखीं सब पाट्ट रूप में थीं।
*” इनके गीतों ने एक तरफ चर्च प्रतिष्ठान को चुनौती दी। दूसरी तरफ दलित समुदाय में चेतना का प्रसार किया। सुदूर इतिहास में दलित स्वाधीनता, बाद में गुलामी की असहनीय पीड़ा और वर्तमान में करवट लेता समय; सभी योहन्नान के गीतों में अभिव्यक्त हुए हैं।”*
( पृ. 225)
वास्तव में दलित साहित्य उनके जातिगत प्रतारणा की आपबीती है ।दलितों के जीवन ने अपनों को निरंतर जिस पीड़ा से जूझते पाया वही पीड़ा शब्द बनकर साहित्य में ढली और भाव संवेदनाओं के रूप में लिपिबद्ध होते चले गए । सत्य है;अतीत इतिहास के रपट में लिपिबद्ध होकर अपने को प्रगट करता है।
केरल में वेद- ब्राह्मण की सर्वोच्चता को भक्ति काल में चुनौती नहीं दी गई; बल्कि आधुनिक युग में एक तरफ योहन्नान ने तो दूसरी ओर श्री नारायण गुरु ने सनातन धर्म में विक्षोभ पैदा कर जातिगत भेदभाव खत्म करने का संदेश दिया।
अप्पचन ने एक पाट्ट में कहा कि *हर जाति के अलग-अलग चर्च हैं, चर्चों कि यह श्रृंखला जाति के अंतर को दूर करने में असमर्थ है।* एक गीत में वे कहते हैं-
*हम हिंदू धर्म के पीछे गए/ अजनबियों की तरह भटके/ हम ईसाइयत के पीछे गए/ अनाथों की तरह चक्कर लगाए/ हिंदुओं ने हमें स्वीकार न किया/ ईसाइयों ने हमें मंजूर न किया /इस दुनिया में कोई नहीं /जो हमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता दे सके।*
(पृ.226)
1940 से केरल की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन स्वरूप दो धाराएं आईं ।पहली गांधीवाद एवं दूसरी मार्क्सवाद। गांधीवाद में दलित ‘हरिजन’ है और मार्क्सवाद में ‘सर्वहारा’। कवि तिलक पंडित करूप्पन को मलयालम का पहला दलित कवि कहते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 26 है। ध्रुव चरितम् ,सौदामिनी, पंचवटी ,बालकलेशम् और उद्यान विरुन्न उल्लेखनीय हैं।
आदि शंकराचार्य रचित ‘मनीषा पंचकर्म’ की प्रस्तुतियाँ पारिवारिक व सामाजिक समारोहों में बहुत रंजक व ज्ञानवर्धक रहती थीं।इस कृति के आधार पर ही इन्होंने ‘पोट्टन तैय्यम’ तैयार की।
पंडित करुप्पन ने तमाम दलित जातियों के बीच मौजूद भेदभाव को रेखांकित किया।
*दूर भागते हैं तीय्यन कणक्कन को देखते ही गाली दे भगाते हैंकणक्कन पुलयन को देखते ही छुआछूत से मरते हैं आपस में पुलयन परयन और उल्लाहन*
(पृ.229)
सुधारवादी दौर के दूसरे रचनाकारों में मुल्लूर एस. पद्मनाभ मणिक्कर का नाम महत्वपूर्ण है।
यह नारायण गुरु के अनुयायी रहे। सामाजिक भेदभाव व जाति -भेद का खंडन इनका विषय रहा ।श्री नारायण गुरु से ही प्रेरित और अद्वैत दर्शन से प्रभावित समतावादी कवियों में एम .पी. अप्पन का नाम भी आता है। इन्होंने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से ऊंच-नीच की मानसिकता का खंडन किया है। संवाद शैली में लिखी कविता में उच्चता के दावे का खंडन बहुत आहिस्ते से किया गया है। संवाद एक राजकुमार और घास की पत्ती के बीच होता है।
गोविंदन आशान को कवि रूप में मुख्यतः उनकी रचना ‘ अरुकोला काण्डम्’ के कारण याद किया जाता है ।वास्तविकता और मिथक के मिश्रण से तैयार इस लंबी कविता का प्लाट दलितों और गैर दलितों की जीवित स्मृति का हिस्सा है। अरुकोला कांण्डम् का चलता हुआ अनुवाद ‘भुतहा खेत’ होगा। यह जगह अब भी इसी नाम से पत्तनमतिट्टा जिले में है। मार्क्सवाद से अंबेडकर वाद की तरफ आने वालों में कवियूर मुरली का नाम लिया जाता है। इन्होंने मलयालम में अंबेडकरवादी दलित साहित्य को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई।
कल्लट शशि( 1932 -1996 )स्कूली जीवन से ही कम्युनिस्ट पार्टी में आए और लेखन कार्य शुरू किया। मात्र 24 वर्ष की आयु में उनकी कविता ‘इंडियायुदे मकल’ (भारत की बेटी, 1956 )छपी। एक दलित स्त्री अम्मिनी के जीवन को पेश करने वाली यह कविता स्वतंत्र देश में दलितों की नई पीढ़ी की दुरावस्था को सामने लाती है।
अपने विश्लेषण में मार्क्सवादीऔर प्रतिबद्धता में अंबेडकरवादी कल्लर! सुकुमार और विशिष्ट कवि के रूप में दिखाई देते हैं। उतरा वी. के. नारायणन, मुनतूर कृष्णन ,के . के.एस.दास इत्यादि कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से केरल में केरल के अतीत को साहित्य में लिपिबद्ध किया ।उद्देश्य यही था कि लोग उनकी पीड़ा से परिचित हों। शासन उन्हें उनकी पीड़ाओं से स्थायी रूप से मुक्त कराएं। एक जन -जागृति की लहर बन परिवर्तन परिलक्षित हो।
दलित कविता का भिन्न तेवर तंकप्पन(1949 )के सृजन में मिलता है। एक उदाहरण:
‘अम्मा’ कविता की स्त्री पुरुष की नियत पहचान कर इस तरह उत्तर देती है-
*आँचल पकड़े काले हाथों को /दाँत से काटकर/ अलौकिक लज्जा की /गंदी खाल उतारकर/ मैं जान लेती हूँ /मेरी कमर/ तुम्हारे कामासक्त आक्रमण/ की शैया नहीं/ कटु अनुभवों के कफों को/ छाती की खान से खींच कर /तुम्हारे मुँह पर थूकने में /समर्थ हूं मैं /नी…च ,नीच*
(पृ .238)
राघवन अत्तोली (1957) मलयालम दलित कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। कवि होने के साथ ही प्रतिष्ठित शिल्पी भी है। इनकी रचनाएं व्यथा की दस्तावेज हैं।
*”भीड़ के बीच भीख में मिले अन्न सी/ क्षत-विक्षत बन खड़ी है वह /पानी लेने पीने में जो करते हैं /छुआछूत की राक्षस क्रीड़ा/ उनके बीच सूखा गला लिए मरने वाली/ यह मेरी माँ”*
किसी भी रचनाकार की रचना से निकले पीड़ा के ये स्वर किसी भी सह्रदय के ह्रदय को छलनी कर आक्रोश पैदा करने में सक्षम है।
और भी कई कवि हैं जिन्होंने प्रतिरोध, प्रतिशोध और विक्षोभ के साथ ही परिवर्तन न्याय और सुधार पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं किंतु रचनाएं अपने वक्त के सत्य को तौलती रहीं। सर्वाधिक अत्याचार स्त्रियों ने सहे अतः सृजन में स्त्री स्वर भी मुखरित हुआ,भले ही उसमें वक्त लगा।
गद्य लेखन आलोचना या कथा साहित्य में दलित स्त्रियों की संख्या और सक्रियता वैसी नहीं है जैसी कविता में ।संभवतः आने वाले समय में अनुपात बढ़े।
वरिष्ठ पीढ़ी की दलित स्त्रियों की कविताएँ अभिधा मूलक और प्रबोधन परक थीं। जल्द ही उनका रूप बदला और अभिव्यक्ति में संश्लिष्टता आई ।आक्रोश सतह से चलकर शिराओं में प्रवाहित होने लगा।
स्त्री कवयित्रियों में वलसला बेबी (1947) वरिष्ठतम पीढ़ी की रचनाकार हैं। वे केरल विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर रहीं । “स्त्रीवादी लेखन पर सेमिनार” कविता पर उनका तल्ख अनुभव व्यक्त हुआ है।
*”औरतों के ज्वलंत मुद्दे उस तितली की तरह/ जो गिरती है कड़ाही से /आग में”*
(पृष्ठ 261)
कविता उस विडंबना पर अँगुली रखती है जो गंभीर ,वास्तविक, जरूरी को अगंभीर, कृत्रिम और गैर-जरूरी से अपदस्थ कर देती है।
के. के. निर्मला (9669-2006) कवि गीतकार होने के साथ पेशेवर गायिका भी थीं।निर्मला मुठभेड़ की तैयारी, ललकार भाव और प्रबोधन की मंशा के साथ कविता रचती हैं। निर्मला की ‘दंड’ शीर्षक कविता, असत्य की ताकतों के सामने सत्य का आव्हान करती है ।कर्म को ताकत व न्याय का मतलब जिसके लिये केवल दंड है। यह कविता दलित अस्मिता की परिचित आवाज है।
*”एक दिन आऊंगी मैं/ दबावों के चलते नहीं/ न किसी की दासी बनकर/ तनी हुई रीढ़ के साथ/ किसी के सामने झुकती हुई नहीं/ बगैर किसी चूक के/ किसी को बातचीत की अनुमति दिए बिना/सोचने का समय दिए बिना आलोचना की परवाह न करके / प्रतिक्रियाओं के लिए अवकाश दिए बगैर/ तब मेरा साथी होगा सत्य/ कर्म मेरी ताकत अगर कोई अदालत है दुनिया में/होगी वह सिर्फ मेरी /होगा सिर्फ एक कानून /मेरा कानून/उसमें होंगे केवल कठोर दंड।’*
(पृ.262)
पुष्पा जॉय (1972 )की कविता ” काली परछांई” आकांक्षाओं का लेखा-जोखा है। जीवन की कठोर वास्तविकताएँ रचनाकार के सम्मुख हैं । *कवयित्री दृष्टा होने से पहले उन वास्तविकताओं से गुजर चुकी हैं*।यह गुजरना असमाप्य प्रक्रिया है। वह प्रेक्षक भी है और
भुक्तभोगी भी।सत्य का साक्षात्कार कराती पुष्पा जॉय की कविता की बानगी देखिये-
*”स्वप्न: खोजता है जो नन्हा मुन्ना मृत मां के वक्षस्थल में/ फिर से :टूटे मस्तिष्क की दीवार अपमान कारी वचन/ बेचारा धड़कता दिल/ यहां : सूर्यास्त की प्रतीक्षा में टकटकी और चौकन्नी बधिरता/ उपरांत :विद्रोह की दुंदुभी शांति प्रेमियों द्वारा लाई गई /मां :छवि! जहाँ रोया जा सके भ्रातत्व का धागा टूटने पर/ मैं: सपनों का एक बंडल, उम्मीदों का कब्रिस्तान और वह दुष्ट जिसने यह सब देखा है/आग: बुरे बच्चों के अंग, जो जलते हैं अच्छी तरह /सुंदरता: काले रंग में पुता एक चेहरा, संभ्रम से नष्ट एक आख्यान /प्रेरणा :आलोचना से पूर्व सान चढ़ा एक चाकू /प्रार्थनाः ज्ञानी का आदेश-/ प्रार्थना करो मेरी /मैं हूं तुम्हारा ईश्वर….”*
(प्र.263)
अंबिका प्रभाकरण (1975) परिवार की त्रासदी पीड़ा का सबसे अंतरंग हिस्सा होती है। छोटी बच्ची इस पीड़ा को सबसे ज्यादा महसूसती है ।माँ पर सतत मंडराया डर उस पर अपनी छाया पहले डालता है ।अंबिका प्रभाकरण की कविता बताती है कि तनहाई कभी निरपेक्ष होकर नहीं आती ।उसका एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य होता है जो समाज व्यवस्था का उत्पाद है।
*”विन्सैंट के द्वारा तोड़े दरवाजे से निकल/ पिता को घर छोड़ते हुए/ मां ने कैसे देखा ?/विगत की चिंता मां क्यों करें /जब उसके सिर पर रखा रसद का बोझ/जमीन पर छलक पड़ रहा है?/ लैंप से उतरी छाया प्रेत है/ और रात की आवाज/ मूसल उठाए चलते दैत्य की है/ रात जबकि लघुशंका के लिए वह उठी /पूरे प्लॉट का चक्कर लगा आई/ मां इतनी डरी क्यों है?/ दो बेटियों को जनने के बाद भी।”*
(पृ.264 )
विजिला (1981) दलित स्त्री कवियों में चर्चित नाम है ।विजिला वाम विचारधारा से जुड़ी रचनाकार हैं। यह दलित स्त्री के अंतर्जगत का सोद्देश्य चित्र प्रस्तुत करती हैं। यह चित्र भौतिक असुरक्षा और उससे टकराती इस्पाती बेफिक्री से बना है। उनकी ‘पगडंडियाँ ‘ नाम की कविता घास काटती हिम्मती महिला उम्माजी से परिचय कराती है। उम्माजी की छींटदार साड़ी और मेहंदी रचे हाथ खतरे का सबब हैं । शिकारी की निगाह इधर घूमी है। पगडंडी पर वही पुराना अंधेरा है। कवयित्री इस अँधेरे को दौड़कर पार करना चाहती है। उसने कभी सपना देखा था कि पगडंडी पर आग लगेगी।
*” पगडंडी पर पहुंचकर/ तेज दौड़ती हूँ।/ सड़क पर पहुंचने के बाद ही/ मुड़कर देखती हूं/ काना जनार्दनन/ सीत्कारी आवाजों के छेद/ सांप का केंचुल/छितरा पड़ा लाल रिबन/ सभी पगडंडी पर प्रतीक्षा में हैं/ पगडंडियों पर/ आग लगने का सपना/ कल देखा था/ किसी से डरे बिना/ उम्माजी तब भी /मेहंदी रची हथेलियों से/ घास काट रही हैं।*
विजिला की नजर से वर्ग का सवाल भी ओझल नहीं हुआ। उन्होंने दलित स्त्रियों में भी वर्ग भेद का मुद्दा उठाया । परिवार विजिला की कविताओं का एक केंद्रीय विषय है ।उसमें माँ की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है।संबंधों के ताने-बाने में शक्ति और संवेदना के समीकरण माँ से निर्धारित होते हैं। मां रचनाकार बेटी को कच्ची सामग्री देती है और दृष्टि भी।
युवतर रचनाकारों में प्रवीणा के .पी.( 1983) उल्लेखनीय नाम है ।प्रवीणा ने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विषय में शोध किया है। उनकी कविताएँ वैश्विक संदर्भों का भी संज्ञान लेती हैं। संरचना में विन्यस्त और गतिशील हिंसा, पहचान के क्रम में झलकती जाती है। शब्दों के अर्थ भी उलटते हैं ।सज्जनों को देख कर दहशत होती है ।देवदूत क्रूरता बरपाते हैं ।वास्तविकता का ऐसा प्रकटन सहम कर जा छिपने को बाध्य कर दे! यह स्वाभाविक लगता है लेकिन चेतनशील व्यक्ति अब पलटकर मुठभेड़ करने को तैयार है।
*अच्छे लोगों से मैं हमेशा डरी रही हूँ/जब भी मैं सज्जनों को देखती हूँ/ मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ/ या फिर मैं वह जगह छोड़ देती हूँ/वे फिर भी मुझे ढूँढ़ निकालते हैं/ और मेरी तरफ पत्थर उछालते हैं/ हम दोनों इसकी वजह नहीं जानते/ मैं चलती हूं अपने सत्य के पथ पर/ बगल से गुजरते देवदूत मुझे कर देते हैं घायल/ और उड़ जाते हैं स्वर्ग की ओर/ उनके पंखों पर लगा है खून/ और मेरे विचारों में आग।*
रम्या तुरवूर की(1984) की रचनाशीलता अपने समकालीनों से भिन्न है। भिन्नता की मुख्य वजह उनकी कविताओं की अंतर्वस्तु है। विशिष्ट अंतर्वस्तु अपनी शैली साथ लिए चलती है।इस लिहाज से रम्या का काव्य मार्ग अपनी संपूर्णता में नवाचारी लगता है।
रम्या के यहाँ विषाद का एक स्रोत प्रेम है और प्रेम कविताओं में देह की मौजूदगी है। दोनों आपस में जुड़े हुए साथ साथ चलते हैं। भग्न प्रेम से उपजे विषाद पर कई बार तिक्तता हावी होती है। तब विषाद का आकाशी रंग धुंधला जाता है । अन्याय उन्हें बहुत उद्विग्न करता है, क्योंकि यह अन्याय शब्दों में घटित होकर चिरकालिक बना है । इसलिए कवयित्री का गुस्सा अक्षरों पर भी
उतरा है। कवयित्री पाती हैं कि अन्याय की वह
परंपरा अब भी कायम है ।द्रोण आज भी अंगूठे
की ताक में रहता है।
*अँधेरों से बने द्रोण सिंहासन पर/आज भी भेदभाव के आँसू/सितारों से बनी/तेरी आँखें/कल के एक/ अँगूठे की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं*
धन्या एम .डी. (1984) चर्चित रचनाकार हैं।
उनकी कविताओं की किताब ‘अमिग्दला’
(2014) ने कवियों और आलोचकों का ध्यान
आकर्षित किया है। काव्यानुभूति की सघन
बनावट और अभिव्यक्ति के अद्भुत मुहावरों के
कारण धन्या समकालीन मलयालम कविता में
विशिष्ट मुकाम हासिल करने की क्षमता रखती
हैं ।उनकी कविताओं में यादों का अछोर संसार
बसता है।
धन्या की कविता चुप्पी की पहचान करती है।
इस चुप्पी में विशाल दुनिया समाई हुई है तो चुप्पी की कल्पना कानों से की जानी है ।कान जो सिर्फ सुनते नहीं देखते भी हैं।
उपरोक्त सभी कवयित्रियों का सृजन मलयालम दलित कविता के उत्तरोत्तर उन्नयन और विस्तार की आश्वस्ति देता है।
*पाठकीय मन्तव्य*
डा.बजरंग बिहारी तिवारी की यह किताब *केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य* न केवल साहित्यकारों के लिये अपितु उनके लिये भी ,जो साहित्यकार नहीं हैं किंतु पढ़ने में जिनकी विशेष रुचि है,लाभान्वित और समृद्ध करती है।देश के अधिकतम लोग एक सर्वाधिक शिक्षित राज्य की उपलब्धता के पीछे के संघर्षों की अकथनीय, असहनीय और अमानवीय पीड़ाओं को जान सके, समझ सके और प्रतिक्रिया दें कि सारा देश उसके साथ है ,हम सब उसके पास भले ही नहीं पर उसके साथ हैं ;यही इसकी उपलब्धता है।
सामाजिक उत्थान के अध्येताओं के लिये यहाँके सामाजिक आंदोलन प्रेरणा श्रोत की तरह हैं।
दलित साहित्य के नये आयाम के उद्घाटन की तरह है यह सृजन।
एक ऐसा साहित्यिक सृजन ! जिसमें आप क्षेत्र विशेष के सामाजिक आंदोलन ही नहीं बल्कि भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी से भी समृद्ध होते हैं । एक दुखांत उपन्यास की तरह घटनाएं आपको विचलित और आक्रोशित करेंगी। दुख शब्द एक होता है। किन्तु सबके अपने-अपने दुखों के अनगिनत प्रकार और कारणों का वजन कितना और कैसा है यह महत्वपूर्ण है।
रचना की सफलता इस बात से है कि एक बार हाथ में लेने के बाद पढ़ते हुए उसकी घटनाएं इतनी जीवंत हो उठती हैं कि आप छोड़ नहीं पाते। शैक्षणिक दृष्टि से यह पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। शोधकी दृष्टिसे ही नहीं बल्कि काॅलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने योग्य स्तर है इसका।
डाॅ. बजरंग बिहारी तिवारी की भाषा सहज एवं सरल है।कथात्मक शैली में वर्णन विषय को रोचक व प्रभावशाली बनाता है।
388 पृष्ठ की इस पुस्तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक इसकी भूमिका है। भूमिका लेखन में पुस्तक की अंतर्वस्तु दर्पण की भाँति परिलक्षित होती है । वास्तव में यही वह पुरातत्व है जो पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिये आपको बाध्य करता है।निश्चित ही पुस्तक से कम मेहनत भूमिका लेखन की नहीं । दोनों सम तुल्य है । भूमिका पुस्तक का सारतत्व है।
किताब के अंत में अनुक्रमणिका के अनुसार संदर्भ और टिप्पणियाँ हर शंका का समाधान करने में मददगार हैं ।
किसी आलोचक के मन में यह सवाल आ सकता है कि सामाजिक आंदोलन पर ज्यादा लिखा गया दलित साहित्य पर कम किन्तु पुस्तक के शीर्षक के अनुरूप प्राथमिकता सामाजिक आंदोलन ही है। फिर भी दलित साहित्य पर भी पर्याप्त चर्चा हुई है।
पढ़ते हुए कहीं – कहीं पर टंकण की त्रुटियाँ व कहीं- कहीं विराम चिन्हों की उपेक्षा नजर आईं जिन्हें अगले संस्करण में सुधारा जा सकता है।
हम उनके 10 वर्ष के अनवरत परिश्रम के फल स्वरूप लिखी गई इस किताब के लिये तहेदिल से उन्हें बधाइयाँ देते हैं । व भविष्य के लिये बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भी।
श्रीमती नीलिमा करैया
एम.ए .,बी.एड.
व्या
ख्याता-हिन्दी
होशं गाबाद (म.प्रष.)
मोबाइल-8319904531

|
|
Adv from Sponsors