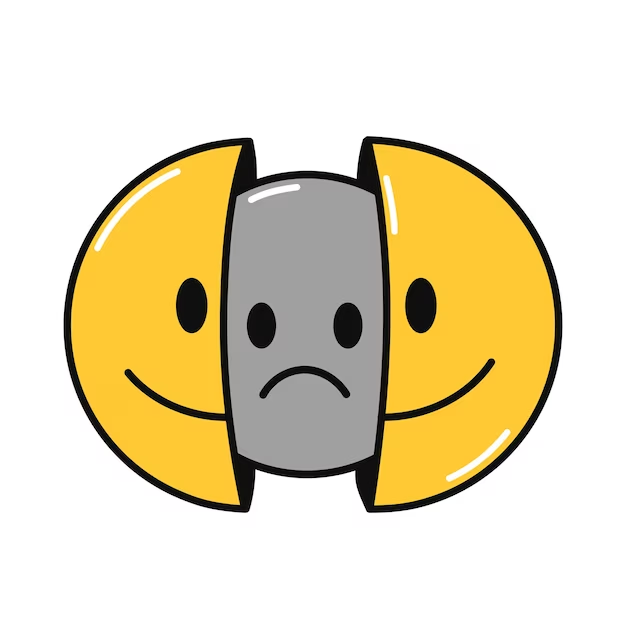आजादी के बाद से ही देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा में लगातार गिरावट देखी जा रही है. उनकी दशा गिरकर अनुसूचित जाति के स्तर तक जा पहुंची है या फिर उससे भी बदतर. कुछ राजनेताओं, व्यक्तियों और ग़ैर सरकारी संगठनों की तो राय है कि समुदाय की ऐसी हालत के लिए ख़ुद मुसलमान ही ज़िम्मेवार हैं. राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने और देश के विकास में योगदान करने के बजाय उन्होंने अलग-थलग रहना पसंद किया. न स़िर्फ राष्ट्र की मुख्यधारा से, बल्कि समाज से भी. मुसलमान अगर राष्ट्रीय मुख्यधारा और समाज से कट कर नहीं रहे होते तो वे इसके फायदे के हिस्सेदार भी होते.
आजादी के बाद से ही देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा में लगातार गिरावट देखी जा रही है. उनकी दशा गिरकर अनुसूचित जाति के स्तर तक जा पहुंची है या फिर उससे भी बदतर. कुछ राजनेताओं, व्यक्तियों और ग़ैर सरकारी संगठनों की तो राय है कि समुदाय की ऐसी हालत के लिए ख़ुद मुसलमान ही ज़िम्मेवार हैं. राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने और देश के विकास में योगदान करने के बजाय उन्होंने अलग-थलग रहना पसंद किया. न स़िर्फ राष्ट्र की मुख्यधारा से, बल्कि समाज से भी. मुसलमान अगर राष्ट्रीय मुख्यधारा और समाज से कट कर नहीं रहे होते तो वे इसके फायदे के हिस्सेदार भी होते.
बहरहाल, देश के विभाजन के बाद विकास के दौर का अगर बारीक़ी से विश्लेषण करें तो जो तथ्य सामने आता है, वह इन आरोपों के बिल्कुल विपरीत है. मुसलमान अब भी विकास के हर क्षेत्र में का़फी पीछे हैं, इसकी हर मुमकिन कोशिश की गई है. हर क्षेत्र, जैसे कि निर्वाचित निकायों, रोज़गार के क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थाओं आदि तो बस कुछ उदाहरण भर हैं, जिनमें उनके प्रवेश का आधिकारिक तौर पर रास्ता बंद किया गया. आज मुसलमानों की जो दयनीय दशा है, उसके लिए आज़ादी के बाद देश में बनी सरकारें पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं. देश के विभाजन के बाद मुसलमानों का जो प्रबुद्ध और संपन्न तबका था, वह पाकिस्तान चला गया. लेकिन वे मुसलमान जो उस समय की मुस्लिम लीग की बातों में नहीं आए और जिन्होंने पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहना पसंद किया, आज न केवल अशिक्षित और ग़रीब हैं, बल्कि बुरी तरह दमित, डरे हुए और हाशिए पर हैं. उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा अनुसूचित जाति में शामिल लोगों जैसी ख़राब है, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा बदतर है.
भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज़रिए अंग्रेजों ने मुसलमान अनुसूचित जातियों को भी दूसरे हिंदू हमपेशों के साथ आरक्षण की सुविधा दी थी, लेकिन आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश (अनुसूचित जाति) 1950 के ज़रिए इसे वापस ले लिया. यहां यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि आज़ादी के बाद हमारी संविधान सभा तक ने भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को बग़ैर किसी संशोधन के 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार कर लिया था. ऐसा लगता है, मानो स्वतंत्रता के बाद हमारा धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व अपना संविधान लागू करने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए उसने आनन- फानन में अध्यादेश जारी करा दिया. यह संविधान सभा के निर्णय का खुला उल्लंघन कहा जाएगा. देश के मुसलमानों के प्रति कभी न ख़त्म होने वाली दुर्भावना और भेदभाव की वह शुरुआत थी और यह सजा आज भी बदस्तूर जारी है. उन्हें अशिक्षा, ग़रीबी और भुखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया गया है. अगर जेल को छोड़ दें तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हर कहीं कम है. आबादी के अनुपात में जेलों में उनकी उपस्थिति अवश्य अधिक है. मुसलमान सालों से जेल में हैं और ज़्यादातर मामलों में उनका ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और अगर शुरू भी हुआ है तो वह प्रारंभिक अवस्था में ही है. ज़्यादातर मामलों में अदालत को उनके ख़िला़फ कोई महत्वपूर्ण सुराग़ हाथ नहीं लगे. 22-24 अगस्त, 2008 को हैदराबाद में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लोगों की लोक अदालत लगी थी, जिसमें विगत दो साल के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपी मुसलमानों के उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई में यह पाया गया कि जिन पर दोष सिद्ध नहीं हो सका और उन्हें रिहा किया तो गया, लेकिन कई साल तक ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से बंदी बनाए रखने के बाद. सरकार की एजेंसियों द्वारा उठाए गए ग़ैर क़ानूनी क़दम से इन भुक्तभोगियों और उनके परिवारों को जो परेशानी हुई, उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा?
बहरहाल, स़िर्फ नमूने के तौर पर केवल तीन क्षेत्रों यानी निर्वाचित निकाय, रोज़गार और शिक्षा में मुसलमानों के कमज़ोर प्रतिनिधित्व के कारणों की समीक्षा की जाए और इसका इतिहास 1947 से खंगाला जाए तो आपको इस बात का आसानी से पता चल जाएगा कि मुसलमानों की प्रगति की राह में किस तरह से रुकावटें पैदा की गईं.
निर्वाचित निकायों में मुसलमान
लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अलग-अलग धड़ों से इस बात को लेकर ख़ूब बावेला मचा कि संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है. यह दलील दी गई कि संसद में लोकसभा की 543 सीटें हैं और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक़, देश में मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत 13.4 है. इसलिए लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 543 का 13.4 फीसदी यानी 72.76 यानी 73 होना चाहिए. जबकि वर्ष 2009 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या केवल 30 (केवल 41 फीसदी) है और इस तरह उसे 43 सीटों का नुक़सान उठाना पड़ा. इस कमी की कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे कि सही नेतृत्व का अभाव, एकजुटता की कमी, वोट का बंटवारा, अशिक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी का अभाव वग़ैरह. लेकिन, दूसरे कारकों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ज़िम्मेवार हैं, वे राष्ट्रपति के दो अध्यादेश हैं. एक तो संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जाति) 1950 और दूसरा संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जनजाति) 1950 है. उक्त आदेश भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जारी किए थे. संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जाति) 1950 दरअसल हमारे पंथनिरपेक्ष संविधान की भावना का आपराधिक उल्लंघन है. यह आरक्षण की सुविधा को केवल हिंदू धर्म मानने वालों तक सीमित कर देता है. आरक्षण की सुविधा जिन अनुसूचित जनजातियों को दी गई है, सुदूर लक्षद्वीप के अपवाद को छोड़ दें तो मुसलमानों में उनका कहीं अस्तित्व नहीं है. संवैधानिक अध्यादेश (अनुसूचित जाति) 1950 के कारण हिंदू धर्म को छोड़ कर हर धर्म के अनुसूचित जाति के लोग आरक्षण के लाभ से वंचित हैं. इसलिए पूरे देश में इस अन्याय के ख़िला़फ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई. सिखों और बौद्धों ने तो इस आदेश के ख़िला़फ तीव्र विरोध जताया था. विभाजन के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि मुसलमान ख़ुद ही परेशानी में थे. लेकिन बौद्धों और सिखों के विरोध ने सरकार को आदेश में सुधार करने पर मजबूर कर दिया. सिखों को अनुसूचित जातियों की सूची में 1956 में और बौद्धों को 1990 में शामिल कर लिया गया. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 में धार्मिक आधार पर भेदभाव जारी ही रहा. इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो दलित पेशे से जुड़े हैं, छह दशक के बाद भी उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. मुसलमान अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश के कुल अनुसूचित जनजातियों की केवल 0.25 फीसदी ही होगी. ज़्यादातर लक्षद्वीप में हैं. वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक़, अनुसूचित जाति और जनजातियां मिलकर देश की कुल आबादी की 24 फीसदी
(अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत और जनजाति आठ प्रतिशत) होंगी. इसका मतलब यह है कि देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण क़रीब 24 फीसदी है. जबकि मुसलमान, जो कि संवैधानिक तौर पर आरक्षण का लाभ पाने के पात्र हैं, उन्हें 0.1 फीसदी भी आरक्षण की सुविधा हासिल नहीं है. विडंबना तो यह है कि जहां हिंदू, सिख और बौद्ध संवैधानिक रूप से 100 फीसदी (सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) सीटों या रिक्तियों के लिए कोशिश करते हैं तो मुसलमान केवल 76 फीसदी सीटों (सामान्य और अनुसूचित जनजाति, जिसका मुसलमानों में अस्तित्व ही नहीं है) की पात्रता रखते हैं. 1950 में प्रस्तुत राष्ट्रपति के इन अध्यादेशों और इनमें संशोधन के बाद संसद एवं विधानसभाओं में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध सीटों की जो स्थिति है, उसे हम साथ दी गई तालिका से समझ सकते हैं. (देखें तालिका)
सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उत्साहवर्द्धक नहीं है. इस बात का ज़िक्र सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है.
Adv from Sponsors