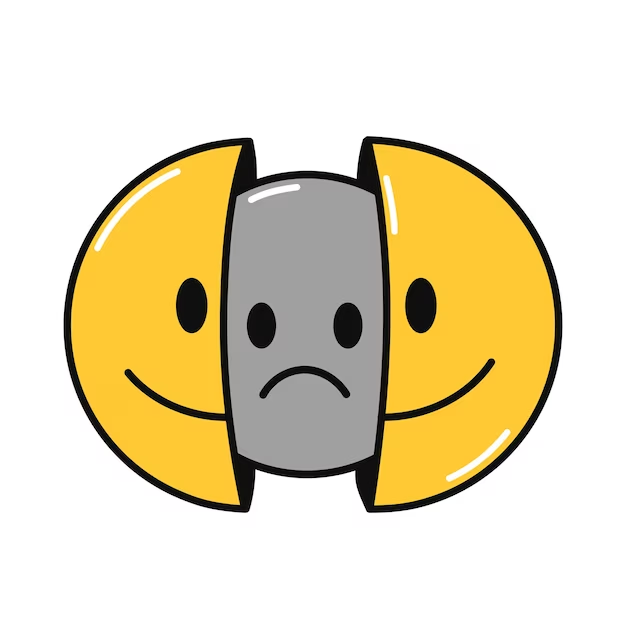भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के हाल के फैसले ने मीडिया में बहस छेड़ दी है. ख़ासकर उनमें जो इस फैसले के पक्ष में हैं और जो नैतिकता के आधार पर इसके विरोध में हैं कि यह संस्कृति, परंपरा और भारतीय समाज के ख़िला़फ है.
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के हाल के फैसले ने मीडिया में बहस छेड़ दी है. ख़ासकर उनमें जो इस फैसले के पक्ष में हैं और जो नैतिकता के आधार पर इसके विरोध में हैं कि यह संस्कृति, परंपरा और भारतीय समाज के ख़िला़फ है.
तथ्यों को समझने के लिए हमें दिल्ली हाईकोर्ट द्बारा दिए गए फैसले के आधार को समझना ज़रूरी है. एक स्वयंसेवी संस्था नाज़ फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईपीसी की धारा 377 की मान्यता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की. दावे का मुख्य आधार यह था कि आईपीसी की धारा 377, दो वयस्क और सहमत लोगों के बीच यौन संबंध पर रोक लगाकर उन मौलिक अधिकारों पर ही रोक लगा रही है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 और 21 में दी गई है. इस मामले में केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान (नाको, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ही आता है) के ज़रिए मुख्य प्रतिवादी बनाया गया था.
इसी रिट याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में इस आधार पर ख़ारिज़ कर दिया था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई का कोई आधार नहीं है और क़ानून की वैधानिकता को अकादमिक तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने तीन फरवरी 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से अलग यह व्यवस्था दी कि मामले पर विचार करने की ज़रूरत है और इसे ऊपर बताए गए आधार पर ख़ारिज़ करने की ज़रूरत नहीं थी. इस तरह मामला फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में गया और इस तरह यह ताज़ा फैसला आया.
दरअसल, विवाद की जड़ में आईपीसी की धारा 377 का वह दंडात्मक प्रावधान है, जो अप्राकृतिक सेक्स को आपराधिक मानता है. वह व्याख्या कुछ इस तरह की है-
अप्राकृतिक दोष- जो भी ऐच्छिक तौर पर प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत किसी दूसरे पुरुष, स्त्री या किसी जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, को उम्रक़ैद या फिर दस वर्ष से अधिक की क़ैद मिलेगी और ज़ुर्माना भी देना होगा.
समय की दरिया में जितना पानी बहा है, उसके साथ ही अप्राकृतिक यौन की व्याख्या भी बदली है. यह भले ही पश्चिमी समाज में अधिक हुआ है, जो दूसरों की तुलना में ख़ुद को अधिक उदारवादी दिखाना चाहता है. भारतीय संदर्भ में इसे यौन विकृति माना जाता है और भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है.
याचिकाकर्ता स्वयंसेवी संगठन नाज़ फाउंडेशन एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में काम कर रहा है. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह इस मुक़दमे को जनहित याचिका के तहत लाना चाहता था, क्योंकि एचआईवी/एड्स रोकने के प्रयास कई बार राज्यों की एजेंसियों द्वारा बाधित होते हैं, क्योंकि एजेंसियां समलैंगिकों और लिंग-रूपांतरित (ट्रांसजेंडर) लोगों के लिए भेदभाव का रवैया रखती हैं. यह काम वे आईपीसी की धारा 377 की आड़ में करतीं हैं, जिसका नतीजा होता है कि ऐसे लोग या समूह अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं. उनको गाली, शोषण, सार्वजनिक भर्त्सना और निजी तौर पर अपमान का सामना करना पड़ता है.
माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने और लिखित दलीलों व बयानों के आधार पर अपना फैसला सुनाया और विस्तार से उन सवालों पर व्यवस्था दी, जो सभी पक्षों ने उठाए थे. ख़ासकर इन संदर्भों में-
– क़ानून का इतिहास
-स्वयंसेवी संस्था को मिली चुनौतियां
-अनुच्छेद 21- किसी व्यक्ति के जीवन, उसके सम्मान, निजता और संप्रभुता का अधिकार
– निजता का अधिकारः आईपीसी की धारा 377 व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार में उल्लंघन
यौन और पहचान
–समलैंगिकों को अपराधी ठहराने का प्रभाव
–राज्य के बाधक हित
-सार्वजनिक स्वास्थ्य की राह में आईपीसी की धारा 377 एक बाधा
–मौलिक अधिकारों को रोकने में नैतिकता को आधार बनाना
-क्या धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14 के मुताबिक दिए गए समानता के अधिकार को बाधित करता है.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से भारत में और विदेशों में उच्चतर न्यायालयों द्वारा दी गई व्यवस्थाओं और क़ानूनों का उल्लेख किया. भारत में कुछ मील के फैसलों में मेनका गांधी का मामला, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, ए के ठाकुर और इंदिरा साहनी आदि शामिल हैं. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा –
-हम घोषणा करते हैं कि धारा 377-जहां तक आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच निजी तौर पर यौन-संबंध को आपराधिक बताता है-संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन करता है. आईपीसी की धारा 377 ग़ैर-सहमति के योनि से इतर संभोग के मामलों में लागू रहेगी ही, जिनमें अवयस्क शामिल हों. वयस्क से हमारा मतलब 18 वर्षों और उससे अधिक के सभी लोगों से है. 18 वर्षों से कम के किसी भी व्यक्ति से किसी यौन संबंध के लिए सहमति देना अपेक्षित नहीं है. यह व्याख्या तब तक मान्य है, जब तक संसद भारत के लॉ कमीशन की 172 वीं रिपोर्ट के प्रस्ताव को प्रभावी बनाने का प्रस्ताव नहीं लाती. यह प्रस्ताव काफी हद तक भ्रम को दूर करता है. दूसरी बात हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा फैसला उन मामलों को फिर से खोलने की वजह नहीं बननी चाहिए, जो धारा 377 के मुताबिक दर्ज़ हैं और अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं.
हाई कोर्ट के इस ़फैसले ने भानुमति का पिटारा खोल दिया है, क्योंकि फैसले के बाद मीडिया में इस मसले पर विचारकों की बाढ़ आ गई है. फैसले के पक्ष और विपक्ष में जमकर लेख लिखे जा रहे हैं, बहसें हो रही है. इसमें संदेह नहीं कि हाईकोर्ट इस फैसले पर संवैधानिक प्रावधानों और मौलिक अधिकारों पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही पहुंचा होगा. हालांकि, काफी हद तक यह भी महसूस किया जा रहा है कि भारतीय समाज की तुलना किस तरह पश्चिमी समाज से की जा सकती है, जहां नैतिक मूल्य दिन पर दिन पतनशील हैं. हम भारतीय अपनी नैतिकता को सबसे ऊपर मानते हैं, और कुछ भी अगर प्रकृति के ख़िला़फ है, तो वह अनैतिक है. काफी हद तक बात सही भी है. भारतीय संदर्भ में नैतिकता की जांच बिल्कुल आसान है- क्या उस विषय पर बच्चों और अभिभावकों के बीच बिना किसी हिचक के बहस हो सकती है? अधिकतर घरों में अगर टीवी पर आमतौर पर भी यौनिकता-खासकर, समलैंगिकता-पर बहस हो रही होती है, तो या तो अभिभावक या फिर बच्चे रिमोट तलाश कर तुरंत ही किसी सुरक्षित(?) चैनल को देखने लगते हैं. इस मसले को तो जाने ही दें. टीवी पर थोड़ा-बहुत नंगापन आने पर भी हम लोग एक-दूसरे से नज़रें चुराने लगते हैं.
इन हालातों में समलैंगिकता के पूरे मसले को नैतिकता की कसौटी पर कसना होगा, न कि केवल अकादमिक और संवैधानिक स्तर पर बहस करनी होगी. सरकार को भी अपना रुख़ बहुत साफ न रखने का दोषी ठहराया जाना चाहिए. केंद्रीय सरकार का भ्रमित और विरोधाभासी रुख कोर्ट में दाख़िल इसके दो मंत्रालयों के हलफनामों से ही स्पष्ट हो जाता है. यहां तक कि हाईकोर्ट ने अपने ़फैसले में इस बात को रेखांकित किया कि गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों ने परस्पर विरोधाभासी हलफनामे दायर किए. गृह मंत्रालय ने धारा 377 को लागू करने को जायज़ ठहराया, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि धारा 377 की वजह से एचआईवी/ एड्स रोकने की कोशिशों को चोट पहुंच रही है. गृह मंत्रालय की दलील मुख्यतः सार्वजनिक नैतिकता पर आधारित थी.
संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार इस मसले पर अपना रुख़ साफ करे और ऊहापोह की नीति न अपनाए. सरकार को जल्द से जल्द इस मसले पर एक स्वस्थ बहस शुरू करनी चाहिए, जिसमें न केवल नाज़ फाउंडेशन जैसे एनजीओ शामिल हों, बल्कि समाज के हरेक तबके जैसे-धार्मिक प्रमुखों, विद्वानों और शिक्षाशास्त्रियों आदि भी को शामिल करना चाहिए. इसके बाद ही हम एक संतुलित फैसला दे सकेंगे, वरना हम ऐसे द्वंद्व में फंसेंगे जहां ऊपरी तौर पर भले हम उदारवादी दिखें, लेकिन आंतरिक तौर पर हम अपने नैतिक मूल्यों और परंपराओं को किसी भी दूसरी बात से अधिक महत्व देते हों.
हाईकोर्ट ने निजी स्थलों पर वयस्कों के बीच आपसी सहमति से यौन-संबंध की अनुमति दी है, पर इस ़फैसले के बाद हम गे और लेस्बियन के विजय-जुलूस निकलते हुए देख रहे हैं. इनके समर्थन में तथाकथित एक्टिविस्ट के लेखों और बहसों की बाढ़ आ गई है. ये कार्यकर्ता जो भूल रहे हैं, वह यह कि इस तथाकथित अल्पसंख्यक समूह-जिसे अप्राकृतिक और बीमार माना जाता है- के समर्थन में लिखकर या चिल्लाकर हम उन छोटे बच्चों के दिमाग़ को प्रदूषित कर रहे हैं, जो इस तरह के लेख या टीवी पर ऐसे विज़ुअल्स देख रहे हैं.
जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी पारिस्थितिकी को बचाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी आनेवाली पीढ़ी को एक स्वस्थ पर्यावरण नसीब हो, वही बात नैतिक मूल्यों के साथ भी सही है. हमें आने वाली पीढ़ी को अच्छे नैतिक मूल्य देने की भी ज़रूरत है.
» लेखक सुप्रिम कोर्ट के वकील है
फैसले को सामाजिक मूल्यों और संस्कृति के आईने में देखें
Adv from Sponsors