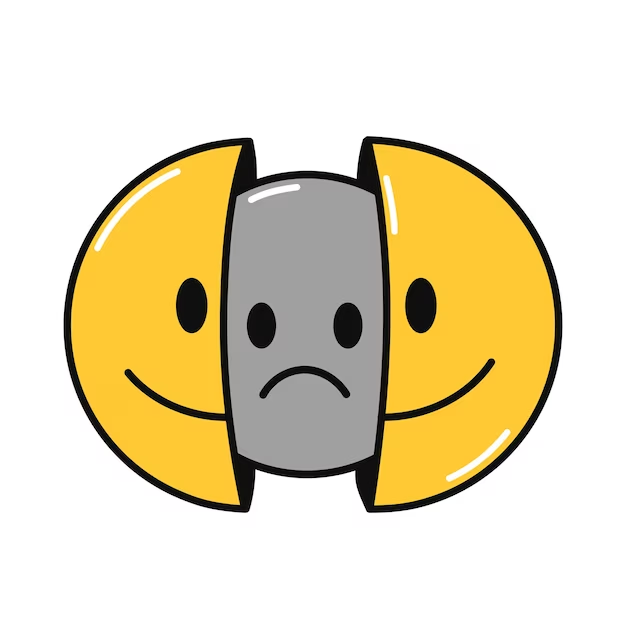बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का एकजुट होना भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार से ऐसा लगने लगा है कि अब वह इस स्थिति में नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी से दो-दो हाथ कर सके. भाजपा को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने अपने धुर विरोधी लालू यादव से हाथ मिलाया है. कांग्रेस ने इस मौ़के का फ़ायदा उठाया और वह भी इस महा-गठबंधन में शामिल हो गई. अब सवाल यह है कि क्या लालू, नीतीश और कांग्रेस का महा-गठबंधन भाजपा को बिहार में रोक पाएगा? क्या यह उपचुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? और, क्या यह महा-गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा बदल पाने में सक्षम है?
 बिहार में अभी चुनाव भी नहीं हुए और महा-गठबंधन के विरोधाभास सामने आने लगे हैं. अभी विधानसभा चुनाव होने में एक साल से ज़्यादा समय बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर महा-गठबंधन के अंदर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का यह महा-गठबंधन विरोधाभासों का पुलिंदा है. इस महा-गठबंधन को सफल बनाने के लिए विरोधाभासों को ख़त्म करना होगा. दस विधानसभा सीटों के लिए हो रहे इस उपचुनाव में चार-चार सीटों पर जदयू और राजद के उम्मीदवार हैं, वहीं दो सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है. महा-गठबंधन को सफल होने के लिए उन्हें 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी. अगर मुकाबला बराबरी का रहा यानी स़िर्फ पांच सीटें मिल पाती हैं, तो इस महा-गठबंधन का प्रयोग सफल नहीं माना जाएगा और अगर इस गठबंधन को पांच से कम सीटें मिलती हैं, तो इस प्रयोग पर उपचुनाव के बाद ही विराम लग जाएगा. कहने का मतलब यह कि महा-गठबंधन अपने विरोधाभासों और चुनौतियों के बीच ऐसा फंसा है कि छोटी-सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है. एक छोटी-सी भूल और एक ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान बिहार की राजनीति सदा के लिए बदल सकता है.
बिहार में अभी चुनाव भी नहीं हुए और महा-गठबंधन के विरोधाभास सामने आने लगे हैं. अभी विधानसभा चुनाव होने में एक साल से ज़्यादा समय बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर महा-गठबंधन के अंदर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का यह महा-गठबंधन विरोधाभासों का पुलिंदा है. इस महा-गठबंधन को सफल बनाने के लिए विरोधाभासों को ख़त्म करना होगा. दस विधानसभा सीटों के लिए हो रहे इस उपचुनाव में चार-चार सीटों पर जदयू और राजद के उम्मीदवार हैं, वहीं दो सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है. महा-गठबंधन को सफल होने के लिए उन्हें 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी. अगर मुकाबला बराबरी का रहा यानी स़िर्फ पांच सीटें मिल पाती हैं, तो इस महा-गठबंधन का प्रयोग सफल नहीं माना जाएगा और अगर इस गठबंधन को पांच से कम सीटें मिलती हैं, तो इस प्रयोग पर उपचुनाव के बाद ही विराम लग जाएगा. कहने का मतलब यह कि महा-गठबंधन अपने विरोधाभासों और चुनौतियों के बीच ऐसा फंसा है कि छोटी-सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं है. एक छोटी-सी भूल और एक ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान बिहार की राजनीति सदा के लिए बदल सकता है.
अगर चुनाव का रिश्ता स़िर्फ अंकगणित से होता, तो बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आज ही पता चल जाता. जैसा कि कई राजनीतिक विश्लेषक और अख़बारों में लिखने वाले धुरंधर बता रहे हैं कि बिहार में बना लालू-नीतीश-कांग्रेस का महा-गठबंधन एक अजेय गठबंधन है. कई टीवी चैनलों ने भी आंकड़े दिखाकर यही दलील दी है. इन सबके मुताबिक, लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन में भाजपा को 29.4 फ़ीसद, राम विलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6.4 फ़ीसद और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 3 फ़ीसद वोट मिले. यानी भाजपा गठबंधन को कुल 38.8 फ़ीसद वोट मिले. जबकि लालू यादव के राजद को 20.1 फ़ीसद, नीतीश कुमार के जदयू को 15.8 फ़ीसद और कांग्रेस को 8.4 फ़ीसद वोट मिले. मतलब यह कि लालू, नीतीश और कांग्रेस के वोट एक साथ जोड़ दिए जाएं, तो वे 44.3 फ़ीसद होते हैं, जो भाजपा गठबंधन से काफी ज़्यादा हैं. इसी दलील को मानते हुए लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए यह महा-गठबंधन तैयार किया है. उन्हें विश्वास है कि भाजपा को रोकने का यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चुनाव का रिश्ता अंक गणित से ज़्यादा बीज गणित से होता है. हर चुनाव का एक एक्स फैक्टर होता है, जो चुनाव में हार और जीत का फैसला करता है. जो राजनीतिक दल और विश्लेषक इस एक्स फैक्टर को चिन्हित करने में कामयाब हो जाते हैं, वही चुनाव का सही आकलन करते हैं और वही जनता की नब्ज समझ पाते हैं.
बिहार का उपचुनाव राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतुहल का विषय है. लालू यादव के सामने अपनी खोई ज़मीन तलाशने और बिहार की राजनीति के केंद्र में आने का मौक़ा है. उन्होंने अपने सबसे प्रखर विरोधी नीतीश कुमार से इसलिए हाथ मिलाया, क्योंकि इस गठबंधन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें ही मिलने वाला है.
बिहार की राजनीति का प्रतिमान बदल चुका है. 2005 से पहले बिहार में 15 सालों तक अंधकार युग था. लालू यादव का एकछत्र राज था. वह चारा घोटाले में फंसे, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया. न कोई विरोध हुआ, न कोई सुगबुगाहट हुई. बिहार में क़ानून का शासन नहीं था, जंगलराज था. आपराधिक घटनाएं ऐसी कि बिहार के बाहर के लोगों को बताया जाए, तो वे विश्वास न करें. सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो चुका था. पुलिस का कोई खास रोल नहीं था, क्योंकि खुलेआम हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध अंजाम दिए जाते थे. दरअसल, उस अंधकार युग में यह सब जीवन का हिस्सा बन चुका था. लोग त्रस्त थे. आज भी लालू युग को याद करते ही बिहार के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन जब भी चुनाव होता था, लालू यादव आसानी से जीत जाते थे. एक तरफ़ अदम्य मुस्लिम-यादव वोट बैंक था, तो दूसरी तरफ़ पार्टी नेताओं की दबंगई थी. कोई विरोधी मैदान में टिक नहीं पाता था. इसी जंगलराज के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जनता का समर्थन मिला. लोगों ने लालू यादव को बिहार की राजनीति में अलग-थलग कर दिया. उनकी पार्टी को चुनाव में लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव इतनी भी सीटें नहीं जीत सके कि वह नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी कर सकें. सवाल यह है कि क्या लालू यादव अगले एक साल में बिहार की जनता के मस्तिष्क से जंगलराज वाली छवि ख़त्म कर सकेंगे? क्या बिहार की आम जनता लालू यादव पर भरोसा कर पाएगी? बिहार में इस महा-गठबंधन के चुनाव जीतने के लिए यही पहली और आख़िरी शर्त है.
नीतीश कुमार 1994 से लालू यादव का विरोध कर रहे हैं. बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति वास्तव में लालू विरोध की राजनीति रही है. दोनों में स़िर्फ राजनीतिक विरोध ही नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक दुश्मनी व्यक्तिगत दुश्मनी की भी शक्ल ले चुकी थी. कई सालों तक दोनों के बीच संवाद तक नहीं रहा. 15 सालों के जंगलराज के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इसलिए बने, क्योंकि बिहार के लोगों ने उन्हें लालू विरोधी मुहिम के नेता के रूप में स्वीकार किया. ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि वह बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाएंगे, विकास करेंगे. चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की. जिस तरह लालू यादव मुस्लिम-यादव वोट बैंक की बदौलत चुनाव जीतते रहे, उसी तरह नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़ा-महादलित-मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की. नीतीश कुमार की यह योजना ज़मीनी हकीकत नहीं बन सकी. नीतीश कुमार 2004 के बाद से जो चुनाव जीत रहे हैं, उसकी बुनियाद दरअसल लालू विरोध ही रहा. पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार की राजनीति का मुख्य मुद्दा नरेंद्र मोदी का विरोध रहा. यह राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से रहा. नीतीश कुमार ने मुसलमानों को अपने समर्थन में करने के लिए मोदी का विरोध किया, साथ ही वह खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए भी वह मोदी का विरोध करते रहे. एनडीए में रहते हुए उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय पर आपत्ति दर्ज की, लेकिन जब ऐसा लगा कि भाजपा मोदी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी, तब उन्होंने भाजपा से रिश्ते तोड़ लिए. पार्टी के नेताओं का मानना है कि भाजपा से अलग होने का ़फैसला नीतीश कुमार का व्यक्तिगत फैसला था.
भ्रष्टाचार और कुशासन जैसे हथियार से एक मजबूत विरोधी को पराजित करने की रणनीति कामयाब होना मुश्किल है. उपचुनाव के नतीजों का असर 2015 के विधानसभा चुनाव से ज़्यादा जदयू और कांग्रेस पर होगा. वैसे भी अक्सर यह देखा गया है कि दो ध्रुवीय चुनाव में नतीजे निर्णायक होते हैं. हार और जीत की तस्वीर साफ़ होती है.
नीतीश कुमार की मुसीबत यह है कि उनका भाजपा से अलग होने का फैसला जदयू के लिए काफी हानिकारक साबित हुआ. लोकसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतने का दमखम रखने वाली पार्टी मात्र दो सीटों में सिमट गई. पार्टी के नेता इस हार के लिए नीतीश कुमार को दोषी मानते हैं. अब नीतीश कुमार की राजनीति का केवल एक ही केंद्रीय बिंदु है कि उन्हें भाजपा से अलग होने का फैसला सही साबित करना है. नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर विधायकों और पार्टी के स्थानीय नेताओं में नाराज़गी है. अब नीतीश कुमार और शरद यादव ने इस फैसले को सही साबित करने के लिए लालू यादव से भी हाथ मिला लिया. पार्टी के नेता अब और भी गुस्से में हैं. नाराज़गी इस कदर है कि उपचुनाव के बाद पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो सकता है. जदयू के विधायकों की दुविधा यह है कि वे बिहार में लालू का जंगलराज ख़त्म करने का वादा करके चुनाव जीते थे और अब लालू यादव के साथ मिलकर वोट किस तरह मांग सकेंगे. जदयू के कई विधायक तो अब नीतीश कुमार और इस महा-गठबंधन के ख़िलाफ़ मुखर हो गए हैं. ख़बर यह है कि जदयू के 116 विधायकों में बहुमत ऐसे विधायकों का है, जो इस उपचुनाव यानी 25 अगस्त के बाद स्वतंत्र रूप से ़फैसला लेंगे. उन्होंने पार्टी के अंदर नीतीश कुमार और शरद यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाने का मन बना लिया है. नीतीश कुमार की समस्या यह है कि यदि उपचुनाव में जदयू के चारों उम्मीदवार हार गए, तो वह पार्टी का विघटन नहीं रोक पाएंगे और अगर चारों उम्मीदवार जीत गए, तो फिर पार्टी का विघटन विधानसभा चुनाव तक टल जाएगा. नीतीश कुमार के लिए महा-गठबंधन के जरिये चुनाव जीतना ज़रूरी है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है, जिसके जरिये वह अपने विधायकों, नेताओं एवं समर्थकों को जवाब दे सकते हैं कि भाजपा से अलग होने का उनका फैसला सही था.
लालू यादव के लिए 2014 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा झटका था. उनके सारे दावे झूठे साबित हुए. लोकसभा चुनाव से पहले तो कई विश्लेषक और सर्वे लालू यादव को 20 सीटें देने को तैयार थे. वजह यह थी कि चुनाव से कुछ दिन पहले वह जेल से छूटकर बाहर आए. कई लोग यह मानकर बैठ गए कि बिहार में लालू के लिए सहानुभूति लहर है. कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद उनकी स्थिति मजबूत हो गई है. ये ख़बरें मीडिया में आने लगीं. लेकिन, जब नतीजे आए, तो पता चला कि लालू यादव के परिवार का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत सका. आरजेडी स़िर्फ चार सीटों में सिमट गई. जो जीता भी, वह लालू यादव की वजह से नहीं, बल्कि अपने दमखम की वजह से. उन चारों उम्मीदवारों की जीत में लालू यादव का कोई खास योगदान नहीं है. सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों की मानें, तो लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम वोट बैंक लालू के साथ थे, सहानुभूति लहर थी और लालू विरोधी पार्टियां भी बंटी हुई थीं. फिर भी लालू यादव को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा. बिहार की जनता का फैसला लालू यादव के जातीय समीकरण और उनकी राजनीति पर भारी पड़ गया.
सीधे शब्दों में कहें, तो बिहार में लालू यादव भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, परिवारवाद और जंगलराज के पर्याय हैं. बिहार की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है. पार्टी के कई बड़े-बड़े नेता लालू यादव से अलग हो चुके हैं. रघुवंश बाबू और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कुछ लोग पार्टी में ज़रूर हैं, लेकिन जबसे लालू यादव ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है, तबसे वह शिथिल पड़े हुए हैं. 15 सालों तक बिहार की राजनीति पर प्रभुत्व रखने वाली पार्टी लोकसभा चुनाव में महज 4 सीटों में सिमट गई. अगर लालू उपचुनाव में भी हारते हैं, तो उनकी पार्टी के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा. पार्टी से पलायन का दौर शुरू होगा. महा-गठबंधन में शामिल होने की लालू यादव की रणनीति पार्टी को बचाए रखने के लिए है. वैसे आकलन यही है कि महा-गठबंधन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लालू यादव को होगा, लेकिन उनकी चुनौती यह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में दावेदारी बनाए रखने मात्र के लिए उन्हें इस उपचुनाव में चारों सीटों पर विजय हासिल करनी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इस महा-गठबंधन का औचित्य ख़त्म हो जाएगा.
बिहार का उपचुनाव राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतुहल का विषय है. लालू यादव के सामने अपनी खोई ज़मीन तलाशने और बिहार की राजनीति के केंद्र में आने का मौक़ा है. उन्होंने अपने सबसे प्रखर विरोधी नीतीश कुमार से इसलिए हाथ मिलाया, क्योंकि इस गठबंधन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें ही मिलने वाला है. भाजपा के लिए यह उपचुनाव अपनी शक्ति का आकलन करने का अवसर है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. भाजपा से अलग होकर लोकसभा चुनाव में वह बुरी तरह हार चुके हैं. पार्टी में उनके ़फैसले का कड़ा विरोध है. नीतीश कुमार के लिए यह उपचुनाव भाजपा से अलग होने के फैसले को सही साबित करने का आख़िरी मा़ैका है. यही वजह है कि देश के राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न राजनीतिक दलों की नज़र बिहार पर टिकी हुई है, लेकिन बिहार की जनता में इस उपचुनाव को लेकर ज़्यादा हलचल नहीं है. जहां तक मतदान की बात है, तो इस उपचुनाव का असर 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला. बिहार की जनता एवं मतदाता राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व हैं. वे इस उपचुनाव का महत्व समझते हैं.
उपचुनाव के नतीजे का असर सरकार पर नहीं पड़ने वाला है. कोई जीते या हारे, बिहार में सरकार पर कोई ख़तरा नहीं है और न कोई नई सरकार बनने वाली है. इसलिए अन्य चुनावों से इस उपचुनाव में राजनीतिक माहौल थोड़ा उदासीन ही रहने वाला है. अगर इसके नतीजे से सरकार पर असर पड़ता दिखाई देता, तो उपचुनाव का माहौल इतना उदासीन नहीं होता. लोगों की हिस्सेदारी कम है, चुनावी माहौल नहीं है. इससे लगता है कि इस उपचुनाव में पिछले चुनावों से कम मतदान होगा. इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह उपचुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है.
भ्रष्टाचार और कुशासन जैसे हथियार से एक मजबूत विरोधी को पराजित करने की रणनीति कामयाब होना मुश्किल है. उपचुनाव के नतीजों का असर 2015 के विधानसभा चुनाव से ज़्यादा जदयू और कांग्रेस पर होगा. वैसे भी अक्सर यह देखा गया है कि दो ध्रुवीय चुनाव में नतीजे निर्णायक होते हैं. हार और जीत की तस्वीर साफ़ होती है. अगर चुनाव में त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला होता है, तो नतीजे निर्णायक नहीं होते. ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए बहुमत हासिल करना मुश्किल हो जाता है. बिहार में महा-गठबंधन बनने के बाद यह तय हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी एक गठबंधन को बहुमत मिलेगा. अब इस चुनौती को भाजपा बिहार में किस तरह लेती है, यह उसकी तैयारी पर निर्भर करता है, क्योंकि भाजपा की मुसीबत यह है कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को लेकर लोग उदासीन हो गए हैं. दिल्ली में नई सरकार तो आ गई, लेकिन उसकी चाल और चरित्र दोनों ही पुरानी सरकारों की तरह हैं, इसलिए बिहार का उपचुनाव राजनीतिक युद्ध से ज़्यादा मानसिक युद्ध में तब्दील हो चुका है. अगले एक साल तक जो भी गठबंधन अपने विरोधाभासों पर नियंत्रण लगा पाएगा और मनोबल ऊंचा रखने में कामयाब रहेगा, वही बिहार में अगली सरकार बनाएगा.
नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन विरोधाभासों का भंडार तो है ही, साथ ही आत्मविश्वास की भी कमी है. बिहार की राजनीति में भाजपा हमेशा तीसरे और चौथे स्थान पर रही. लालू, नीतीश और कांग्रेस को महा-गठबंधन बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया है कि भाजपा को चुनाव में पराजित करना मुश्किल है. नीतीश कुमार को अगर भाजपा को हराना था, तो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए सुशासन को आगे लेकर जाना था, भ्रष्टाचार और अपराधों पर लगाम लगाना था, विकास के नए आयाम रचने थे और लोगों का विश्वास जीतना था, लेकिन उन्होंने पहले भाजपा से रिश्ते तोड़कर अपने मतदाताओं को नाराज़ किया और फिर मुख्यमंत्री पद छोड़कर सरकार की साख ख़त्म कर दी. आपराधिक घटनाओं में तेजी आ गई. लोग अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं फिर से बिहार में जंगलराज की वापसी न हो जाए. नीतीश कुमार लगातार गलत फैसले के शिकार हो रहे हैं. बिहार में भाजपा को रोकने के लिए बने इस महा-गठबंधन की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. वह इसलिए, क्योंकि आम मतदाता लालू युग की वापसी नहीं चाहते. बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा में बुनियादी बदलाव आ चुका है. जाति और धर्म के नाम पर होने वाले मतदान की अपनी सीमाएं हैं, जो पिछले कुछ चुनावों से टूट रही हैं. युवा मतदाता जाति और धर्म के आधार पर मतदान नहीं करते. लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में यादव वोट लालू यादव के हाथ से बाहर चला गया और कुर्मी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ मतदान किया. यही वजह है कि जातीय समीकरण के आधार पर किसी भी गठबंधन की जीत या हार का आकलन भ्रामक है. 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर महा-गठबंधन में लालू यादव का पलड़ा भारी रहा, उनके उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हुई और चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, तो इस महा-गठबंधन को लोग लालू यादव के जंगलराज की वापसी के रूप में देखेंगे.