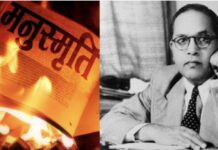उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर बीसवीं सदी के मध्य तक भारत ने कई महान सपूत पैदा किये जो न सिर्फ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े बल्कि तमाम तरह के शोषण के ख़िलाफ़ और समतामूलक समाज बनाने में अपने आप को ‘होम’ कर दिया। ऐसे ही एक महान सपूत और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे आचार्य नरेंद्र देव।असाधारण और विलक्षण प्रतिभा के धनी भारत के प्रमुख बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, विधायक एवं सांसद रहे आचार्य नरेंद्र देव की आज 69वीं पुण्यतिथि है।वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी आंदोलन के अध्येता क़ुरबान अली की आचार्य जी को श्रद्धांजलि।
आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवाद का पितामह कहा जाता है। वे सही मायनों में भारतीय समाजवाद के पितामह थे। बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व, शालीन आचरण और प्रांजल भाषा, चेहरे से टपकती ममता, करुणा और प्यार।सादगी की ऐसी प्रतिमूर्ति कि जो एक बार उनके संपर्क में आया वो हमेशा के लिए आचार्य जी का होकर रह गया और आचार्य जी उसके।राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब महात्मा गांधी की आँख के तारे कहे जाने वाले आचार्य जी ने कहा की केवल गांधीजी की अहिंसक विचारधारा और शांतिपूर्ण तरीक़ों से देश आज़ाद नहीं हो सकता और इसके लिए उन्होंने हिंसा तथा उग्रवाद का समर्थन भी किया लेकिन तब भी आचार्य जी की भाषा आक्रामक नहीं हुई और गांधीजी के प्रति उनमें कोई तल्ख़ी नहीं आयी।देश को स्वतंत्र कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आन्दोलन में खींच लाया और भारत की आर्थिक दशा व गरीबों की दुर्दशा ने उन्हें समाजवादी बना दिया।हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, बंगला, संस्कृत, प्राकृत, पाली, जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं के जानकार आचार्य जी का अध्ययन अत्यंत विशाल और अध्यापन शैली अत्यंत सरल थी।
1911 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ए., 1913 में बनारस के क़ुईन्स कॉलेज से एम.ए. और 1915 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. करने के बाद आचार्य जी ने फै़जाबाद (उ.प्र.) में अपने पिता की तरह वकालत शुरू की। इसी के आसपास वे राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतकार आचार्य नरेंद्र देव राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ चिंतक और मनीषी भी थे।बाल गंगाधर तिलक और महर्षि योगी अरविंद के संपर्क में आने के बाद वे भारत की स्वाधीनता के लिए समर्पित हो गए। उनके चिंतन पर स्वामी रामतीर्थ, श्रीमती एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय का भी गहरा असर था। 1920 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी।राजनीति के साथ-साथ वे इतिहास, समाजशास्त्र और शिक्षाशास्त्र के भी विद्वान थे। सच्चे अर्थों में वे एक शिक्षक ही थे। पं. जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वे काशी विद्यापीठ में 1921 में अध्यापन करने लगे और बाद में उसके कुलपति भी बने।
विद्यापीठ में सेवाकाल को अपनी अक्षुण्ण पूंजी स्वीकारते हुए, उन्होंने अपने ‘संस्मरणनों’ में लिखा है, “मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं – एक पढ़ने-लिखने की और, दूसरी राजनीति की, और इन दोनों में संघर्ष रहता है। यदि इन दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाए तो मुझे बड़ा परितोष रहता है और यह सुविधा मुझे विद्यापीठ में मिली। इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा था जो विद्यापीठ की सेवा में गुज़रा।अपनी जिंदगी पर एक निगाह डालने से मालूम होता है कि जब मेरी आंखें मुंदेंगी तो मुझे एक परितोष होगा कि जो काम मैंने विद्यापीठ में किया वह स्थायी है।”
 काशी विद्यापीठ में अध्यापन करने के बाद वे 1947 से 1951 तक लखनऊ विश्वविद्यालय और 1951 से 1953 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।एक अध्यापक के तौर पर वे मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन की ओर उन्मुख हुए। महात्मा गाँधी का सानिध्य उनके लिए युगांतकारी सिद्ध हुआ और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गए।वे समाजवाद के सूत्रधार बने और उसके सिद्धान्त के रचनाकार भी।आचार्यजी, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया के साथ समाजवाद का त्रिभुज कहे जाते थे।1934 में आचार्य जी ने जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ‘कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी’ की स्थापना की और उसके पहले सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस से बाहर आने पर 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ उसकी अध्यक्षता भी आचार्य जी ने ही की। समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का वही स्थान रहा है जो एक परिवार में मुखिया का होता है।
काशी विद्यापीठ में अध्यापन करने के बाद वे 1947 से 1951 तक लखनऊ विश्वविद्यालय और 1951 से 1953 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।एक अध्यापक के तौर पर वे मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन की ओर उन्मुख हुए। महात्मा गाँधी का सानिध्य उनके लिए युगांतकारी सिद्ध हुआ और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गए।वे समाजवाद के सूत्रधार बने और उसके सिद्धान्त के रचनाकार भी।आचार्यजी, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया के साथ समाजवाद का त्रिभुज कहे जाते थे।1934 में आचार्य जी ने जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ‘कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी’ की स्थापना की और उसके पहले सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस से बाहर आने पर 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ उसकी अध्यक्षता भी आचार्य जी ने ही की। समाजवादी आंदोलन में आचार्य नरेंद्र देव का वही स्थान रहा है जो एक परिवार में मुखिया का होता है।
 समाजवादी विचारों के प्रचार-प्रसार हेतु उन्होंने लखनऊ से ‘संघर्ष’ (साप्ताहिक) पत्रिका का संपादन किया और ‘जनवाणी’ के जरिए शिक्षण पद्धति और शिक्षकों की स्थिति का विवेचन किया।आचार्य जी ने “विद्यापीठ” त्रैमासिक पत्रिका, “समाज” त्रैमासिक और “समाज” साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया। इनमें जो लेख, टिप्पणियाँ वगैरह समय-समय पर प्रकाशित हुए उनके संग्रह हैं: ‘राष्ट्रीयता और समाजवाद’, ‘समाजवाद-लक्ष्य तथा साधन’(भाषण संग्रह) ‘राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास’, ‘समाजवाद और राष्ट्रीय क्रांति’, ‘सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद’, ‘भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास’, ‘युद्ध और भारत’, ‘किसानों के सवाल’ आदि। इसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार और नई संस्कृति के आवाहन के लिए संपादक का दायित्व ओढ़ते हुए राष्ट्रीय पत्रकारिता को भी गति प्रदान की। वे ‘जनवाणी, ‘संघर्ष’, ‘जनता, ‘समाज’ आदि पत्रिकाओं के संपादन और प्रकाशन से भी जुड़े रहे।
समाजवादी विचारों के प्रचार-प्रसार हेतु उन्होंने लखनऊ से ‘संघर्ष’ (साप्ताहिक) पत्रिका का संपादन किया और ‘जनवाणी’ के जरिए शिक्षण पद्धति और शिक्षकों की स्थिति का विवेचन किया।आचार्य जी ने “विद्यापीठ” त्रैमासिक पत्रिका, “समाज” त्रैमासिक और “समाज” साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया। इनमें जो लेख, टिप्पणियाँ वगैरह समय-समय पर प्रकाशित हुए उनके संग्रह हैं: ‘राष्ट्रीयता और समाजवाद’, ‘समाजवाद-लक्ष्य तथा साधन’(भाषण संग्रह) ‘राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास’, ‘समाजवाद और राष्ट्रीय क्रांति’, ‘सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद’, ‘भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास’, ‘युद्ध और भारत’, ‘किसानों के सवाल’ आदि। इसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार और नई संस्कृति के आवाहन के लिए संपादक का दायित्व ओढ़ते हुए राष्ट्रीय पत्रकारिता को भी गति प्रदान की। वे ‘जनवाणी, ‘संघर्ष’, ‘जनता, ‘समाज’ आदि पत्रिकाओं के संपादन और प्रकाशन से भी जुड़े रहे।
बौद्ध दर्शन के अध्ययन में आचार्य जी की विशेष रुचि रही है। नैतिक व्यवस्था की स्थापना में नास्तिक नरेंद्र देव जी धर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना।आजीवन वे बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते रहे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में “बौद्ध-धर्म-दर्शन” उन्होंने पूरा किया और “अभिधर्मकोश” भी प्रकाशित कराया।साथ ही “अभिधम्मत्थसंहहो” का हिंदी अनुवाद भी किया। प्राकृत तथा पाली व्याकरण हिंदी में तैयार किया।बौद्ध दर्शन के पारिभाषिक शब्दों के कोश का निर्माण कार्य भी उन्होंने शुरू किया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आचार्य जी ने पेरुंदुराई में एक व्याख्यात्मक कोश भी बनाया था, किंतु उनके आकस्मिक निधन से यह काम पूरा न हो सका।
 इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति, संस्कृति, भाषा आदि के संदर्भ में उनकी अपनी विशिष्ट सोच थी। उनकी बौद्धिक प्रखरता और पांडित्य से प्रभावित होकर ही उनके एक अन्यतम साथी श्रीप्रकाश ने उन्हें ‘आचार्य’ कहना शुरू कर दिया था। उनकी समस्त रचनाओं का संकलन तीन खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में पाठ्य पुस्तकों की कमी को देखते हुए, उन्होंने अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, इटली आदि देशों का इतिहास भी लिखा।उत्तर-प्रदेश शासन ने 1937 में गठित शिक्षा-सुधार समिति का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया था।उनके शिष्यों में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी और सोशलिस्ट नेता राजनारायण तथा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे।चंद्रशेखर तो आचार्य जी की प्रेरणा से ही राजनीति में आए और अंत तक उन्हें अपना गुरु मानते रहे।एक अध्यापक, चिन्तक, मनीषी और समाजवादी नेता के रूप में आजादी के आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आचार्य जी का अप्रतिम योगदान है।
इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति, संस्कृति, भाषा आदि के संदर्भ में उनकी अपनी विशिष्ट सोच थी। उनकी बौद्धिक प्रखरता और पांडित्य से प्रभावित होकर ही उनके एक अन्यतम साथी श्रीप्रकाश ने उन्हें ‘आचार्य’ कहना शुरू कर दिया था। उनकी समस्त रचनाओं का संकलन तीन खंडों में प्रकाशित हुआ है। हिंदी में पाठ्य पुस्तकों की कमी को देखते हुए, उन्होंने अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, इटली आदि देशों का इतिहास भी लिखा।उत्तर-प्रदेश शासन ने 1937 में गठित शिक्षा-सुधार समिति का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया था।उनके शिष्यों में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी और सोशलिस्ट नेता राजनारायण तथा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे।चंद्रशेखर तो आचार्य जी की प्रेरणा से ही राजनीति में आए और अंत तक उन्हें अपना गुरु मानते रहे।एक अध्यापक, चिन्तक, मनीषी और समाजवादी नेता के रूप में आजादी के आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में आचार्य जी का अप्रतिम योगदान है।

राजनीति के अलावा, आचार्य जी की दूसरी प्रवृत्ति, उन्हीं के शब्दों में, “लिखने पढ़ने की ओर” रही। इस दिशा में आचार्य नरेंद्र देव जी का योगदान अत्यंत महत्व का है। विद्यापीठ के द्वारा पिछले वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्व का काम हुआ है, उसकी आज भी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की खोज ही चल रही है, विशेष उपयोगिता है। काशी विद्यापीठ के अध्यापक, आचार्य और कुलपति की हैसियत से आपने अपनी विद्वत्ता, उदारता और चरित्र के द्वारा अध्यापन और प्रशासन का जो उच्च आदर्श कायम किया है, वह अनुकरणीय है।
आचार्य जी मूलतः मार्क्सवादी समाजवादी थे और चिंतन-पद्धति के रूप में मार्क्सवाद को मानने थे।आचार्य जी ने एक मौके पर कहा भी कि ‘वे पार्टी छोड़ सकते हैं पर मार्क्सवाद नहीं।’ वे मार्क्सवाद और भारत की पराधीन दुनिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई विरोध नहीं देखते थे।वैसे ही वे किसान और मजदूरों की क्रांतिकारी शक्ति के बीच विरोध नहीं, बल्कि परस्पर पूरकता देखते थे।वे कृषि क्रांति को समाजवादी क्रांति से जोड़ने के पक्षधर थे।इसीलिए उन्होंने काफ़ी समय किसान राजनीति को दिया।किंतु वे बराबर कहा करते थे कि इस युग की दो मुख्य प्रेरणाएँ राष्ट्रीयता और समाजवाद हैं और राष्ट्रीय परिस्थितियों और आकांक्षाओं की दृष्टि से ही समाजवाद का अर्थ बताने पर जोर देते रहे। भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवाल से जोड़ना, आचार्य जी की भारतीय समाजवाद को एक स्थायी देन है।
आचार्य जी की समाजवादी व्याख्याएँ मानववादी आधारों पर विकसित हुई। उन्होंने साम्यवादियों की तरह इसके अंतर्गत केवल पेट का सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा, ’समाजवाद का सवाल केवल रोटी का सवाल नहीं है, समाजवाद मानव स्वतंत्रता की कुंजी है।….एक स्वतंत्र-सुखी समाज में संपूर्ण मनुष्यत्व की सृष्टि तभी हो सकती है जब साधन भी हों। उन्होंने अतीत के अनुभव के आलोक में ही वर्तमान को देखा और इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र तथा साहित्य के विविध विषयों पर अधिकारपूर्वक कलम चलाई। उन्होंने उसी साहित्य को प्रगतिशील माना, जो जीवन को केंद्र में रखकर चलता हो।
अपनी पुस्तक ‘समाजवाद: लक्ष्य और साधन’ में वे कहते हैं ‘‘समाजवाद का ध्येय वर्गहीन समाज की स्थापना है। समाजवाद प्रचलित समाज का इस प्रकार का संगठन करना चाहता है कि वर्तमान परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले शोषक और शोषित, पीड़क और पीड़ित वर्गों का अंत हो जाए; वह सहयोग के आधार पर संगठित व्यक्तियों का ऐसा समूह बन जाए जिसमें एक सदस्य की उन्नति का अर्थ स्वभावतः दूसरे सदस्य की उन्नति हो और सब मिल कर सामूहिक रूप से परस्पर उन्नति करते हुए जीवन व्यतीत करें।’’ (समाजवाद: लक्ष्य और साधन से उद्धृत)
 आचार्य जी राजनीतिक रूप से कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और आजादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी-प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रहे।17 मई 1934 को पटना में संपन्न हुए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी।इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा:
आचार्य जी राजनीतिक रूप से कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और आजादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी-प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रहे।17 मई 1934 को पटना में संपन्न हुए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता भी उन्होंने ही की थी।इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा:
“समाजवाद इस देश में स्थायी रूप से स्थापित हो चुका है और कांग्रेस के अंदर तथा देश में प्रतिदिन इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के अंदर उभरी इस नई विचारधारा का सामाजिक आधार लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी वर्ग है।कांग्रेस के बाहर इसके अनुयायियों में मजदूरों और बहुत कुछ हद तक किसानों के प्रतिनिधि हैं जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के वास्तविक क्रांतिकारी तत्व हैं। वास्तव में मजदूर वर्ग ही इसका अगुआ है जबकि किसान और बुद्धिजीवी वर्ग इसके सहायक मात्र हैं। कांग्रेस के अंदर हममें से अधिकांश लोग आज केवल बौद्धिक समाजवादी हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय संघर्ष के साथ हमारे लंबे जुड़ाव ने हमें बार-बार जनता के साथ घनिष्ठ संपर्क में लाया है, इसलिए हमारे केवल सिद्धांतों और सिद्धांतों में बदल जाने का कोई खतरा नहीं दिखता। हमें मजदूरों और किसानों को अपने साथ जोड़कर अपने आंदोलन के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम शिक्षित वर्ग को समाजवादी विचारों के रहस्यों से परिचित कराकर संतुष्ट नहीं होंगे। मैं समाजवादी अध्ययन मंडलों के गठन और भारतीय भाषाओं में समाजवादी साहित्य के निर्माण के महत्व को कम करके नहीं आंकता। यह अच्छा काम है और सबसे जरूरी भी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामने असली काम जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, आर्थिक मुद्दों पर उनके बीच रोजाना आंदोलन चलाना और उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक वर्ग में संगठित करना है। जनता के बीच काम करके ही हम खुद को प्रतिक्रियावादी प्रभावों से मुक्त कर सकते हैं और सर्वहारा दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। हम बौद्धिक वर्ग के सदस्य जो बड़ी गलती करते हैं, वह है जनता को पृष्ठभूमि में धकेलना। सच तो यह है कि हम हमेशा जनता को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनसे कभी नहीं सीखते। मन का यह रवैया गलत है। हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी इच्छाओं और जरूरतों के वफादार व्याख्याकार के रूप में काम करना चाहिए।”
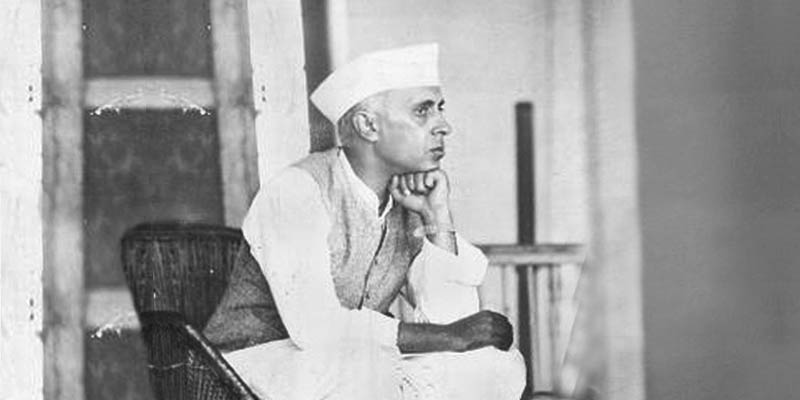 साथ ही आचार्य नरेन्द्र देव ने अपने इसी भाषण में अपने नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही भावुकता के साथ याद याद किया और कहा:
साथ ही आचार्य नरेन्द्र देव ने अपने इसी भाषण में अपने नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही भावुकता के साथ याद याद किया और कहा:
“मित्रों, आज हम कांग्रेस के भीतर समाजवादी आंदोलन की पहली इकाई की स्थापना कर रहे हैं। हमारे महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू की अनुपस्थिति में हमारा कार्य अत्यंत कठिन हो गया है। हम नहीं जानते कि हम उनकी बहुमूल्य सलाह, मार्गदर्शन और नेतृत्व से कब तक वंचित रहेंगे। मुझे विश्वास है कि वे कांग्रेस के भीतर इस नई पार्टी के जन्म का खुशी से स्वागत करेंगे और जेल की सलाखों के पीछे से हमारी प्रगति को गहरी दिलचस्पी से देखेंगे(पंडित जी उस समय देहरादून जेल में बंद थे)। आइए उनके महान उदाहरण से हमें उनकी कैद की अवधि के दौरान और प्रेरणा मिले और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि जिस उद्देश्य का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अंततः सफल होगा।”
ग़ौरतलब है कि 1934 से लेकर 1940 तक कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल थे जिनमें ईएमएस नंबूदरीपाद, सज्जाद ज़हीर, ए के गोपालन, पी. सुंदरैया, ज़ेड ए अहमद, दिनकर मेहता, सोली बाटलीवाला और बीपीएल बेदी के नाम उल्लेखनीय हैं।
1936 में आचार्य जी के भाषण का एक अंश है: ‘‘हमारा काम केवल साम्राज्यवाद के शोषण का ही अंत करना नहीं है किंतु साथ-साथ देश के उन सभी वर्गों के शोषण का अंत करना है जो आज जनता का शोषण कर रहे हैं। हम एक ऐसी नई सभ्यता का निर्माण करना चाहते हैं जिसका मूल प्राचीन सभ्यता में होगा, जिसका रूप-रंग देशी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यता के उत्कृष्ट अंश सुरक्षित रहेंगे और साथ-साथ उसमें ऐसे नवीन अंशों का भी समावेश होगा जो आज जगत में प्रगतिशील हैं और संसार के सामने एक नवीन आदर्श रखना चाहते हैं।’’ (आचार्य नरेंद्र देव वाड्मय, खंड 1)
आचार्य जी के गंभीर अध्येता अनिल नौरिया ने माना है कि, ‘‘आचार्य नरेंद्र देव के विचारों की सबसे बड़ी सार्थकता व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का सामाजिक परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया के साथ संवर्धन करने में है। उनका सामाजिक परिवर्तन के नैतिक पक्ष पर आग्रह जहां भारतीय दृष्टि से जुड़ा है वहीँ सामाजिक शक्तियों के वैज्ञानिक विश्लेषण का आग्रह मार्क्सवादी दृष्टि से। वे निश्चित रूप से मार्क्सवाद की बोल्शेविक धारा में विकसित नैतिकता-निरपेक्ष प्रवृत्ति के विरोधी थे।’’ (आचार्य नरेंद्र देव बर्थ सेंटेनरी वॉल्यूम).
1948 में जब सोशलिस्ट, कांग्रेस पार्टी से बाहर आ गए और स्वतंत्र रूप से सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया तो 1946 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत कर यूपी विधानसभा के सदस्य बने आचार्य जी और उनके ग्यारह अन्य सहयोगियों ने विधान सभा से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उस समय न इसकी जरूरत थी, न किसी ने मांग की थी। लेकिन आचार्य जी का मानना था कि कांग्रेस पार्टी से बाहर हो जाने और अलग पार्टी बना लेने के बाद विधानसभा का सदस्य बने रहना उनके लिए नैतिक रूप से उचित नहीं होगा।इसके बाद हुए उपचुनावों में वे खुद और उनके लगभग सभी साथी सहयोगी चुनाव हार गए। इन चुनावों में आचार्य जी के खिलाफ अत्यंत अशोभनीय प्रचार किया गया गया लेकिन वे अपने राजनीतिक सिद्धांतों और आदर्शों से विमुख नहीं हुए।अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद भी उनके इसी उप-चुनाव के बाद शुरू हुआ था।
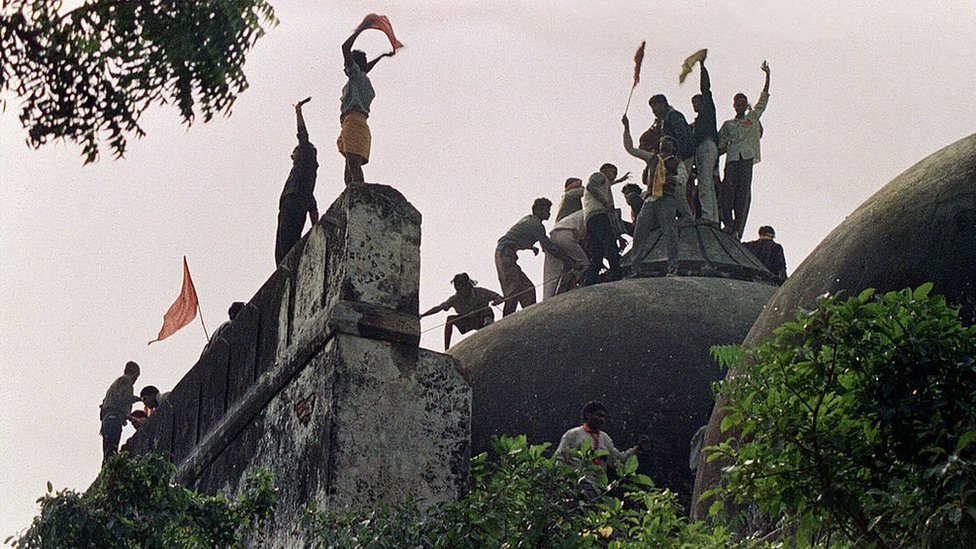 आचार्य नरेंद्र देव मानव समाज के कल्याण और नैतिक जीवन के विकास के लिए अन्याय का विरोध आवश्यक समझते थे उनका विचार था कि शोषण विहीन समाज में सामाजिकता के आधार पर मनुष्य का नैतिक विकास हो सकता है लेकिन स्वार्थ प्रेरणा पर आश्रित वर्ग समाज में सामाजिक भावनाओं का विकास बहुत कुछ अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए वे राजनीतिक स्वराज्य के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्वराज्य के लिए भी प्रयत्नशील रहे और राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाने के बाद जीवन पर्यन्त देश में जनतांत्रिक समाजवादी समाज निर्मित करने का प्रयास करते रहे। आचार्य नरेंद्र देव जी को देश और दुनिया मार्क्सवादी-समाजवादी तथा बौद्ध दर्शन का प्रखर विद्वान जानती और मानती है। लेकिन आचार्य जी के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी कम ही लोगों को है।
आचार्य नरेंद्र देव मानव समाज के कल्याण और नैतिक जीवन के विकास के लिए अन्याय का विरोध आवश्यक समझते थे उनका विचार था कि शोषण विहीन समाज में सामाजिकता के आधार पर मनुष्य का नैतिक विकास हो सकता है लेकिन स्वार्थ प्रेरणा पर आश्रित वर्ग समाज में सामाजिक भावनाओं का विकास बहुत कुछ अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए वे राजनीतिक स्वराज्य के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्वराज्य के लिए भी प्रयत्नशील रहे और राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाने के बाद जीवन पर्यन्त देश में जनतांत्रिक समाजवादी समाज निर्मित करने का प्रयास करते रहे। आचार्य नरेंद्र देव जी को देश और दुनिया मार्क्सवादी-समाजवादी तथा बौद्ध दर्शन का प्रखर विद्वान जानती और मानती है। लेकिन आचार्य जी के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी कम ही लोगों को है।
 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के 4 प्रमुख जिलों रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में किसान आंदोलन तेजी से चला। आचार्य जी ने इस आंदोलन में खुलकर भाग लिया तथा उनके प्रभावशाली भाषण के चलते किसान, आंदोलन में डटे रहे। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज में गोली चलायी। दमन के बावजूद आंदोलन उग्र रूप धारण कर लगातार चलता रहा तब सरकार को किसानों की बेदखली रोकने वाली मांग स्वीकार करनी पड़ी। अवध आंदोलन आचार्य जी की भूमिका के चलते सफल रहा। आंदोलन के दौरान किसानों को यह प्रतिज्ञा करायी गयी कि वे गैरकानूनी टैक्स अदा नहीं करेंगे, बेगार-बिना मजदूरी नहीं करेंगे। पलई, भूसा तथा रसल बाजार भाव पर बेचेंगे तथा नजराना नहीं देंगे। बेदखल खेत को कोई दूसरा किसान नहीं खरीदेगा तथा बेदखली कानून मंजूर होने तक सतत संघर्ष चलाएंगे।
1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के 4 प्रमुख जिलों रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में किसान आंदोलन तेजी से चला। आचार्य जी ने इस आंदोलन में खुलकर भाग लिया तथा उनके प्रभावशाली भाषण के चलते किसान, आंदोलन में डटे रहे। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए 7 जनवरी 1921 को मुंशीगंज में गोली चलायी। दमन के बावजूद आंदोलन उग्र रूप धारण कर लगातार चलता रहा तब सरकार को किसानों की बेदखली रोकने वाली मांग स्वीकार करनी पड़ी। अवध आंदोलन आचार्य जी की भूमिका के चलते सफल रहा। आंदोलन के दौरान किसानों को यह प्रतिज्ञा करायी गयी कि वे गैरकानूनी टैक्स अदा नहीं करेंगे, बेगार-बिना मजदूरी नहीं करेंगे। पलई, भूसा तथा रसल बाजार भाव पर बेचेंगे तथा नजराना नहीं देंगे। बेदखल खेत को कोई दूसरा किसान नहीं खरीदेगा तथा बेदखली कानून मंजूर होने तक सतत संघर्ष चलाएंगे।
 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।किसान सभा के गठन में आचार्यजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी वजह से आचार्य जी को 1939 में गया में हुए किसान सभा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया जिसमें आचार्यजी ने किसान सभा और कांग्रेस संगठन के संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि साम्राज्यवाद के विरोध में दोनों को एक साथ खड़े होकर किसान क्रांति को मज़बूत करने की जरूरत है ताकि किसान जमीन का मालिक बन जाये। राज्य और किसानों के बीच मध्यवर्ती शोषकों का अंत हो जाय। कर्जे के बोझ से किसानों को छुटकारा मिले तथा श्रम का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। सोशलिस्ट पार्टी ने आचार्य जी की प्रेरणा से 25 नवंबर 1949 को लखनऊ में एक विशाल ‘किसान मार्च’ आयोजित किया जिसमें 50 हजार से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया।फरवरी 1950 में डॉ. लोहिया की अध्यक्षता में रीवा में हिंद किसान पंचायत का पहला अधिवेशन हुआ, तब आचार्य जी ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए किसानों से संगठित होने का आह्वान किया। आचार्य जी ने जमींदारी उन्मूलन कमेटी को 1947 में लिखे ‘मेमोरेंडम’ में कहा कि जिस तरह से ज़मींदारों ने किसानों को लूटा, खसोटा और चूसा है यदि उसका हिसाब लगाया जाये तो किसानों के ऋण से मुक्त होना जमींदारों के बूते की बात नहीं। ऐसी हालत में जमीदारों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए।
1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।किसान सभा के गठन में आचार्यजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी वजह से आचार्य जी को 1939 में गया में हुए किसान सभा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया जिसमें आचार्यजी ने किसान सभा और कांग्रेस संगठन के संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि साम्राज्यवाद के विरोध में दोनों को एक साथ खड़े होकर किसान क्रांति को मज़बूत करने की जरूरत है ताकि किसान जमीन का मालिक बन जाये। राज्य और किसानों के बीच मध्यवर्ती शोषकों का अंत हो जाय। कर्जे के बोझ से किसानों को छुटकारा मिले तथा श्रम का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। सोशलिस्ट पार्टी ने आचार्य जी की प्रेरणा से 25 नवंबर 1949 को लखनऊ में एक विशाल ‘किसान मार्च’ आयोजित किया जिसमें 50 हजार से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया।फरवरी 1950 में डॉ. लोहिया की अध्यक्षता में रीवा में हिंद किसान पंचायत का पहला अधिवेशन हुआ, तब आचार्य जी ने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए किसानों से संगठित होने का आह्वान किया। आचार्य जी ने जमींदारी उन्मूलन कमेटी को 1947 में लिखे ‘मेमोरेंडम’ में कहा कि जिस तरह से ज़मींदारों ने किसानों को लूटा, खसोटा और चूसा है यदि उसका हिसाब लगाया जाये तो किसानों के ऋण से मुक्त होना जमींदारों के बूते की बात नहीं। ऐसी हालत में जमीदारों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए।
आचार्य जी ने देवरिया ज़िले में किसानों की फसल खराब होने के बाद हुए सत्याग्रह में भागीदारी करते हुए किसानों और सरकारी कर्मचारियों के भेद को समाप्त करने की मांग की। 1950 में पंजाब में भी नरेंद्र देव जी ने हिसार जिले में बेदखली के खिलाफ संघर्ष किया था। आचार्य जी का किसान संघर्ष का लंबा इतिहास है। आचार्य जी जीवन पर्यन्त दमे के मरीज रहे। इसी रोग के कारण 19 फ़रवरी, 1956 को मद्रास (वर्तमान चेन्नई) के इरोड में उनका निधन हो गया।
उनके निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 फरवरी 1956 को राज्य सभा में कहा:
“आचार्य नरेंद्र देव का निधन हममें से कई लोगों के लिए और, मैं समझता हूं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है।वे दुर्लभ विशिष्टता वाले व्यक्ति थे- कई क्षेत्रों में विशिष्टता- आत्मा में दुर्लभ, मन और बुद्धि में दुर्लभ, मन की अखंडता में दुर्लभ और अन्यथा। केवल उनका शरीर ही उनसे दूर हुआ है।मुझे नहीं मालूम कि यहां इस सदन में कोई और व्यक्ति ऐसा मौजूद है जो मुझसे ज्यादा समय तक उनके साथ जुड़ा रहा हो। 40 साल से भी पहले हम एक साथ आए थे और हमने आजादी के संघर्ष की धूल और गर्मी में और जेल जीवन की लंबी खामोशी में एक साथ अनगिनत अनुभव साझा किए थे, जहां हमने-मुझे अब याद नहीं-विभिन्न स्थानों(जेलों) पर चार या पांच साल एक साथ बिताए थे, और अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को करीब से जानने लगे थे और इसलिए, हममें से कई लोगों के लिए एक ओर जहाँ सार्वजनिक तौर पर क्षति की भावना है, वहीं दूसरी ओर निजी तौर पर भी क्षति की भावना है और यह भावना है कि एक असाधारण व्यक्ति चला गया है और उसके जैसा कोई व्यक्ति दोबारा मिलना बहुत कठिन होगा।”
राज्य सभा के सभापति और तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, “आचार्य नरेंद्र देव अपने आदर्शों, निष्ठा और स्वतंत्र निर्णय-क्षमता के लिए सुविख्यात थे।वे उस समय समाजवादी बने थे जब समाजवाद लोक-प्रचलन में भी नहीं आया था। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया।कालांतर में वे समाजवादी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाएँ लंबे समय तक स्मरण की जाएँगी।वे किसी भी रूप में छद्म से सर्वथा दूर थे।उनके विचारों ने हमारी पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया और हमारी नीतियों को नई दिशा प्रदान की हमने एक महान् देशभक्त, एक महान् नेता और एक बहुमूल्य व्यक्तित्व खो दिया है ।”
 जयप्रकाश नारायण ने आचार्य जी को अजातशत्रु कहा था। उन्होंने कहा था कि “आचार्य जी और गांधी जी के अतिरिक्त उन्हें अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आदमियत, इंसानियत, व्यक्तित्व, बौद्धिक शक्ति, ज्ञान, वाक्पटुता, भाषण शक्ति, इतिहास और दर्शन की समझ आचार्य नरेंद्र देव जैसी रखता हो। आचार्य नरेंद्र देव जी समाजवादी समाज के साथ-साथ समाजवादी सभ्यता का निर्माण करना चाहते थे। उनका स्पष्ट मत था कि समाजवादी समाज को बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ-साथ जनता के मानस को बदलने की जागृत करने की, स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाने तथा समाजवादी नैतिक मूल्यों के समुचित प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है।”
जयप्रकाश नारायण ने आचार्य जी को अजातशत्रु कहा था। उन्होंने कहा था कि “आचार्य जी और गांधी जी के अतिरिक्त उन्हें अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आदमियत, इंसानियत, व्यक्तित्व, बौद्धिक शक्ति, ज्ञान, वाक्पटुता, भाषण शक्ति, इतिहास और दर्शन की समझ आचार्य नरेंद्र देव जैसी रखता हो। आचार्य नरेंद्र देव जी समाजवादी समाज के साथ-साथ समाजवादी सभ्यता का निर्माण करना चाहते थे। उनका स्पष्ट मत था कि समाजवादी समाज को बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ-साथ जनता के मानस को बदलने की जागृत करने की, स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाने तथा समाजवादी नैतिक मूल्यों के समुचित प्रशिक्षण की नितांत आवश्यकता है।”
राहुल सांकृत्यायन ने आचार्य जी के बारे में कहा कि उनकी अंग्रेजी भाषा पर असाधारण पकड़ थी। बौद्ध दर्शन पर उनकी किताब ‘अभिकोशभाष्य’ को उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ बताया। ‘कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ का अनुवाद भी आचार्य जी और राहुल जी ने मिलकर शुरू किया था।
राममनोहर लोहिया ने आचार्य जी के बारे में कहा कि “वे बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य, बौद्ध इतिहास के साथ-साथ राजनीति की गहराई से समझ रखने वाले विद्वान थे। मंत्री पद न लेना इंकार करना उनके लिए छोटी बात थी। आचार्य जी के भाषण शिक्षाप्रद और जोशीले होते थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ में हजारों विद्यार्थियों को समाजवादी विचार से शिक्षित किया”।
 समाजवादी लेखक और पत्रकार और अब राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश के अनुसार, “आचार्य नरेंद्र देव और उनके सहयोगियों का सम्यक मूल्यांकन होना शेष है। पतनोन्मुख सत्ता या समाज, सर्वदा सत्ताधीशों या उनके प्रियजनों के अवदान के संदर्भ में चारण गीत गाता है।यह दोषपूर्ण दृष्टि है। इससे बीमार समाज जनमता-पनपता है, जो समाज अपने मनीषियों-ऋषितुल्य चिंतकों को भुलाने लगे, वह गंभीर सामाजिक रोग से पीड़ित हो कर बिखरता है।आज हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। इस माहौल में आचार्य जी जैसे तपस्वी, त्यागी और उद्धट विद्वान की याद अंधेरे में बढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। आचार्य नरेंद्र देव और उनके साथियों ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, बल्कि एक वैकल्पिक और नये समाज के लिए अपने जीवन की आहुति दी। सत्ता को ठुकरा कर संघर्ष का वरण किया।आचार्य जी उन चिंतकों में से थे, जो सदैव समय और वर्तमान की परिधि से आगे देखते-आंकते थे।वह देश, काल की सीमा से परे एक नये समाज की बुनियाद रखने वाले मनीषी थे। वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा रहे। उन्होंने ‘क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों’ की परिकल्पना की, जो राष्ट्रीय और समाजवादी क्रांति के लिए अपरिहार्य हैं। वह जीवनपर्यंत मार्क्सवादी रहे। राष्ट्रीयता की बात जिस शिद्दत से उन्होंने की, वह अनूठी है। देश में समाजवाद का सपना देखने वाले वह शिखर पुरुष रहे। इस संबंध में गांधीजी और उनके बीच गंभीर चर्चा हुई। इस कारण भारतीय संस्कृति-परंपरा के तहत देसी मुहावरे में उन्होंने समाजवाद को परिभाषित करने की कोशिश की। कट्टर मार्क्सवादियों की तरह केवल अफीम के रूप में उन्होंने ‘धर्म’ की चर्चा नहीं की, बल्कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा को पहचाना।उन्होंने निराकार समाजवादियों की कल्पना नहीं की। उनका सपना था, जहां-जहां आम जनता की बहुतायत है, वहां-वहां समाजवादी पाये जाने चाहिए। जनता के स्वार्थ, हक के लिए जहां भी जन संघर्ष हो रहा हो या साम्राज्यवादी या शोषणवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई चल रही हो, समाजवादियों को उसका हरावल दस्ता बनना चाहिए। ‘वर्ग चेतना’ और राष्ट्रीय चेतना के बीच सेतु बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो समाज, देश, क्षेत्रीय संकीर्णताओं सांप्रदायिक-भाषिक, जातिगत और क्षुद्र स्वार्थों की परिधि में लिपटा हो, वहां राष्ट्रीय चेतना अंकुरित नहीं होती।किसानों के संबंध में आचार्य जी ने गंभीरता से उस दौर में ही विचार किया। वह मानते थे, कोई अकेला नेता समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। ऐसे समाज की स्थापना मजदूर और किसान ही कर सकते हैं या उनकी पार्टी कर सकती है।’’
समाजवादी लेखक और पत्रकार और अब राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश के अनुसार, “आचार्य नरेंद्र देव और उनके सहयोगियों का सम्यक मूल्यांकन होना शेष है। पतनोन्मुख सत्ता या समाज, सर्वदा सत्ताधीशों या उनके प्रियजनों के अवदान के संदर्भ में चारण गीत गाता है।यह दोषपूर्ण दृष्टि है। इससे बीमार समाज जनमता-पनपता है, जो समाज अपने मनीषियों-ऋषितुल्य चिंतकों को भुलाने लगे, वह गंभीर सामाजिक रोग से पीड़ित हो कर बिखरता है।आज हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। इस माहौल में आचार्य जी जैसे तपस्वी, त्यागी और उद्धट विद्वान की याद अंधेरे में बढ़ रही युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। आचार्य नरेंद्र देव और उनके साथियों ने न सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, बल्कि एक वैकल्पिक और नये समाज के लिए अपने जीवन की आहुति दी। सत्ता को ठुकरा कर संघर्ष का वरण किया।आचार्य जी उन चिंतकों में से थे, जो सदैव समय और वर्तमान की परिधि से आगे देखते-आंकते थे।वह देश, काल की सीमा से परे एक नये समाज की बुनियाद रखने वाले मनीषी थे। वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा रहे। उन्होंने ‘क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों’ की परिकल्पना की, जो राष्ट्रीय और समाजवादी क्रांति के लिए अपरिहार्य हैं। वह जीवनपर्यंत मार्क्सवादी रहे। राष्ट्रीयता की बात जिस शिद्दत से उन्होंने की, वह अनूठी है। देश में समाजवाद का सपना देखने वाले वह शिखर पुरुष रहे। इस संबंध में गांधीजी और उनके बीच गंभीर चर्चा हुई। इस कारण भारतीय संस्कृति-परंपरा के तहत देसी मुहावरे में उन्होंने समाजवाद को परिभाषित करने की कोशिश की। कट्टर मार्क्सवादियों की तरह केवल अफीम के रूप में उन्होंने ‘धर्म’ की चर्चा नहीं की, बल्कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा को पहचाना।उन्होंने निराकार समाजवादियों की कल्पना नहीं की। उनका सपना था, जहां-जहां आम जनता की बहुतायत है, वहां-वहां समाजवादी पाये जाने चाहिए। जनता के स्वार्थ, हक के लिए जहां भी जन संघर्ष हो रहा हो या साम्राज्यवादी या शोषणवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई चल रही हो, समाजवादियों को उसका हरावल दस्ता बनना चाहिए। ‘वर्ग चेतना’ और राष्ट्रीय चेतना के बीच सेतु बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने स्वीकार किया कि जो समाज, देश, क्षेत्रीय संकीर्णताओं सांप्रदायिक-भाषिक, जातिगत और क्षुद्र स्वार्थों की परिधि में लिपटा हो, वहां राष्ट्रीय चेतना अंकुरित नहीं होती।किसानों के संबंध में आचार्य जी ने गंभीरता से उस दौर में ही विचार किया। वह मानते थे, कोई अकेला नेता समाजवादी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। ऐसे समाज की स्थापना मजदूर और किसान ही कर सकते हैं या उनकी पार्टी कर सकती है।’’
भारतीय समाजवाद के इस पितामह को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि ।
– क़ुरबान अली
(क़ुरबान अली, पिछले 45 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं।1980 से वे समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका ‘जनता’ में लिख रहे हैं।वे साप्ताहिक ‘रविवार’ ‘सन्डे ऑब्ज़र्वर’ बीबीसी, दूरदर्शन न्यूज़, राज्य सभा टीवी से संबद्ध रह चुके हैं और इन दिनों समाजवादी आंदोलन का इतिहास(1934-1977) लिखने और इस आंदोलन के दस्तावेज़ों को संपादित करने में व्यस्त हैं।उनसे संपर्क का पता है: qurban100@gmail.com )