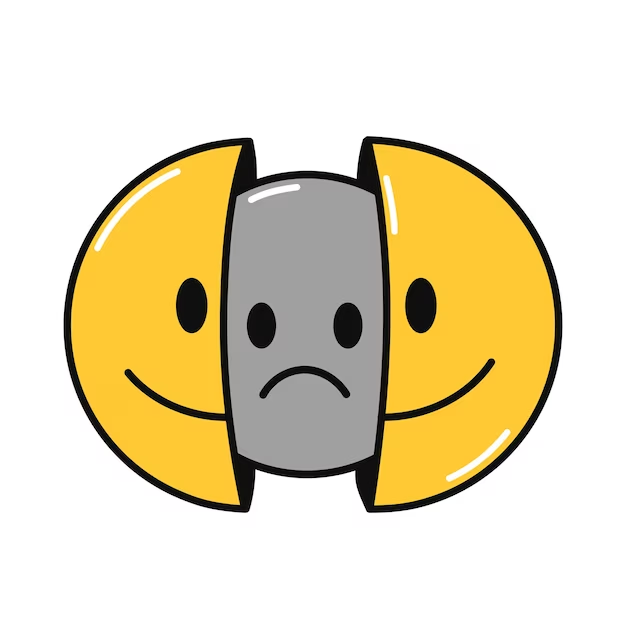जल, जंगल और ज़मीन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन का मूलभूत आधार हैं. सदियों से नदी के किनारे और जंगल में बसे लोगों का इन संसाधनों पर नैसर्गिक अधिकार रहा है. लेकिन सरकार नव-उदारवादी व्यवस्था की आड़ में आम आदमी को उसके इस अधिकार से वंचित करने की हरसंभव कोशिश करती रही है. चाहे वह जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े क़ानून बनाने की बात हो, या फिर इन संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की साजिश. आखिर किसके लिए हैं जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े क़ानून? प्रस्तुत है एक विश्लेषण...
 इस देश में आज भी गुलाम भारत के क़ानून ही चलते हैं. अंग्रेज यहां न सिर्फ अंग्रेजियत, बल्कि खुद के बनाए वे क़ानून भी छोड़ गए, जो दरअसल गैरक़ानूनी तरीके से भारत पर जबरन शासन करने के लिए बनाए गए थे. आज़ादी के बाद भी इस देश में सवा सौ साल पुराने क़ानून का होना यही बताता है कि आज भी इस देश का आम आदमी उसी तरह शासित हो रहा है, जैसे वह अंग्रेजों द्वारा शासित हो रहा था. हालांकि संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां बहस होती है और आनन-फानन में क़ानून भी बन जाते हैं. कहने को तो उक्त क़ानून जनता के लिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी क़ानून के बनने और उसे बनाने के पीछे की कुल सच्चाई यही है? क्या कोई क़ानून सचमुच उन करोड़ों लोगों के हितों से जुड़ा होता है, जिनके लिए दो जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना बेहद कठिन होता है. जल, जंगल और ज़मीन, ये तीन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सदियों से करोड़ों लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराते आ रहे हैं. नदियों के किनारे सभ्यताएं तो विकसित होती रहती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आज 21वीं सदी में भी हमारा समाज जल, जंगल और ज़मीन पर ही निर्भर है.
इस देश में आज भी गुलाम भारत के क़ानून ही चलते हैं. अंग्रेज यहां न सिर्फ अंग्रेजियत, बल्कि खुद के बनाए वे क़ानून भी छोड़ गए, जो दरअसल गैरक़ानूनी तरीके से भारत पर जबरन शासन करने के लिए बनाए गए थे. आज़ादी के बाद भी इस देश में सवा सौ साल पुराने क़ानून का होना यही बताता है कि आज भी इस देश का आम आदमी उसी तरह शासित हो रहा है, जैसे वह अंग्रेजों द्वारा शासित हो रहा था. हालांकि संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, वहां बहस होती है और आनन-फानन में क़ानून भी बन जाते हैं. कहने को तो उक्त क़ानून जनता के लिए जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी क़ानून के बनने और उसे बनाने के पीछे की कुल सच्चाई यही है? क्या कोई क़ानून सचमुच उन करोड़ों लोगों के हितों से जुड़ा होता है, जिनके लिए दो जून की रोटी का जुगाड़ कर पाना बेहद कठिन होता है. जल, जंगल और ज़मीन, ये तीन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो सदियों से करोड़ों लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराते आ रहे हैं. नदियों के किनारे सभ्यताएं तो विकसित होती रहती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आज 21वीं सदी में भी हमारा समाज जल, जंगल और ज़मीन पर ही निर्भर है.
आदिवासियों और जंगल के आसपास रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन का आधार ही जल, जंगल और ज़मीन हैं. इसके अलावा, देश की सत्तर फीसदी आबादी खेती से जुड़ी हुई है, यानी ज़मीन के सहारे अपना जीवनयापन कर रही है. लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि इस देश की सरकार जल, जंगल और ज़मीन पर आम आदमी के पुश्तैनी अधिकार को खत्म क्यों करना चाहती है? क्यों सरकार तथाकथित विकास के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में आ गई है? क्यों बड़े-बड़े होटल्स, मॉल्स, अपार्टमेंट्स के लिए खेती वाली ज़मीन का अधिग्रहण करके पूंजीपतियों के हाथों सौंप रही है? क्यों नदियों का पानी उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख रही है? क्यों जंगल के जंगल औद्योगिक घरानों को कारखाने लगाने के लिए दे दिए जाते हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या इस देश में क़ानून नामक कोई चीज नहीं है? जाहिर है कि क़ानून है, लेकिन ये क़ानून भी आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों को ़फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े क़ानूनों को ही देखिए, ये क़ानून भी आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि ख़ास लोगों के लिए खास मक़सद से बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं.
जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े
क़ानूनों की हक़ीक़त?
संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल: सवा सौ साल पुराने भूमि अधिग्रहण क़ानून में संशोधन के लिए सरकार ने क़रीब एक साल पहले प्रयास शुरू किए. मामला स्थायी समिति के पास गया और अंतत: संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास आ गया है, जिसे अब संसद से पारित कराया जाना है, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दु:खद पहलू यही है कि संसद की स्थायी समिति ने इस बिल में संशोधन के लिए जितने भी सुझाव दिए थे, उन्हें मंत्रालय ने मानने से इंकार कर दिया. यानी संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल भी आम आदमी के बजाय कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति करने वाला ही साबित होगा. इसका मतलब यही निकलता है कि सरकार उन लोगों के जीवन और आजीविका के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो वर्षों से अपनी ज़मीन और आजीविका बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने इन अमूल्य संसाधनों के लिए कोई मुआवज़ा नहीं चाहते, बल्कि अपनी ज़मीन पर अपना हक़ चाहते हैं.
हैरानी की बात तो यह है कि संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल में ग्रामसभा जैसी स्थानीय संस्था की कोई भूमिका नहीं है. यही तथ्य नए संशोधित भूमि अधिग्रहण क़ानून को भी महत्वहीन बना देता है. अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब ज़मीन अधिग्रहण में ग्रामीणों की कोई भूमिका या सहमति ही नहीं होगी, तो फिर आज़ाद भारत और गुलाम भारत के क़ानूनों में क्या फर्क़ रह जाएगा? प्रस्तावित बिल में स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि उस कृषि भूमि का ज़बरदस्ती अधिग्रहण न किया जाए, जो एक-फसली या बहु-फसली हो. इस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स़िर्फ बहु-फसली ज़मीन को ही अधिग्रहण के दायरे से बाहर रखने की बात कही, जबकि जन संगठनों का स्पष्ट मानना है कि इस तरह देश के 75 प्रतिशत किसान अधिग्रहण के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि देश में अधिकांश जगहों पर खेती वर्षा पर निर्भर है. इन खेतों में वर्ष में केवल एक फसल ही सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता के कारण पैदा की जा सकती है. ऐसी ज़मीनें भी अधिकांशत: दलित-आदिवासियों और छोटे किसानों के अधीन हैं. स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि निजी अथवा पीपीपी प्रोजेक्ट, जिसे सार्वजनिक उद्देश्य के प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित न किया गया हो, के लिए ज़बरदस्ती ज़मीन का अधिग्रहण न किया जाए, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस सुझाव को सिरे से नकार दिया. मंत्रालय ने कहा कि किसी भी निजी प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 80 प्रतिशत लोगों की सहमति मिलने पर ज़मीन अधिग्रहीत कर ली जाएगी. ज़ाहिर है कि ऐसी स्थिति में यह बिल नव-उदारवाद के दौर में व्यवसायिक घरानों को ही फायदा पहुंचाएगी. ग्रामसभा को लेकर स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि सामाजिक प्रभाव, पारिस्थितिक प्रभाव का आकलन और एक्सपर्ट कमेटी द्वारा समीक्षा का कार्य ग्रामसभा के सहयोग से किया जाना चाहिए तथा संबंधित रिपोर्ट ग्रामसभा को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लीनियर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे पर प्रभावित होने वाले 80 प्रतिशत परिवारों की सहमति पर ज़ोर दिया, जबकि इस मुद्दे पर जन संगठनों का कहना था कि इस क़ानून में किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामसभा की सीधी भागीदारी और सहमति आवश्यक होनी चाहिए. निजी योजनाओं के लिए केवल 80 प्रतिशत प्रभावित लोगों की सहमति पर्याप्त नहीं है.
इसके अलावा, भू-वापसी के मसले पर स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया था कि यदि अधिग्रहीत की गई ज़मीन का पांच साल तक उपयोग नहीं होता है, तो अधिग्रहण की तिथि के पांच साल बाद उसे उसके मालिक को वापस कर देना चाहिए. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस सुझाव को माना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी बहुत सी अधिग्रहीत ज़मीनें हैं, जिनका इस्तेमाल 25 सालों तक नहीं हुआ, फिर भी वे ज़मीनें उनके पुराने मालिकों को नहीं लौटाई गईं. ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि 5 साल बाद ज़मीन वापस कर दी जाएगी? अब आप ख़ुद सोचिए, अगर यह संशोधित बिल क़ानून बन जाता है, तो किसका फायदा होगा?
अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण बिल: ऐसी नदियों, जो एक राज्य से निकल कर दो अन्य राज्यों में बहती हों, के राष्ट्रीयकरण के लिए एक नया विधेयक तैयार किया गया है और उसे लोकसभा में पेश भी किया जा चुका है. उक्त नए विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि अंतर्राज्यीय नदियों पर किसी राज्य का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का ही अधिकार होना चाहिए. केंद्र सरकार का उनके जल पर पूरा नियंत्रण होगा और उसी की मर्जी से जल का बंटवारा होगा. राज्य सरकारें पानी और बिजली की अपनी ज़रूरत केंद्र सरकार को बताएंगी और फिर केंद्र सरकार यह निश्चित करेगी कि किसे कितना पानी देना है.
साथ ही किसी अंतर्राज्यीय नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लगाने का पूर्ण अधिकार भी केंद्र सरकार का ही होगा. बहरहाल, यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे भाजपा सांसद रमन डेका ने पेश किया है. इस विधेयक के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे मतभेद खत्म हो जाएंगे और पानी का बंटवारा सही ढंग से हो सकेगा. लेकिन सवाल यह उठता है कि जो भी प्रमुख नदियां हैं, वे किसी एक राज्य से निकल कर दो-तीन राज्यों तक जाती हैं. ऐसे में, अगर यह विधेयक क़ानून बनता है, तो फिर सारी प्रमुख नदियों पर राज्य की जगह केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा. अब ज़ाहिर है कि यह प्रावधान देश के संघीय स्वरूप को प्रभावित करेगा. अब इसकी क्या गारंटी है कि केंद्र में बैठी किसी पार्टी की सरकार राज्य में बैठी दूसरी पार्टी की सरकार के साथ, राजनीतिक कारणों के चलते, पानी बंटवारे को लेकर आनाकानी नहीं करेगी? पानी वैसे भी राज्य का विषय है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार नदियों पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है? जाहिर है, जंगल और ज़मीन के साथ जल भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है. हालांकि, पानी की लूट भी इस देश में सालों से मची हुई है.
अफसोस की बात तो यह है कि कॉरपोरेट घराने जिस तरह नदियों के पानी का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं और नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, उसके लिए तो सरकार कोई सख्त नियम-क़ानून नहीं बना रही है, लेकिन वह राष्ट्रीयकरण के बहाने नदियों पर अपने एकाधिकार के लिए क़ानून ज़रूर बनाना चाहती है.
वन अधिकार क़ानून: कहने को तो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 यानी वन अधिकार अधिनियम उन लोगों को वन और वन संपदा पर अधिकार देने की बात करता है, जो वनों में रहते हैं या वन संपदा के सहारे अपना जीवन जीते हैं, लेकिन यह क़ानून भी अब तक ऐसे लोगों को उनका अधिकार देने में असफल ही साबित हुआ है. यह क़ानून मुख्य रूप से 13 दिसंबर, 2006 से पहले जंगल में कृषि/जोती गई भूमि पर क़ानूनी अधिकार देता है, वन उत्पाद, जंगल में चारागाह और जलाशयों के उपयोग का अधिकार देता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है. देश के अनेक हिस्सों से आ रही खबरों के मुताबिक़, इस क़ानून के प्रावधानों का घोर उल्लंघन हो रहा है और इस खेल में ख़ुद सरकारी अधिकारी ही शामिल हैं, जो आदिवासियों को जबरन उनकी ज़मीन से बेदख़ल करने की कोशिश करते हैं और साथ ही उन्हें वन अधिकार क़ानून से मिले अधिकार से वंचित भी रखते हैं. इस क़ानून के पारित होने के बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह आदेश दिया था कि जंगल में रहने वाले लोगों की ज़मीनें बिना उनकी सहमति के, किसी प्रोजेक्ट या कॉरपोरेट हाउस को न दी जाए, लेकिन इस संबंध में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज (सरकारी अधिकारियों) ने अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं. उल्टे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और अन्य जगहों पर राज्य सरकारों द्वारा ज़बरदस्ती लोगों को धमका कर उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किए जाने की घटनाएं लगातार जारी हैं.
ग़ौरतलब है कि यही वन अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व एरिया में रहने वाले लोगों के साथ भी हो रहा है. वन विभाग अवैध तरीक़े से लोगों के वनों पर अधिकार का हनन कर रहा है. वन भूमि पर अधिकार के लिए वनाधिकार कमेटी लोगों द्वारा दिए गए सबूतों की जांच करती है, लेकिन इस काम में वन विभाग के अधिकारी सहयोग नहीं करते और सच तो यह है कि लोगों के दावे जानबूझ कर खारिज कर दिए जाते हैं. उदाहरण के लिए, राजस्थान राज्य सरकार ने प्रत्येक दावे के लिए यह ज़रूरी कर दिया है कि उस पर फॉरेस्ट बीट गार्ड या किसी अन्य अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए. इसका नतीजा यह होता है कि हस्ताक्षर के लिए दावेदारों को इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की चिरौरी करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है और तब भी, कई बार उनका काम नहीं होता. कुल मिलाकर इस सब का नतीजा यह निकलता है कि असली दावेदारों को उनका हक़ नहीं मिल पाता या उनके दावे खारिज कर दिए जाते हैं. इस संबंध में सरकार को जहां ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहीं सरकार उन्हें और अधिक शक्तियां दे देती है.
वन अधिकार क़ानून व्यक्तिगत अधिकार के अतिरिक्त सामुदायिक अधिकार भी देता है. इसका अर्थ यह हुआ कि एक समुदाय को इतनी शक्तियां मिलेंगी और उसे यह अधिकार होगा कि वह मिल-जुल कर अपने जंगल की देखभाल कर सके और उसे भू एवं वन माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों से बचा सके, लेकिन इस अधिकार का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने दिया जाता. सरकार चाहती, तो इस अधिकार को लागू करा सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रही है. यानी जिस केंद्र सरकार ने वन अधिकार क़ानून बनाया और जिन राज्य सरकारों को यह क़ानून लागू करना था, वही इसका उल्लंघन कर रही हैं. सवाल यह उठता है कि आखिर उक्त सरकारें ऐसा किसके लिए कर रही हैं? जाहिर है, जंगल और ज़मीन से आम आदमी को बेदखल करके सरकार वहां पर कॉरपोरेट घरानों का साम्राज्य स्थापित कराना चाहती है, अन्यथा जिस सरकार ने ख़ुद ऐसा क़ानून बनाकर लोगों को अधिकार देने की बात कही, वही इसे लागू कराने से हिचकती क्यों?
जल,जंगल और ज़मीन – आखिर सरकार किसके लिए कानून बनाती है?
Adv from Sponsors